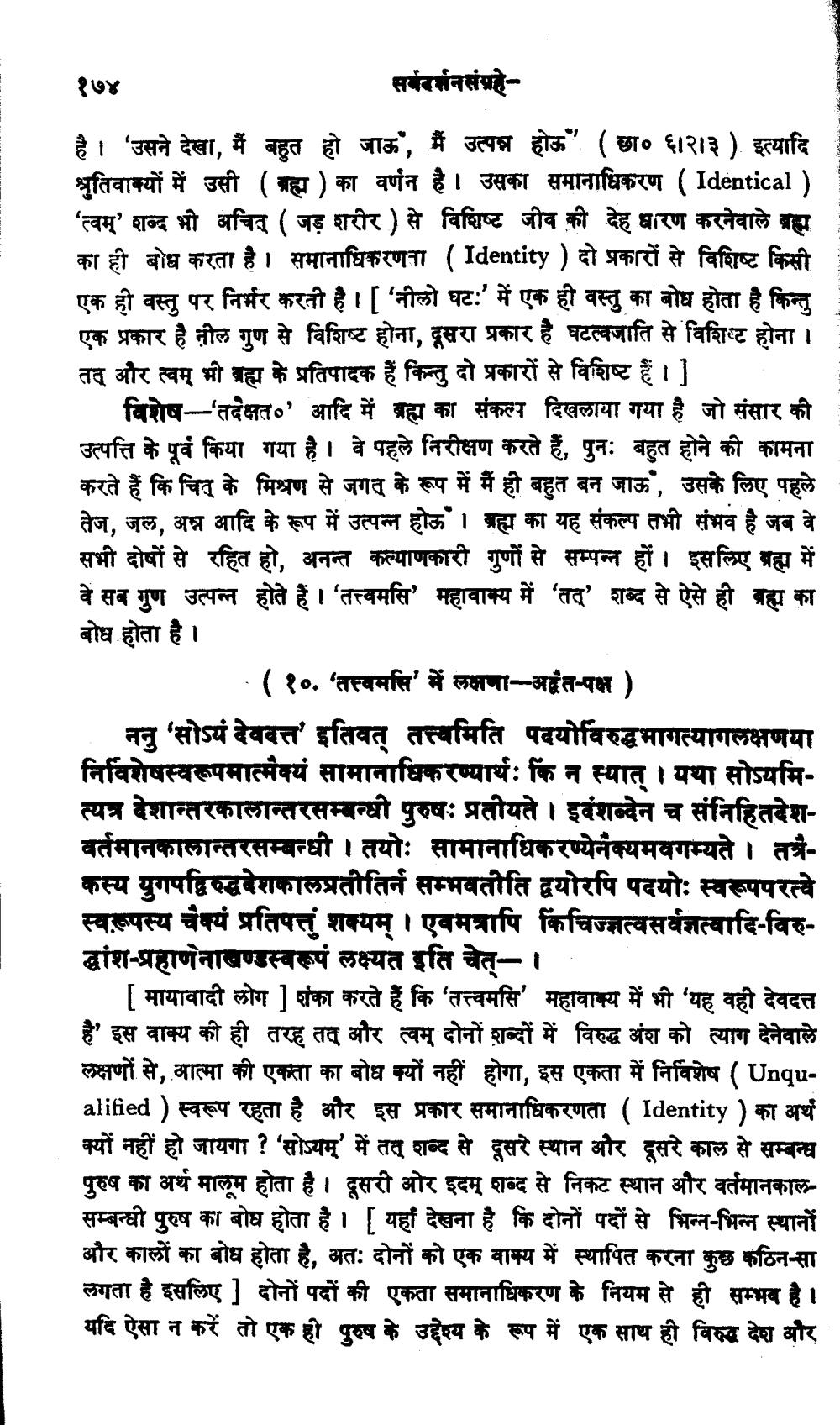________________
१७४
सर्वसनसंग्रहेहै। 'उसने देखा, मैं बहुत हो जाऊ', मैं उत्पन्न होऊ" (छा० ६।२।३ ) इत्यादि। श्रुतिवाक्यों में उसी (ब्रह्म ) का वर्णन है। उसका समानाधिकरण ( Identical ) 'त्वम्' शब्द भी अचित ( जड़ शरीर ) से विशिष्ट जीव की देह धारण करनेवाले ब्रह्म का ही बोध करता है। समानाधिकरणता ( Identity ) दो प्रकारों से विशिष्ट किसी एक ही वस्तु पर निर्भर करती है। [ 'नीलो घटः' में एक ही वस्तु का बोध होता है किन्तु एक प्रकार है नील गुण से विशिष्ट होना, दूसरा प्रकार है घटत्वजाति से विशिष्ट होना। तत् और त्वम् भी ब्रह्म के प्रतिपादक हैं किन्तु दो प्रकारों से विशिष्ट हैं।]
विशेष–'तदेक्षत०' आदि में ब्रह्म का संकल दिखलाया गया है जो संसार की उत्पत्ति के पूर्व किया गया है। वे पहले निरीक्षण करते हैं, पुनः बहुत होने की कामना करते हैं कि चित् के मिश्रण से जगत के रूप में मैं ही बहुत बन जाऊ', उसके लिए पहले तेज, जल, अन्न आदि के रूप में उत्पन्न होऊ । ब्रह्म का यह संकल्प तभी संभव है जब वे सभी दोषों से रहित हो, अनन्त कल्याणकारी गुणों से सम्पन्न हों। इसलिए ब्रह्म में वे सब गुण उत्पन्न होते हैं । 'तत्त्वमसि' महावाक्य में 'तत्' शब्द से ऐसे ही ब्रह्म का बोध होता है।
- (१०. 'तत्त्वमसि' में लक्षना-अहूत-पक्ष ) ननु 'सोऽयं देवदत्त' इतिवत् तत्त्वमिति पदयोविरुद्धभागत्यागलक्षणया निविशेषस्वरूपमात्मैक्यं सामानाधिकरण्यार्थः किं न स्यात् । यथा सोऽयमित्यत्र देशान्तरकालान्तरसम्बन्धी पुरुषः प्रतीयते । इदंशब्देन च संनिहितदेशवर्तमानकालान्तरसम्बन्धी । तयोः सामानाधिकरण्येनैक्यमवगम्यते। तत्रकस्य युगपद्विरुद्धदेशकालप्रतीतिर्न सम्भवतीति द्वयोरपि पदयोः स्वरूपपरत्वे स्वरूपस्य चैक्यं प्रतिपत्तुं शक्यम् । एवमत्रापि किंचिज्जत्वसर्वज्ञत्वादि-विरुद्धांश-प्रहाणेनाखण्डस्वरूपं लक्ष्यत इति चेत् ।
[मायावादी लोग ] शंका करते हैं कि 'तत्त्वमसि' महावाक्य में भी 'यह वही देवदत्त है' इस वाक्य की ही तरह तत् और त्वम् दोनों शब्दों में विरुद्ध अंश को त्याग देनेवाले लक्षणों से, आत्मा की एकता का बोध क्यों नहीं होगा, इस एकता में निर्विशेष ( Unqualified ) स्वरूप रहता है और इस प्रकार समानाधिकरणता ( Identity ) का अर्थ क्यों नहीं हो जायगा ? 'सोऽयम्' में तत् शब्द से दूसरे स्थान और दूसरे काल से सम्बन्ध पुरुष का अर्थ मालूम होता है। दूसरी ओर इदम् शब्द से निकट स्थान और वर्तमानकालसम्बन्धी पुरुष का बोध होता है। [यहां देखना है कि दोनों पदों से भिन्न-भिन्न स्थानों और कालों का बोध होता है, अतः दोनों को एक वाक्य में स्थापित करना कुछ कठिन-सा लगता है इसलिए ] दोनों पदों की एकता समानाधिकरण के नियम से ही सम्भव है। यदि ऐसा न करें तो एक ही पुरुष के उद्देश्य के रूप में एक साथ ही विरुव देश और