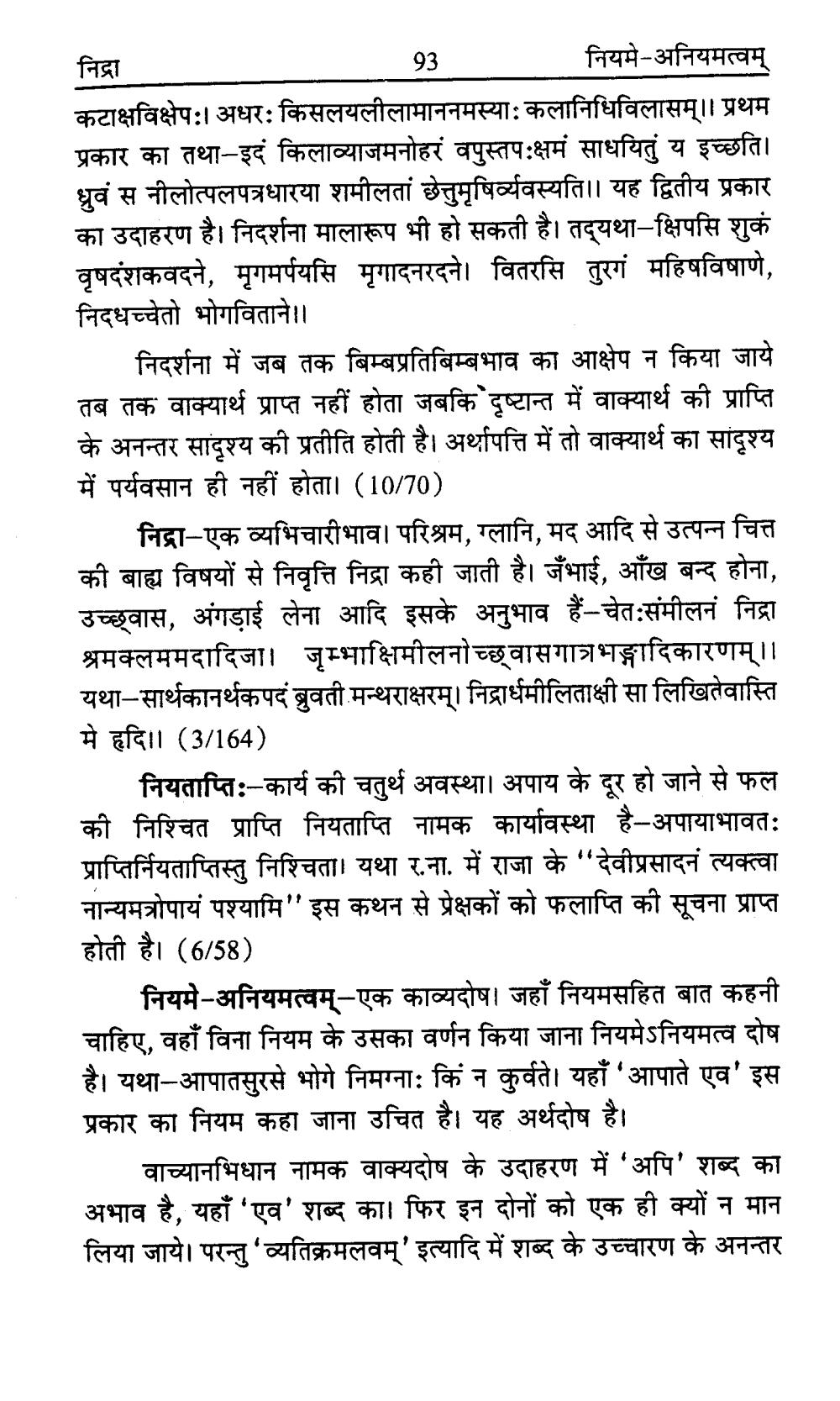________________
निद्रा
93
नियमे -अनियमत्वम् कटाक्षविक्षेपः। अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम् ।। प्रथम प्रकार का तथा - इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति । ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति । । यह द्वितीय प्रकार का उदाहरण है। निदर्शना मालारूप भी हो सकती है । तद्यथा - क्षिपसि शुकं वृषदंशकवदने, मृगमर्पयसि मृगादनरदने । वितरसि तुरगं महिषविषाणे, निदधच्चेतो भोगविताने ।।
निदर्शना में जब तक बिम्बप्रतिबिम्बभाव का आक्षेप न किया जाये तब तक वाक्यार्थ प्राप्त नहीं होता जबकि दृष्टान्त में वाक्यार्थ की प्राप्ति के अनन्तर सादृश्य की प्रतीति होती है । अर्थापत्ति में तो वाक्यार्थ का सांदृश्य में पर्यवसान ही नहीं होता । ( 10/70 )
निद्रा - एक व्यभिचारी भाव। परिश्रम, ग्लानि, मद आदि से उत्पन्न चित्त की बाह्य विषयों से निवृत्ति निद्रा कही जाती है। जँभाई, आँख बन्द होना, उच्छ्वास, अंगड़ाई लेना आदि इसके अनुभाव हैं- चेत: संमीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । जुम्भाक्षिमीलनोच्छ्वास गात्र भङ्गादिकारणम् ।। यथा - सार्थकानर्थकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम् । निद्रार्धमीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि । (3/164)
नियताप्तिः - कार्य की चतुर्थ अवस्था । अपाय के दूर हो जाने से फल की निश्चित प्राप्ति नियताप्ति नामक कार्यावस्था है- अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिस्तु निश्चिता । यथा र.ना. में राजा के " देवीप्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि" इस कथन से प्रेक्षकों को फलाप्ति की सूचना प्राप्त होती है। (6/58)
नियमे - अनियमत्वम् - एक काव्यदोष । जहाँ नियमसहित बात कहनी चाहिए, वहाँ विना नियम के उसका वर्णन किया जाना नियमेऽनियमत्व दोष है । यथा - आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुर्वते । यहाँ 'आपाते एव' इस प्रकार का नियम कहा जाना उचित है। यह अर्थदोष है।
वाच्यानभिधान नामक वाक्यदोष के उदाहरण में 'अपि' शब्द का अभाव है, यहाँ 'एव' शब्द का। फिर इन दोनों को एक ही क्यों न मान लिया जाये। परन्तु 'व्यतिक्रमलवम्' इत्यादि में शब्द के उच्चारण के अनन्तर