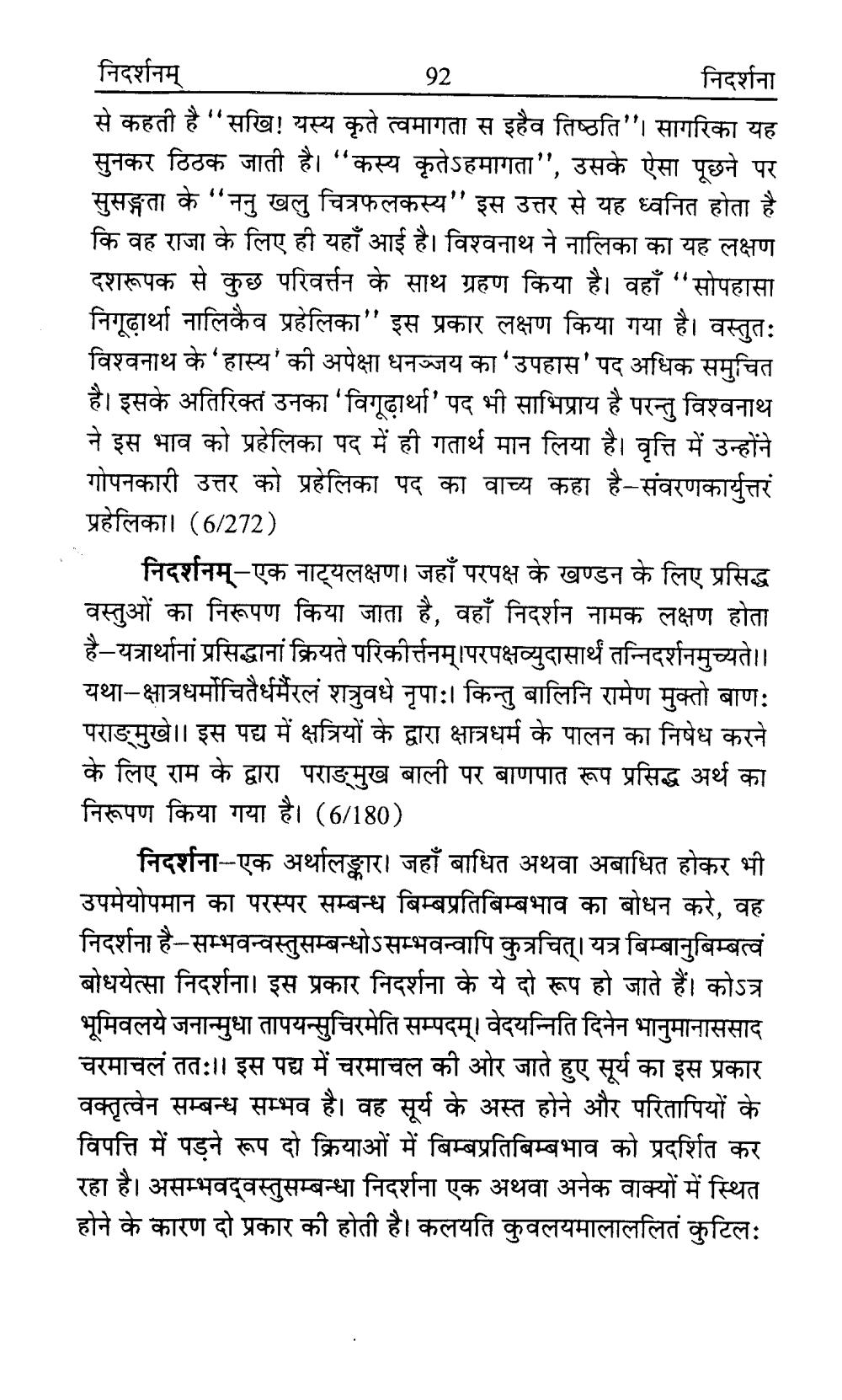________________
निदर्शनम्
92
निदर्शना
से कहती है " सखि ! यस्य कृते त्वमागता स इहैव तिष्ठति" । सागरिका यह सुनकर ठिठक जाती है । " कस्य कृतेऽहमागता", उसके ऐसा पूछने पर सुसङ्गता के " ननु खलु चित्रफलकस्य " इस उत्तर से यह ध्वनित होता है कि वह राजा के लिए ही यहाँ आई है । विश्वनाथ ने नालिका का यह लक्षण दशरूपक से कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है। वहाँ "सोपहासा निगूढ़ार्था नालिकैव प्रहेलिका " इस प्रकार लक्षण किया गया है। वस्तुतः विश्वनाथ के 'हास्य' की अपेक्षा धनञ्जय का 'उपहास' पद अधिक समुचित है। इसके अतिरिक्त उनका 'विगूढ़ार्था' पद भी साभिप्राय है परन्तु विश्वनाथ ने इस भाव को प्रहेलिका पद में ही गतार्थ मान लिया है। वृत्ति में उन्होंने गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका पद का वाच्य कहा है-संवरणकार्युत्तरं प्रहेलिका । (6/272)
निदर्शनम् - एक नाट्यलक्षण । जहाँ परपक्ष के खण्डन के लिए प्रसिद्ध वस्तुओं का निरूपण किया जाता है, वहाँ निदर्शन नामक लक्षण होता है - यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्त्तनम् । परपक्षव्युदासार्थं तन्निदर्शनमुच्यते ।। यथा- क्षात्रधर्मोचितैर्धर्मैरलं शत्रुवधे नृपाः । किन्तु बालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराङ्मुखे ।। इस पद्य में क्षत्रियों के द्वारा क्षात्रधर्म के पालन का निषेध करने के लिए राम के द्वारा पराङ्मुख बाली पर बाणपात रूप प्रसिद्ध अर्थ का निरूपण किया गया है। (6/180)
निदर्शना- एक अर्थालङ्कार । जहाँ बाधित अथवा अबाधित होकर भी उपमेयोपमान का परस्पर सम्बन्ध बिम्बप्रतिबिम्बभाव का बोधन करे, वह निदर्शना है - सम्भवन्वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्वापि कुत्रचित् । यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना । इस प्रकार निदर्शना के ये दो रूप हो जाते हैं। कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति सम्पदम् । वेदयन्निति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं ततः।। इस पद्य में चरमाचल की ओर जाते हुए सूर्य का इस प्रकार वक्तृत्वेन सम्बन्ध सम्भव है। वह सूर्य के अस्त होने और परितापियों के विपत्ति में पड़ने रूप दो क्रियाओं में बिम्बप्रतिबिम्बभाव को प्रदर्शित कर रहा है। असम्भववस्तुसम्बन्धा निदर्शना एक अथवा अनेक वाक्यों में स्थित होने के कारण दो प्रकार की होती है। कलयति कुवलयमालाललितं कुटिल: