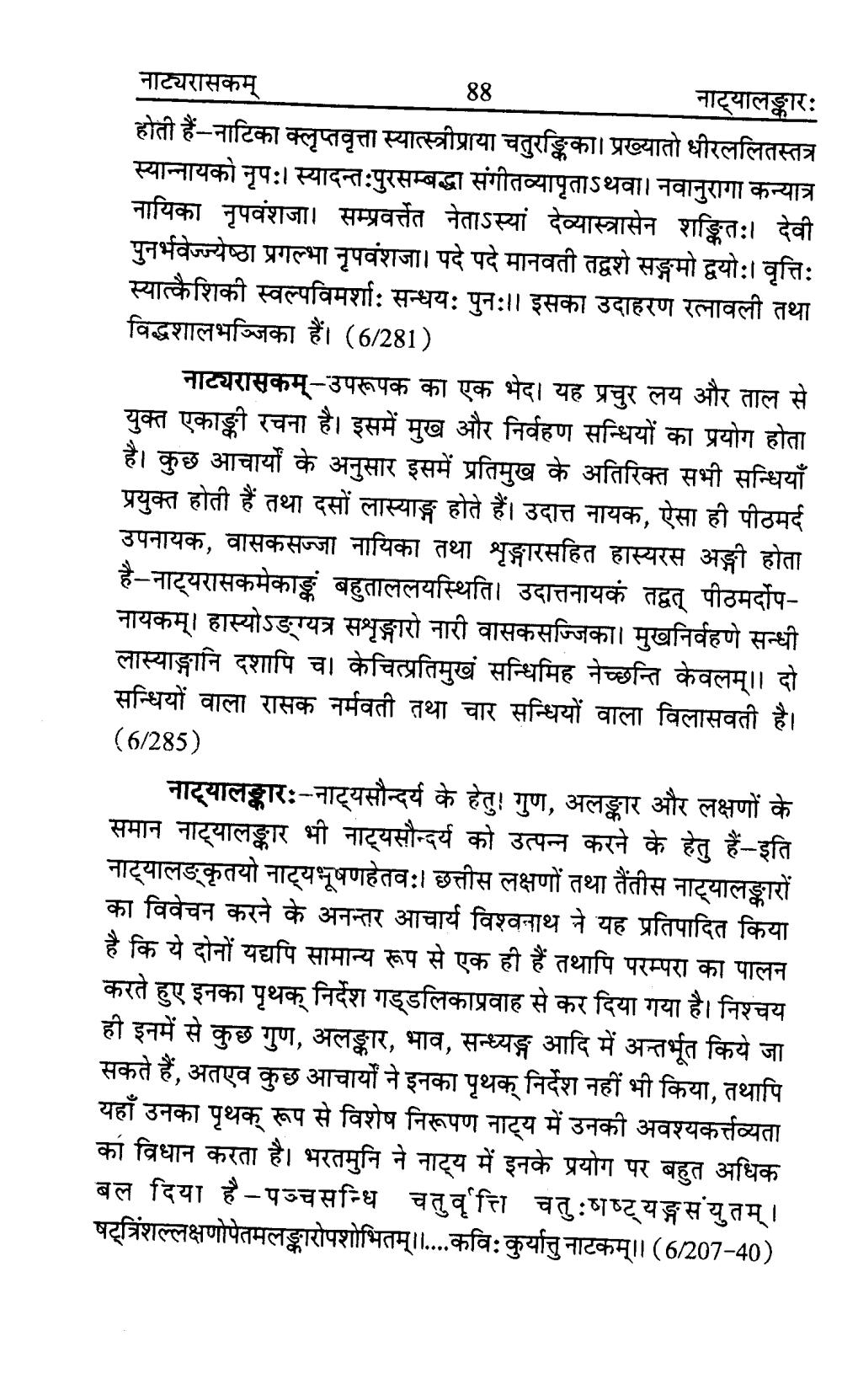________________
नाट्यरासकम्
88
नाट्यालङ्कारः
होती हैं-नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्स्त्रीप्राया चतुरङ्किका । प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः। स्यादन्तःपुरसम्बद्धा संगीतव्यापृताऽथवा । नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा । सम्प्रवर्त्तेत नेताऽस्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कितः । देवी पुनर्भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा । पदे पदे मानवती तद्वशे सङ्गमो द्वयोः । वृत्ति: स्यात्कैशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः । । इसका उदाहरण रत्नावली तथा विद्धशालभञ्जिका हैं। (6/281 )
नाट्यरासकम्-उपरूपक का एक भेद। यह प्रचुर लय और ताल से युक्त एकाङ्की रचना है। इसमें मुख और निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता है। कुछ आचार्यों के अनुसार इसमें प्रतिमुख के अतिरिक्त सभी सन्धियाँ प्रयुक्त होती हैं तथा दसों लास्याङ्ग होते हैं। उदात्त नायक, ऐसा ही पीठमर्द उपनायक, वासकसज्जा नायिका तथा शृङ्गारसहित हास्यरस अङ्गी होता है-नाट्यरासकमेकाङ्कं बहुताललयस्थिति । उदात्तनायकं तद्वत् पीठमर्दोपनायकम्। हास्योऽङ्ग्यत्र सशृङ्गारो नारी वासकसज्जिका । मुखनिर्वहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च । केचित्प्रतिमुखं सन्धिमिह नेच्छन्ति केवलम् ।। दो सन्धियों वाला रासक नर्मवती तथा चार सन्धियों वाला विलासवती है। (6/285)
नाट्यालङ्कारः - नाट्यसौन्दर्य के हेतु ! गुण, अलङ्कार और लक्षणों के समान नाट्यालङ्कार भी नाट्यसौन्दर्य को उत्पन्न करने के हेतु हैं - इति नाट्यालङ्कृतयो नाट्यभूषणहेतवः । छत्तीस लक्षणों तथा तैंतीस नाट्यालङ्कारों का विवेचन करने के अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने यह प्रतिपादित किया है कि ये दोनों यद्यपि सामान्य रूप से एक ही हैं तथापि परम्परा का पालन करते हुए इनका पृथक् निर्देश गड्डलिकाप्रवाह से कर दिया गया है। निश्चय ही इनमें से कुछ गुण, अलङ्कार, भाव, सन्ध्यङ्ग आदि में अन्तर्भूत किये जा सकते हैं, अतएव कुछ आचार्यों ने इनका पृथक् निर्देश नहीं भी किया, तथापि यहाँ उनका पृथक् रूप से विशेष निरूपण नाट्य में उनकी अवश्यकर्त्तव्यता का विधान करता है। भरतमुनि ने नाट्य में इनके प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है - पञ्चसन्धि चतुर्वृत्ति चतुःषष्ट्यङ्गसंयुतम् । षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतमलङ्कारोपशोभितम् ।... कवि : कुर्यात्तु नाटकम्।। (6/207-40)