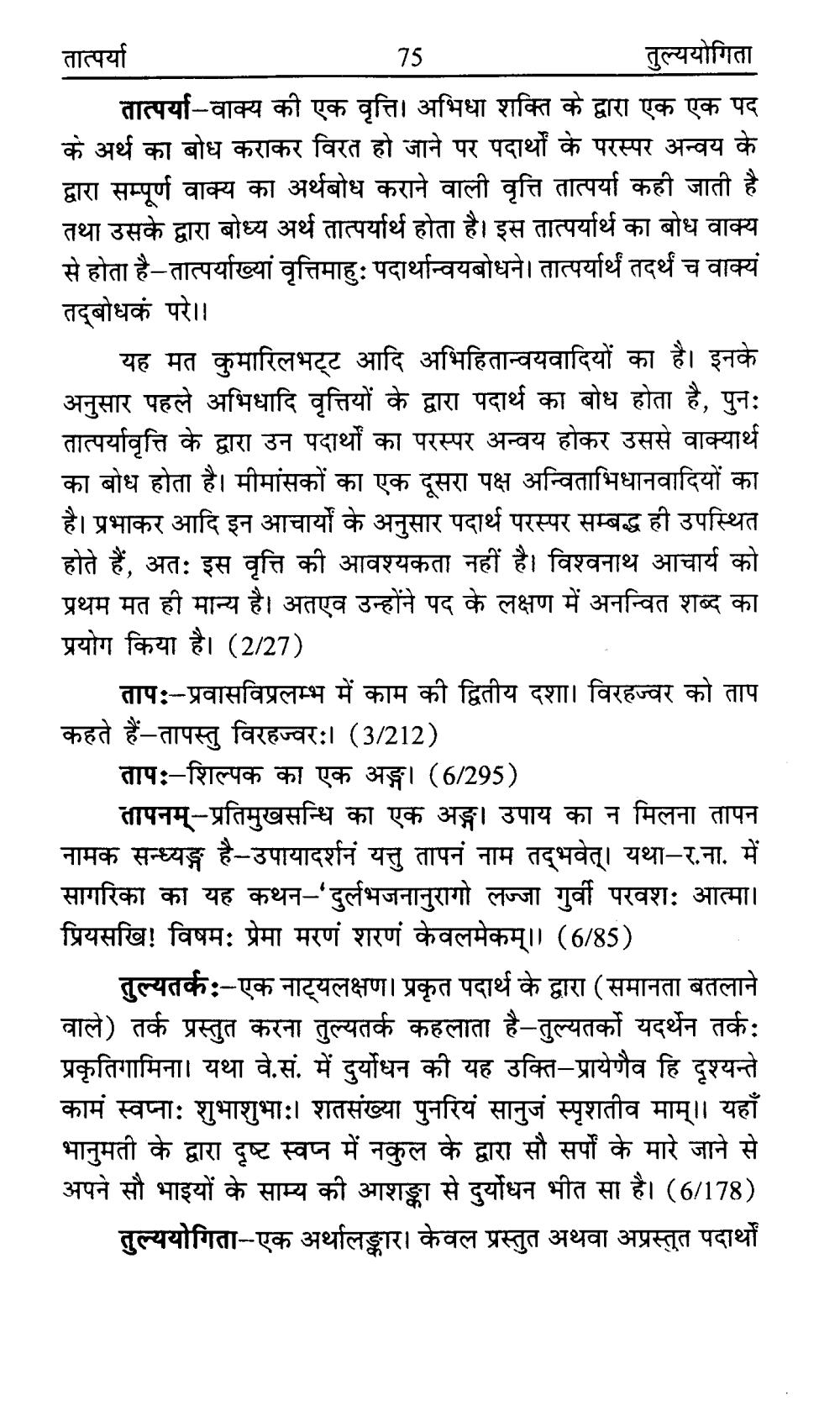________________
75
तात्पर्या
तुल्ययोगिता तात्पर्या-वाक्य की एक वृत्ति। अभिधा शक्ति के द्वारा एक एक पद के अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर पदार्थों के परस्पर अन्वय के द्वारा सम्पूर्ण वाक्य का अर्थबोध कराने वाली वृत्ति तात्पर्या कही जाती है तथा उसके द्वारा बोध्य अर्थ तात्पर्यार्थ होता है। इस तात्पर्यार्थ का बोध वाक्य से होता है-तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने। तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे।।
यह मत कुमारिलभट्ट आदि अभिहितान्वयवादियों का है। इनके अनुसार पहले अभिधादि वृत्तियों के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, पुनः तात्पर्यावृत्ति के द्वारा उन पदार्थों का परस्पर अन्वय होकर उससे वाक्यार्थ का बोध होता है। मीमांसकों का एक दूसरा पक्ष अन्विताभिधानवादियों का है। प्रभाकर आदि इन आचार्यों के अनुसार पदार्थ परस्पर सम्बद्ध ही उपस्थित होते हैं, अतः इस वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। विश्वनाथ आचार्य को प्रथम मत ही मान्य है। अतएव उन्होंने पद के लक्षण में अनन्वित शब्द का प्रयोग किया है। (2/27)
तापः-प्रवासविप्रलम्भ में काम की द्वितीय दशा। विरहज्वर को ताप कहते हैं-तापस्तु विरहज्वरः। (3/212)
तापः-शिल्पक का एक अङ्ग। (6/295)
तापनम्-प्रतिमुखसन्धि का एक अङ्ग। उपाय का न मिलना तापन नामक सन्ध्यङ्ग है-उपायादर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्। यथा-र.ना. में सागरिका का यह कथन-'दुर्लभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवशः आत्मा। प्रियसखि! विषमः प्रेमा मरणं शरणं केवलमेकम्।। (6/85)
तुल्यतर्क:-एक नाट्यलक्षण। प्रकृत पदार्थ के द्वारा (समानता बतलाने वाले) तर्क प्रस्तुत करना तुल्यतर्क कहलाता है-तुल्यतर्को यदर्थेन तर्क: प्रकृतिगामिना। यथा वे.सं. में दुर्योधन की यह उक्ति-प्रायेणैव हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः। शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतीव माम्।। यहाँ भानुमती के द्वारा दृष्ट स्वप्न में नकुल के द्वारा सौ सर्यों के मारे जाने से अपने सौ भाइयों के साम्य की आशङ्का से दुर्योधन भीत सा है। (6/178)
तुल्ययोगिता-एक अर्थालङ्कार। केवल प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदार्थों