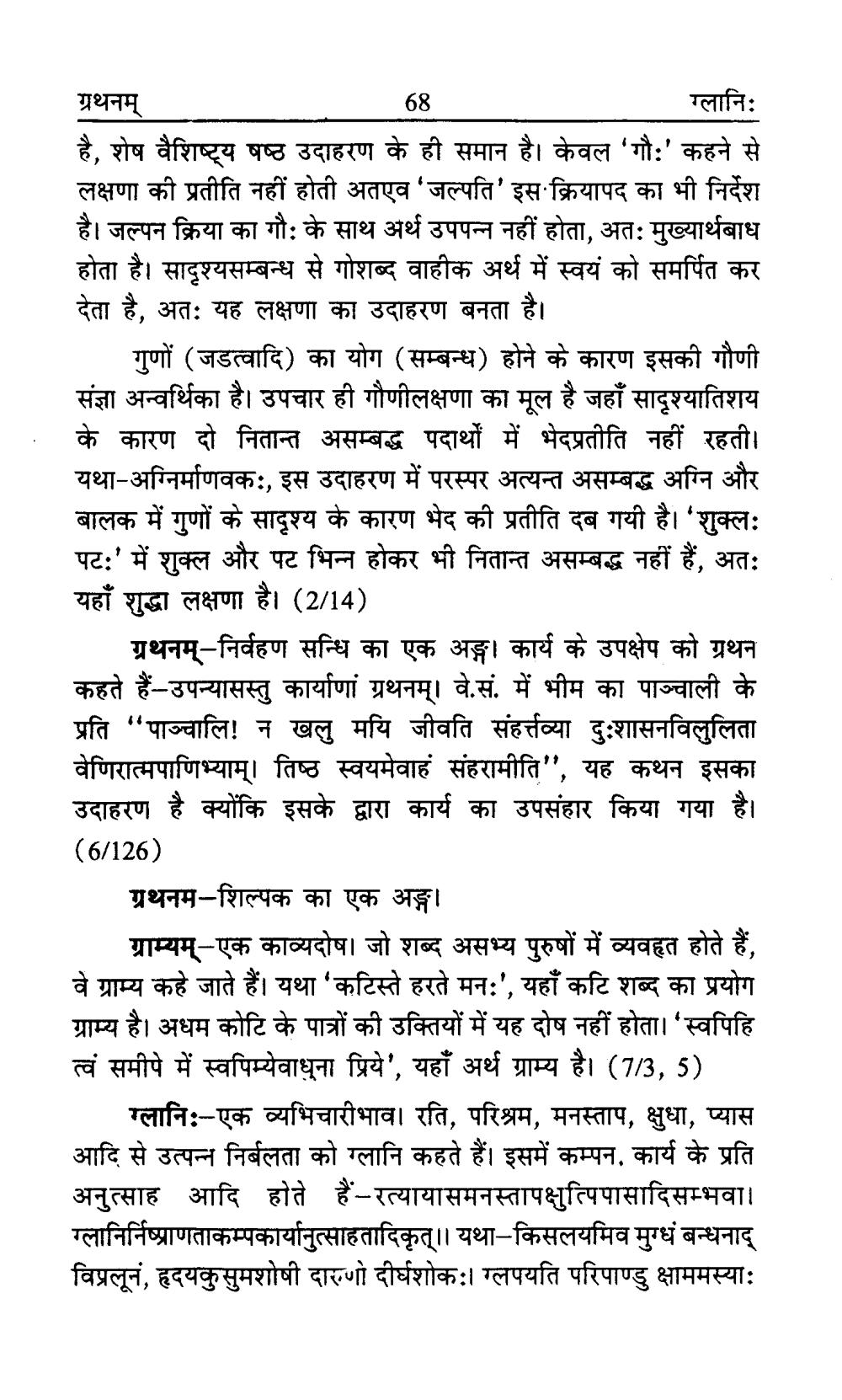________________
ग्रथनम्
68
ग्लानिः है, शेष वैशिष्ट्य षष्ठ उदाहरण के ही समान है। केवल 'गौः' कहने से लक्षणा की प्रतीति नहीं होती अतएव 'जल्पति' इस क्रियापद का भी निर्देश है। जल्पन क्रिया का गौ: के साथ अर्थ उपपन्न नहीं होता, अत: मुख्यार्थबाध होता है। सादृश्यसम्बन्ध से गोशब्द वाहीक अर्थ में स्वयं को समर्पित कर देता है, अतः यह लक्षणा का उदाहरण बनता है।
गुणों (जडत्वादि) का योग (सम्बन्ध) होने के कारण इसकी गौणी संज्ञा अन्वर्थिका है। उपचार ही गौणीलक्षणा का मूल है जहाँ सादृश्यातिशय के कारण दो नितान्त असम्बद्ध पदार्थों में भेदप्रतीति नहीं रहती। यथा-अग्निर्माणवकः, इस उदाहरण में परस्पर अत्यन्त असम्बद्ध अग्नि और बालक में गुणों के सादृश्य के कारण भेद की प्रतीति दब गयी है। 'शुक्लः पटः' में शुक्ल और पट भिन्न होकर भी नितान्त असम्बद्ध नहीं हैं, अतः यहाँ शुद्धा लक्षणा है। (2/14)
ग्रथनम्-निर्वहण सन्धि का एक अङ्ग। कार्य के उपक्षेप को ग्रथन कहते हैं-उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनम्। वे.सं. में भीम का पाञ्चाली के प्रति "पाञ्चालि! न खलु मयि जीवति संहर्त्तव्या दुःशासनविलुलिता वेणिरात्मपाणिभ्याम्। तिष्ठ स्वयमेवाहं संहरामीति", यह कथन इसका उदाहरण है क्योंकि इसके द्वारा कार्य का उपसंहार किया गया है। (6/126)
ग्रथनम-शिल्पक का एक अङ्ग।
ग्राम्यम्-एक काव्यदोष। जो शब्द असभ्य पुरुषों में व्यवहत होते हैं, वे ग्राम्य कहे जाते हैं। यथा 'कटिस्ते हरते मनः', यहाँ कटि शब्द का प्रयोग ग्राम्य है। अधम कोटि के पात्रों की उक्तियों में यह दोष नहीं होता। 'स्वपिहि त्वं समीपे में स्वपिम्येवाधुना प्रिये', यहाँ अर्थ ग्राम्य है। (7/3, 5)
ग्लानिः-एक व्यभिचारीभाव। रति, परिश्रम, मनस्ताप, क्षुधा, प्यास आदि से उत्पन्न निर्बलता को ग्लानि कहते हैं। इसमें कम्पन. कार्य के प्रति अनुत्साह आदि होते हैं-रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा। ग्लानिर्निष्प्राणताकम्पकार्यानुत्साहतादिकृत्।। यथा-किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद् विप्रलून, हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः