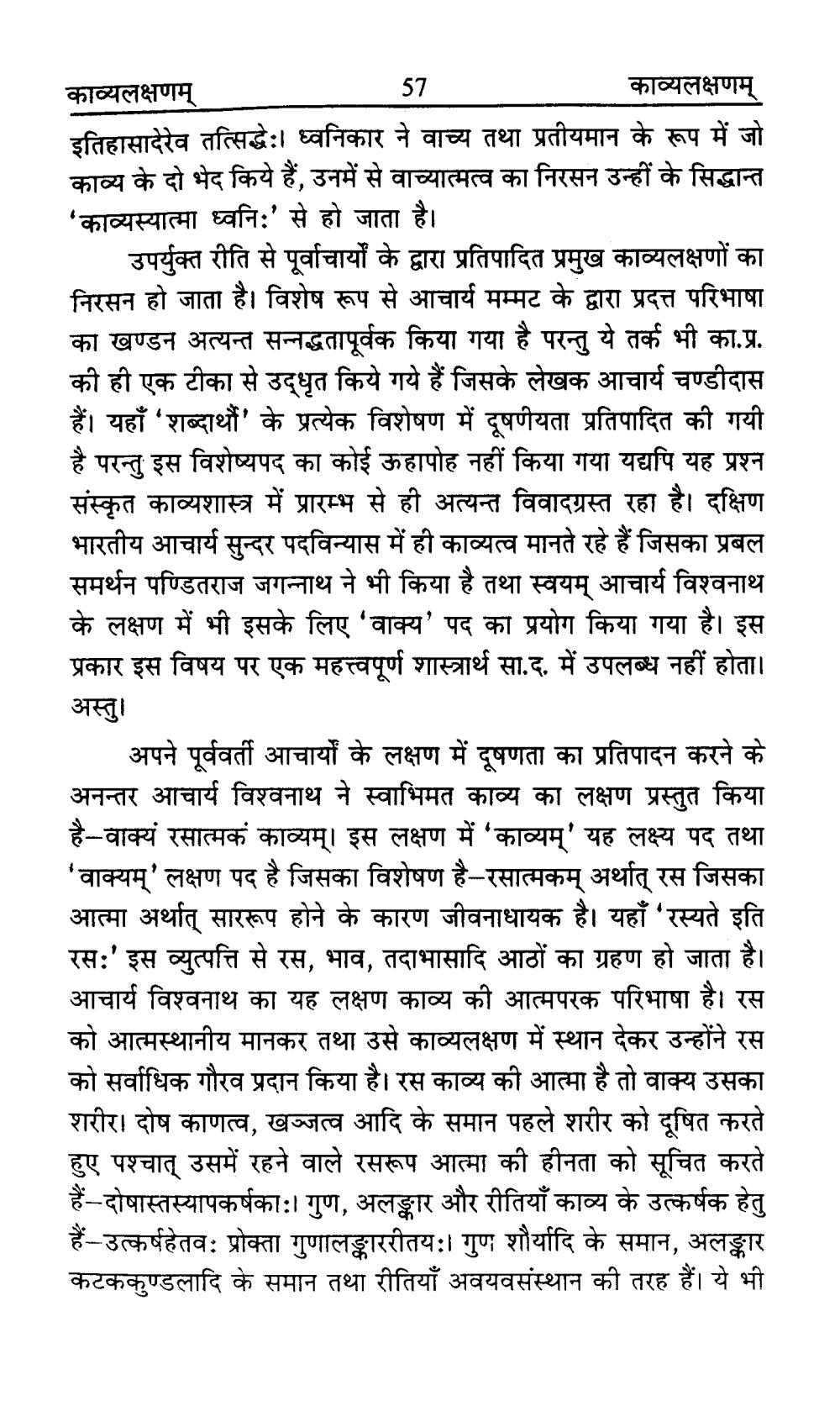________________
काव्यलक्षणम्
काव्यलक्षणम् इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः। ध्वनिकार ने वाच्य तथा प्रतीयमान के रूप में जो काव्य के दो भेद किये हैं, उनमें से वाच्यात्मत्व का निरसन उन्हीं के सिद्धान्त 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' से हो जाता है।
उपर्युक्त रीति से पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख काव्यलक्षणों का निरसन हो जाता है। विशेष रूप से आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदत्त परिभाषा का खण्डन अत्यन्त सन्नद्धतापूर्वक किया गया है परन्तु ये तर्क भी का.प्र. की ही एक टीका से उद्धृत किये गये हैं जिसके लेखक आचार्य चण्डीदास हैं। यहाँ 'शब्दार्थों' के प्रत्येक विशेषण में दूषणयता प्रतिपादित की गयी है परन्तु इस विशेष्यपद का कोई ऊहापोह नहीं किया गया यद्यपि यह प्रश्न संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रारम्भ से ही अत्यन्त विवादग्रस्त रहा है। दक्षिण भारतीय आचार्य सुन्दर पदविन्यास में ही काव्यत्व मानते रहे हैं जिसका प्रबल समर्थन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है तथा स्वयम् आचार्य विश्वनाथ के लक्षण में भी इसके लिए 'वाक्य' पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस विषय पर एक महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ सा.द. में उपलब्ध नहीं होता। अस्तु। _अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के लक्षण में दूषणता का प्रतिपादन करने के अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने स्वाभिमत काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है-वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। इस लक्षण में 'काव्यम्' यह लक्ष्य पद तथा 'वाक्यम्' लक्षण पद है जिसका विशेषण है-रसात्मकम् अर्थात् रस जिसका
आत्मा अर्थात् साररूप होने के कारण जीवनाधायक है। यहाँ 'रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति से रस, भाव, तदाभासादि आठों का ग्रहण हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ का यह लक्षण काव्य की आत्मपरक परिभाषा है। रस को आत्मस्थानीय मानकर तथा उसे काव्यलक्षण में स्थान देकर उन्होंने रस को सर्वाधिक गौरव प्रदान किया है। रस काव्य की आत्मा है तो वाक्य उसका शरीर। दोष काणत्व, खञ्जत्व आदि के समान पहले शरीर को दूषित करते हुए पश्चात् उसमें रहने वाले रसरूप आत्मा की हीनता को सूचित करते हैं-दोषास्तस्यापकर्षकाः। गुण, अलङ्कार और रीतियाँ काव्य के उत्कर्षक हेतु हैं-उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः। गुण शौर्यादि के समान, अलङ्कार कटककुण्डलादि के समान तथा रीतियाँ अवयवसंस्थान की तरह हैं। ये भी