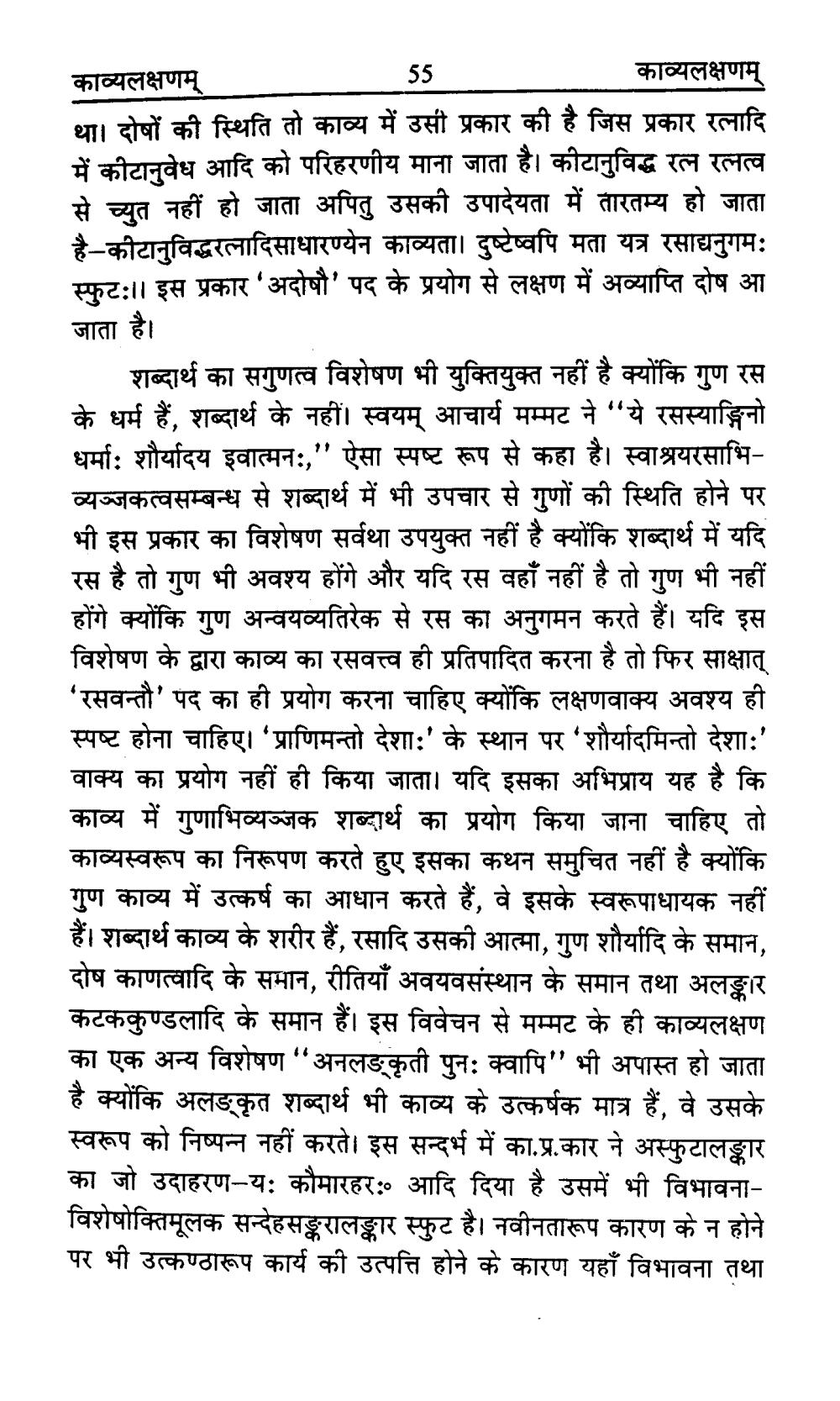________________
SS
काव्यलक्षणम्
काव्यलक्षणम् था। दोषों की स्थिति तो काव्य में उसी प्रकार की है जिस प्रकार रत्नादि में कीटानवेध आदि को परिहरणीय माना जाता है। कीटानुविद्ध रत्न रत्नत्व से च्युत नहीं हो जाता अपितु उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता है-कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसायनुगमः स्फुटः।। इस प्रकार 'अदोषौ' पद के प्रयोग से लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाता है।
शब्दार्थ का सगुणत्व विशेषण भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि गुण रस के धर्म हैं, शब्दार्थ के नहीं। स्वयम् आचार्य मम्मट ने “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः," ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्वसम्बन्ध से शब्दार्थ में भी उपचार से गुणों की स्थिति होने पर भी इस प्रकार का विशेषण सर्वथा उपयुक्त नहीं है क्योंकि शब्दार्थ में यदि रस है तो गुण भी अवश्य होंगे और यदि रस वहाँ नहीं है तो गुण भी नहीं होंगे क्योंकि गुण अन्वयव्यतिरेक से रस का अनुगमन करते हैं। यदि इस विशेषण के द्वारा काव्य का रसवत्त्व ही प्रतिपादित करना है तो फिर साक्षात् 'रसवन्तौ' पद का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि लक्षणवाक्य अवश्य ही स्पष्ट होना चाहिए। 'प्राणिमन्तो देशाः' के स्थान पर 'शौर्यादमिन्तो देशाः' वाक्य का प्रयोग नहीं ही किया जाता। यदि इसका अभिप्राय यह है कि काव्य में गुणाभिव्यञ्जक शब्दार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए तो काव्यस्वरूप का निरूपण करते हुए इसका कथन समुचित नहीं है क्योंकि गुण काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं, वे इसके स्वरूपाधायक नहीं हैं। शब्दार्थ काव्य के शरीर हैं, रसादि उसकी आत्मा, गुण शौर्यादि के समान, दोष काणत्वादि के समान, रीतियाँ अवयवसंस्थान के समान तथा अलङ्कार कटककुण्डलादि के समान हैं। इस विवेचन से मम्मट के ही काव्यलक्षण का एक अन्य विशेषण "अनलङ्कृती पुनः क्वापि" भी अपास्त हो जाता है क्योंकि अलङ्कृत शब्दार्थ भी काव्य के उत्कर्षक मात्र हैं, वे उसके स्वरूप को निष्पन्न नहीं करते। इस सन्दर्भ में का.प्र.कार ने अस्फुटालङ्कार का जो उदाहरण-यः कौमारहर: आदि दिया है उसमें भी विभावनाविशेषोक्तिमूलक सन्देहसङ्करालङ्कार स्फुट है। नवीनतारूप कारण के न होने पर भी उत्कण्ठारूप कार्य की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ विभावना तथा