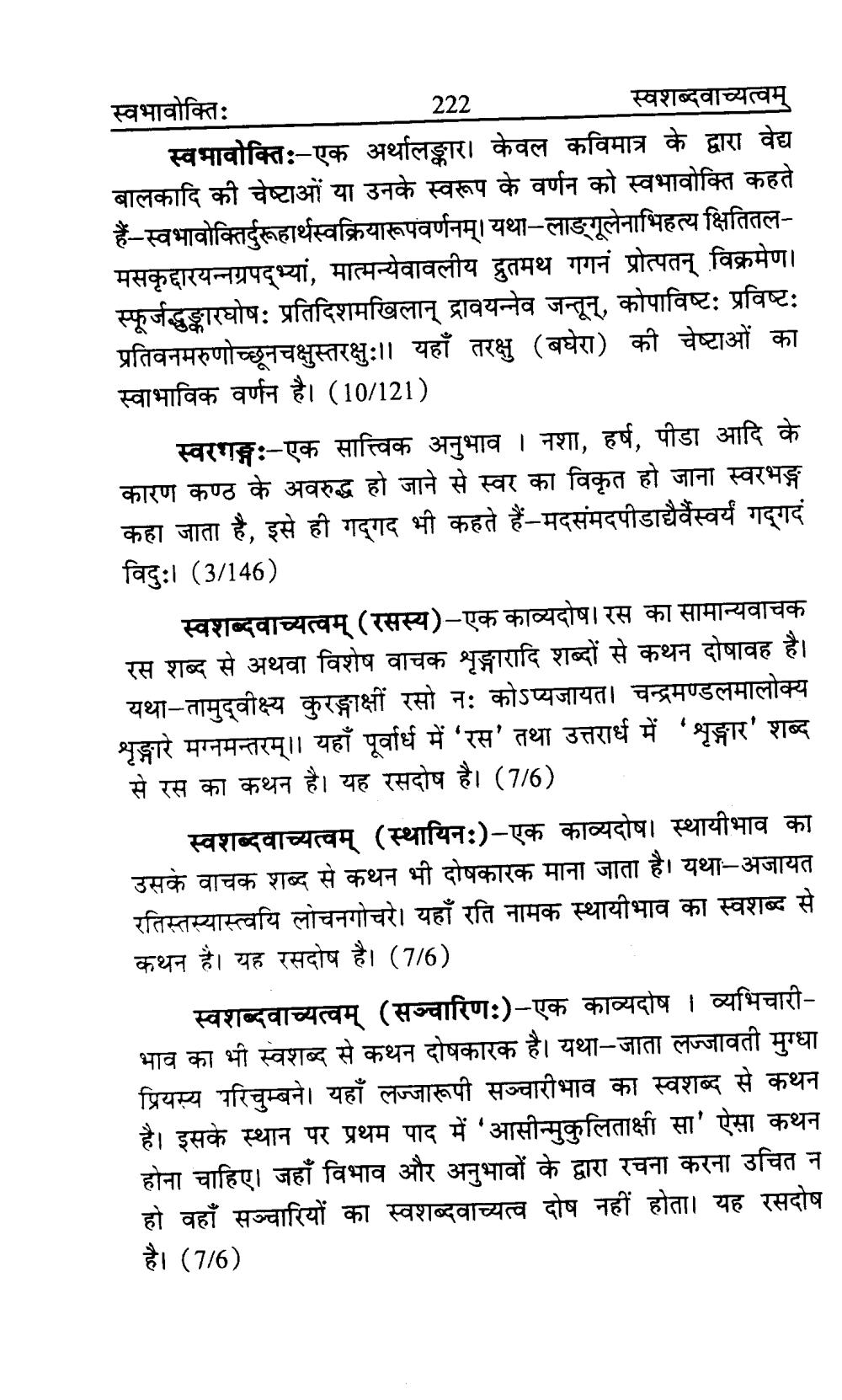________________
222
-
स्वभावोक्तिः
स्वशब्दवाच्यत्वम् स्वभावोक्तिः-एक अर्थालङ्कार। केवल कविमात्र के द्वारा वेद्य बालकादि की चेष्टाओं या उनके स्वरूप के वर्णन को स्वभावोक्ति कहते हैं-स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्। यथा-लाङ्गेलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृद्दारयन्नग्रपद्भ्यां , मात्मन्येवावलीय द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन् विक्रमेण। स्फूर्जद्धङ्कारघोषः प्रतिदिशमखिलान् द्रावयन्नेव जन्तून्, कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षुस्तरक्षुः।। यहाँ तरक्षु (बघेरा) की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन है। (10/121)
स्वरगङ्गः-एक सात्त्विक अनुभाव । नशा, हर्ष, पीडा आदि के कारण कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने से स्वर का विकृत हो जाना स्वरभङ्ग कहा जाता है, इसे ही गद्गद भी कहते हैं-मदसंमदपीडाद्यैर्वैस्वयं गद्गदं विदुः। (3/146)
स्वशब्दवाच्यत्वम् (रसस्य)-एक काव्यदोष। रस का सामान्यवाचक रस शब्द से अथवा विशेष वाचक शृङ्गारादि शब्दों से कथन दोषावह है। यथा-तामुवीक्ष्य कुरङ्गाक्षी रसो नः कोऽप्यजायत। चन्द्रमण्डलमालोक्य शृङ्गारे मग्नमन्तरम्।। यहाँ पूर्वार्ध में 'रस' तथा उत्तरार्ध में 'शृङ्गार' शब्द से रस का कथन है। यह रसदोष है। (7/6)
स्वशब्दवाच्यत्वम् (स्थायिनः)-एक काव्यदोष। स्थायीभाव का उसके वाचक शब्द से कथन भी दोषकारक माना जाता है। यथा-अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे। यहाँ रति नामक स्थायीभाव का स्वशब्द से कथन है। यह रसदोष है। (7/6)
स्वशब्दवाच्यत्वम् (सञ्चारिणः)-एक काव्यदोष । व्यभिचारीभाव का भी स्वशब्द से कथन दोषकारक है। यथा-जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने। यहाँ लज्जारूपी सञ्चारीभाव का स्वशब्द से कथन है। इसके स्थान पर प्रथम पाद में 'आसीन्मुकुलिताक्षी सा' ऐसा कथन होना चाहिए। जहाँ विभाव और अनुभावों के द्वारा रचना करना उचित न हो वहाँ सञ्चारियों का स्वशब्दवाच्यत्व दोष नहीं होता। यह रसदोष है। (7/6)