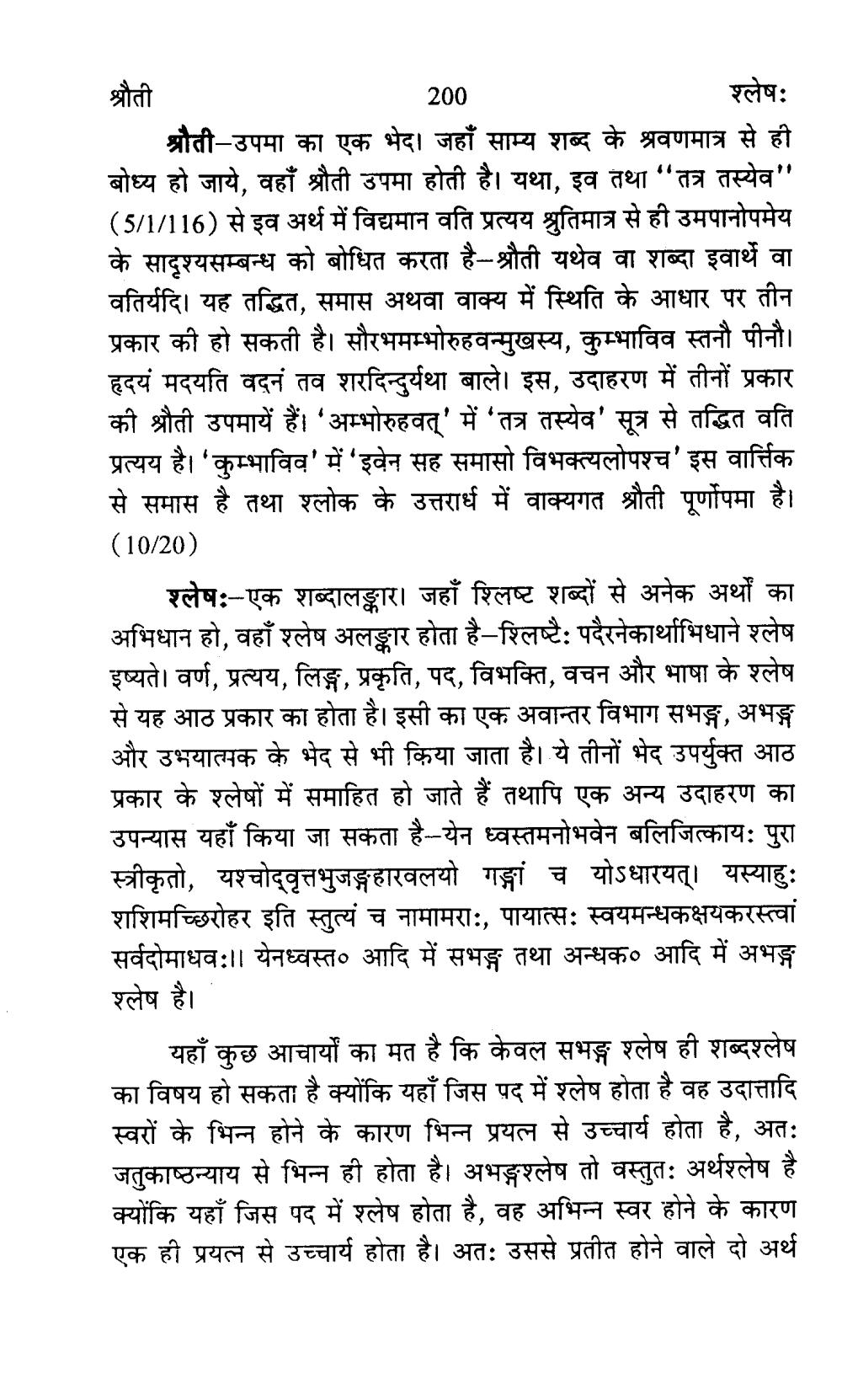________________
श्रौती
200
श्लेष :
श्रौती- उपमा का एक भेद । जहाँ साम्य शब्द के श्रवणमात्र से ही बोध्य हो जाये, वहाँ श्रौती उपमा होती है। यथा, इव तथा " तत्र तस्येव " (5/1/116) से इव अर्थ में विद्यमान वति प्रत्यय श्रुतिमात्र से ही उमपानोपमेय के सादृश्यसम्बन्ध को बोधित करता है - श्रौती यथेव वा शब्दा इवार्थे वा वतिर्यदि । यह तद्धित, समास अथवा वाक्य में स्थिति के आधार पर तीन प्रकार की हो सकती है। सौरभमम्भोरुहवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनौ । हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले। इस, उदाहरण में तीनों प्रकार की श्रौती उपमायें हैं। 'अम्भोरुहवत्' में 'तत्र तस्येव' सूत्र से तद्धित वति प्रत्यय है। 'कुम्भाविव' में 'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वार्त्तिक से समास है तथा श्लोक के उत्तरार्ध में वाक्यगत श्रौती पूर्णोपमा है। (10/20)
श्लेषः-एक शब्दालङ्कार । जहाँ श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान हो, वहाँ श्लेष अलङ्कार होता है - श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते । वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा के श्लेष से यह आठ प्रकार का होता है। इसी का एक अवान्तर विभाग सभङ्ग, अभङ्ग और उभयात्मक के भेद से भी किया जाता है। ये तीनों भेद उपर्युक्त आठ प्रकार के श्लेषों में समाहित हो जाते हैं तथापि एक अन्य उदाहरण का उपन्यास यहाँ किया जा सकता है - येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्काय: पुरा स्त्रीकृतो, यश्चोद्वृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्। यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः, पायात्सः स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः।। येनध्वस्त० आदि में सभङ्ग तथा अन्धक० आदि में अभङ्ग श्लेष है।
यहाँ कुछ आचार्यों का मत है कि केवल सभङ्ग श्लेष ही शब्दश्लेष का विषय हो सकता है क्योंकि यहाँ जिस पद में श्लेष होता है वह उदात्तादि स्वरों के भिन्न होने के कारण भिन्न प्रयत्न से उच्चार्य होता है, अतः जतुकाष्ठन्याय से भिन्न ही होता है। अभङ्गश्लेष तो वस्तुत: अर्थश्लेष है क्योंकि यहाँ जिस पद में श्लेष होता है, वह अभिन्न स्वर होने के कारण एक ही प्रयत्न से उच्चार्य होता है। अत: उससे प्रतीत होने वाले दो अर्थ