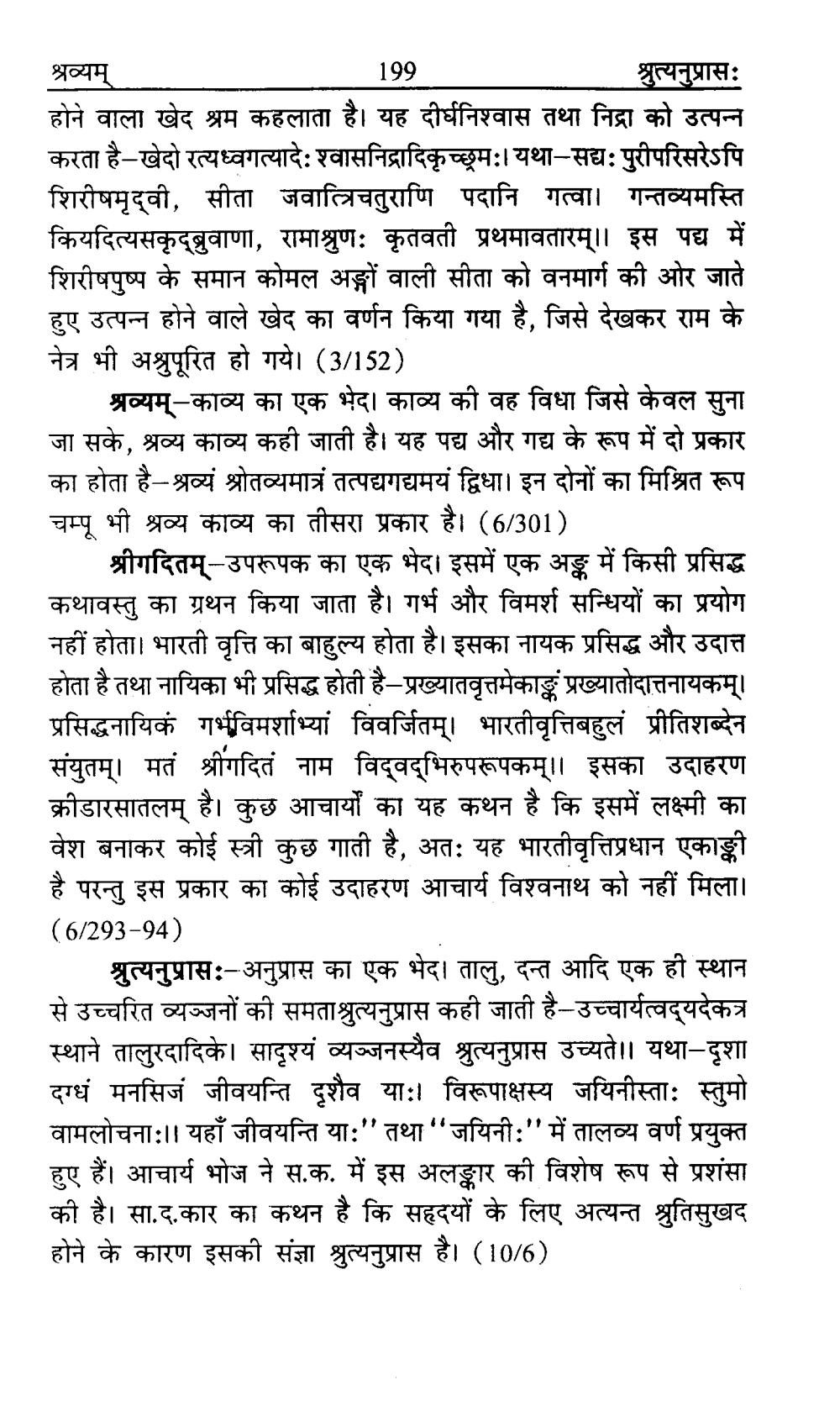________________
श्रव्यम्
199
श्रुत्यनुप्रासः होने वाला खेद श्रम कहलाता है। यह दीर्घनिश्वास तथा निद्रा को उत्पन्न करता है-खेदो रत्यध्वगत्यादे: श्वासनिद्रादिकृच्छ्रमः। यथा-सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी, सीता जवात्रिचतुराणि पदानि गत्वा। गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृब्रुवाणा, रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्।। इस पद्य में शिरीषपुष्प के समान कोमल अङ्गों वाली सीता को वनमार्ग की ओर जाते हुए उत्पन्न होने वाले खेद का वर्णन किया गया है, जिसे देखकर राम के नेत्र भी अश्रुपूरित हो गये। (3/152)
श्रव्यम्-काव्य का एक भेद। काव्य की वह विधा जिसे केवल सुना जा सके, श्रव्य काव्य कही जाती है। यह पद्य और गद्य के रूप में दो प्रकार का होता है-श्रव्यं श्रोतव्यमानं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा। इन दोनों का मिश्रित रूप चम्पू भी श्रव्य काव्य का तीसरा प्रकार है। (6/301)
श्रीगदितम्-उपरूपक का एक भेद। इसमें एक अङ्क में किसी प्रसिद्ध कथावस्तु का ग्रथन किया जाता है। गर्भ और विमर्श सन्धियों का प्रयोग नहीं होता। भारती वृत्ति का बाहुल्य होता है। इसका नायक प्रसिद्ध और उदात्त होता है तथा नायिका भी प्रसिद्ध होती है-प्रख्यातवृत्तमेकाक्प्रख्यातोदात्तनायकम्। प्रसिद्धनायिकं गर्भविमर्शाभ्यां विवर्जितम्। भारतीवृत्तिबहुलं प्रीतिशब्देन संयुतम्। मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्भिरुपरूपकम्।। इसका उदाहरण क्रीडारसातलम् है। कुछ आचार्यों का यह कथन है कि इसमें लक्ष्मी का वेश बनाकर कोई स्त्री कुछ गाती है, अतः यह भारतीवृत्तिप्रधान एकाङ्की है परन्तु इस प्रकार का कोई उदाहरण आचार्य विश्वनाथ को नहीं मिला। (6/293-94)
श्रुत्यनुप्रासः-अनुप्रास का एक भेद। तालु, दन्त आदि एक ही स्थान से उच्चरित व्यञ्जनों की समताश्रुत्यनुप्रास कही जाती है-उच्चार्यत्वद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके। सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते।। यथा-दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः। विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः।। यहाँ जीवयन्ति याः" तथा "जयिनी:" में तालव्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। आचार्य भोज ने स.क. में इस अलङ्कार की विशेष रूप से प्रशंसा की है। सा.द.कार का कथन है कि सहृदयों के लिए अत्यन्त श्रुतिसुखद होने के कारण इसकी संज्ञा श्रुत्यनुप्रास है। (10/6)