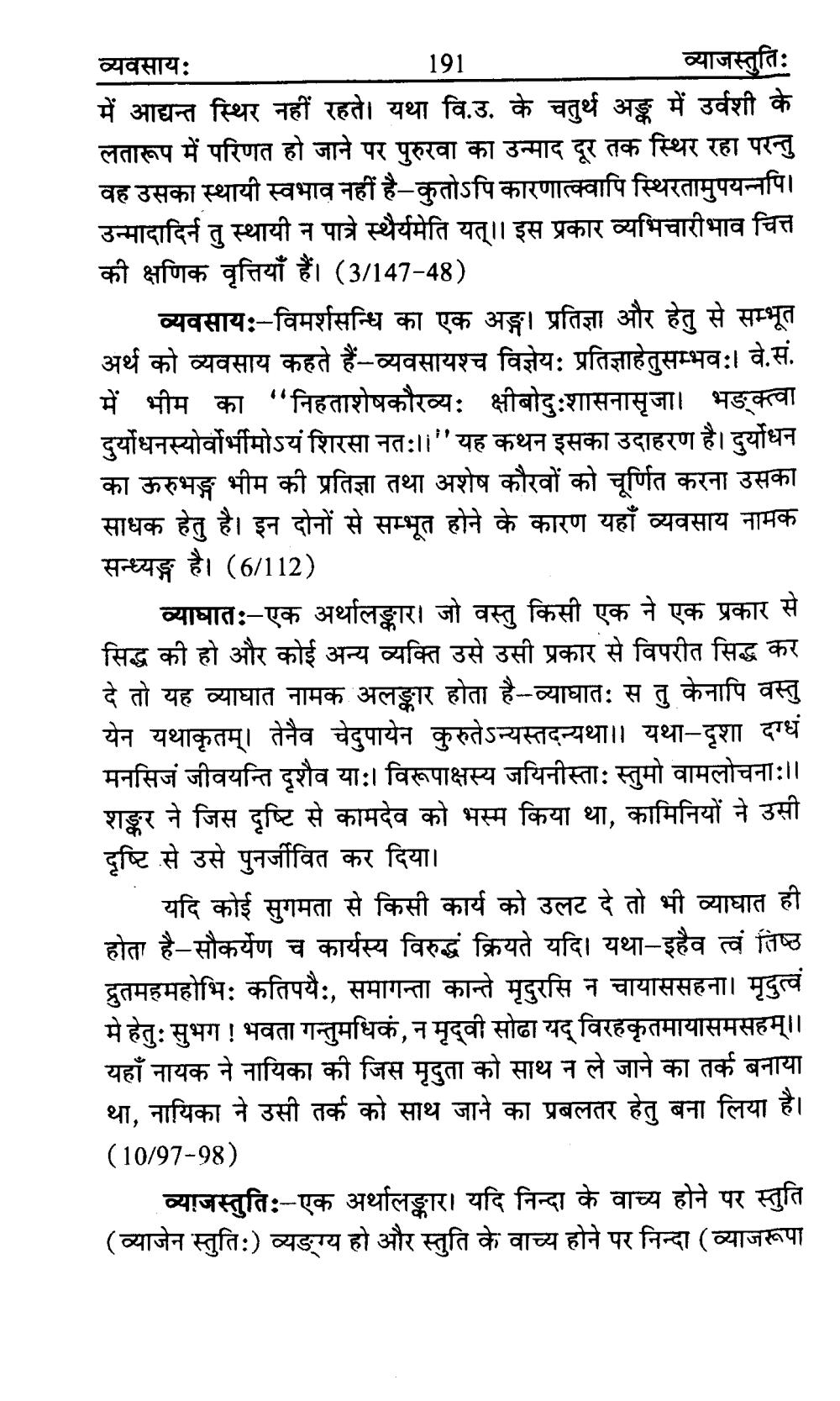________________
व्यवसायः
191
व्याजस्तुतिः
में आद्यन्त स्थिर नहीं रहते । यथा वि.उ. के चतुर्थ अङ्क में उर्वशी के लतारूप में परिणत हो जाने पर पुरुरवा का उन्माद दूर तक स्थिर रहा परन्तु वह उसका स्थायी स्वभाव नहीं है- कुतोऽपि कारणात्क्वापि स्थिरतामुपयन्नपि । उन्मादादिर्न तु स्थायी न पात्रे स्थैर्यमेति यत् । । इस प्रकार व्यभिचारी भाव चित्त की क्षणिक वृत्तियाँ हैं। (3/147-48)
व्यवसाय:- विमर्शसन्धि का एक अङ्ग । प्रतिज्ञा और हेतु से सम्भूत अर्थ को व्यवसाय कहते हैं - व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्भवः । वे.सं. में भीम का " निहताशेषकौरव्यः क्षीबोदुःशासनासृजा । भङ्क्त्वा दुर्योधनस्योर्वोर्भीमोऽयं शिरसा नतः ।। " यह कथन इसका उदाहरण है। दुर्योधन का ऊरुभङ्ग भीम की प्रतिज्ञा तथा अशेष कौरवों को चूर्णित करना उसका साधक हेतु है। इन दोनों से सम्भूत होने के कारण यहाँ व्यवसाय नामक सन्ध्यङ्ग है। (6/112)
व्याघातः-एक अर्थालङ्कार । जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध की हो और कोई अन्य व्यक्ति उसे उसी प्रकार से विपरीत सिद्ध कर दे तो यह व्याघात नामक अलङ्कार होता है- व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम् । तेनैव चेदुपायेन कुरुतेऽन्यस्तदन्यथा । । यथा दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः । विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ।। शङ्कर ने जिस दृष्टि से कामदेव को भस्म किया था, कामिनियों ने उसी दृष्टि से उसे पुनर्जीवित कर दिया।
यदि कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे तो भी व्याघात ही होता है - सौकर्येण च कार्यस्य विरुद्धं क्रियते यदि । यथा - इहैव त्वं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयैः समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना । मृदुत्वं मेहेतुः सुभग ! भवता गन्तुमधिकं, न मृद्वी सोढा यद् विरहकृतमायासमसहम्।। यहाँ नायक ने नायिका की जिस मृदुता को साथ न ले जाने का तर्क बनाया था, नायिका ने उसी तर्क को साथ जाने का प्रबलतर हेतु बना लिया है। (10/97-98)
व्याजस्तुति:- एक अर्थालङ्कार । यदि निन्दा के वाच्य होने पर स्तुति ( व्याजेन स्तुति:) व्यङ्ग्य हो और स्तुति के वाच्य होने पर निन्दा ( व्याजरूपा