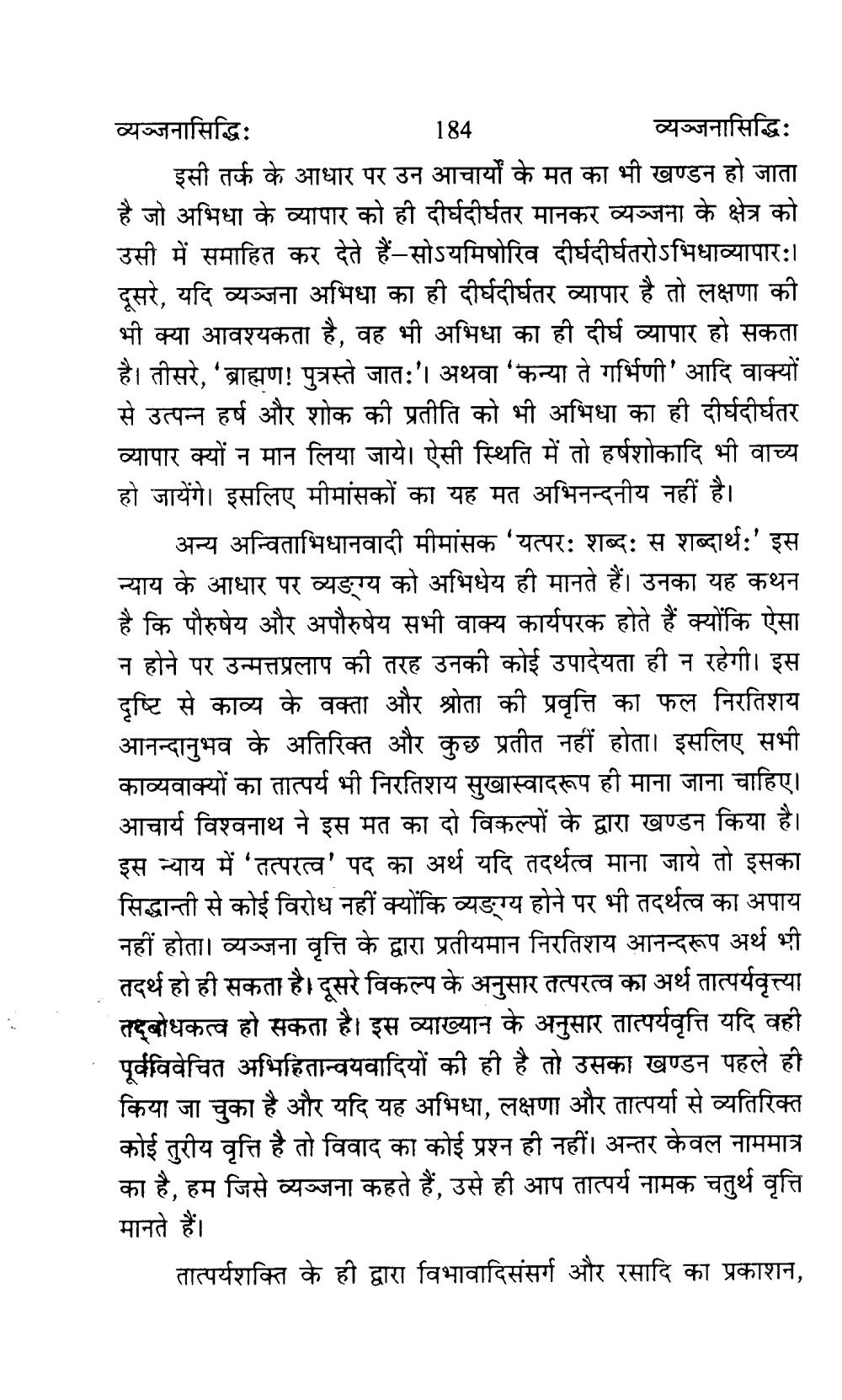________________
व्यञ्जनासिद्धिः
184
व्यञ्जनासिद्धिः
इसी तर्क के आधार पर उन आचार्यों के मत का भी खण्डन हो जाता है जो अभिधा के व्यापार को ही दीर्घदीर्घतर मानकर व्यञ्जना के क्षेत्र को उसी में समाहित कर देते हैं- सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः । दूसरे, यदि व्यञ्जना अभिधा का ही दीर्घदीर्घतर व्यापार है तो लक्षणा की भी क्या आवश्यकता है, वह भी अभिधा का ही दीर्घ व्यापार हो सकता है । तीसरे, 'ब्राह्मण! पुत्रस्ते जातः'। अथवा 'कन्या ते गर्भिणी' आदि वाक्यों से उत्पन्न हर्ष और शोक की प्रतीति को भी अभिधा का ही दीर्घदीर्घतर व्यापार क्यों न मान लिया जाये। ऐसी स्थिति में तो हर्षशोकादि भी वाच्य हो जायेंगे। इसलिए मीमांसकों का यह मत अभिनन्दनीय नहीं है।
अन्य अन्विताभिधानवादी मीमांसक 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः ' इस न्याय के आधार पर व्यङ्ग्य को अभिधेय ही मानते हैं। उनका यह कथन है कि पौरुषेय और अपौरुषेय सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं क्योंकि ऐसा न होने पर उन्मत्तप्रलाप की तरह उनकी कोई उपादेयता ही न रहेगी। इस दृष्टि से काव्य के वक्ता और श्रोता की प्रवृत्ति का फल निरतिशय आनन्दानुभव के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। इसलिए सभी काव्यवाक्यों का तात्पर्य भी निरतिशय सुखास्वादरूप ही माना जाना चाहिए । आचार्य विश्वनाथ ने इस मत का दो विकल्पों के द्वारा खण्डन किया है। इस न्याय में 'तत्परत्व' पद का अर्थ यदि तदर्थत्व माना जाये तो इसका सिद्धान्ती से कोई विरोध नहीं क्योंकि व्यङ्ग्य होने पर भी तदर्थत्व का अपाय नहीं होता। व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा प्रतीयमान निरतिशय आनन्दरूप अर्थ भी तदर्थ हो ही सकता है। दूसरे विकल्प के अनुसार तत्परत्व का अर्थ तात्पर्यवृत्त्या तद्बोधकत्व हो सकता है। इस व्याख्यान के अनुसार तात्पर्यवृत्ति यदि वही पूर्वविवेचित अभिहितान्वयवादियों की ही है तो उसका खण्डन पहले ही किया जा चुका है और यदि यह अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या से व्यतिरिक्त कोई तुरीय वृत्ति है तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं । अन्तर केवल नाममात्र का है, हम जिसे व्यञ्जना कहते हैं, उसे ही आप तात्पर्य नामक चतुर्थ वृत्ति मानते हैं।
तात्पर्यशक्ति के ही द्वारा विभावादिसंसर्ग और रसादि का प्रकाशन,