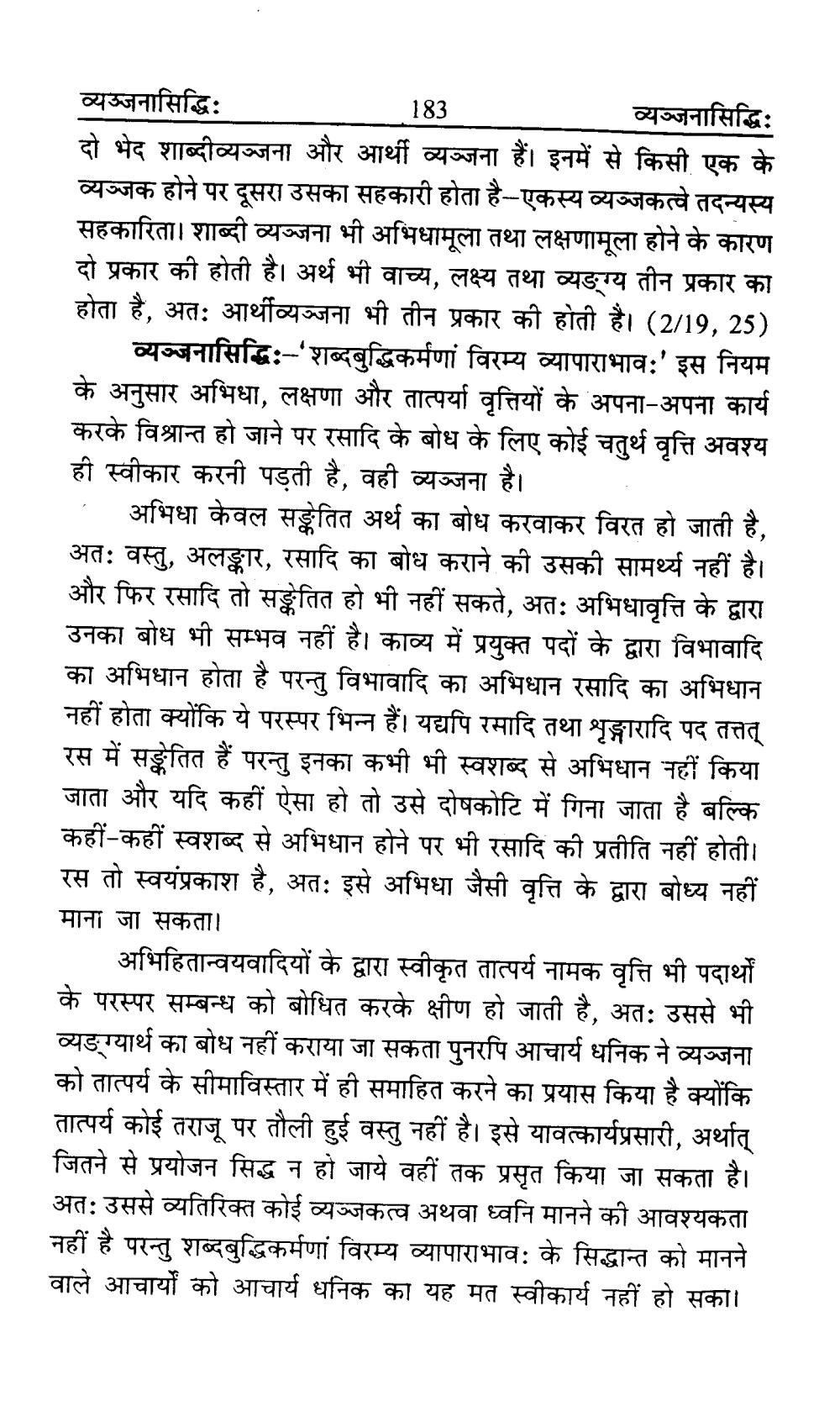________________
183
व्यञ्जनासिद्धिः
व्यञ्जनासिद्धिः दो भेद शाब्दीव्यञ्जना और आर्थी व्यञ्जना हैं। इनमें से किसी एक के व्यञ्जक होने पर दूसरा उसका सहकारी होता है-एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। शाब्दी व्यञ्जना भी अभिधामूला तथा लक्षणामूला होने के कारण दो प्रकार की होती है। अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य तीन प्रकार का होता है, अतः आर्थीव्यञ्जना भी तीन प्रकार की होती है। (2/19, 25)
व्यञ्जनासिद्धिः-'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः' इस नियम के अनुसार अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या वृत्तियों के अपना-अपना कार्य करके विश्रान्त हो जाने पर रसादि के बोध के लिए कोई चतुर्थ वृत्ति अवश्य ही स्वीकार करनी पड़ती है, वही व्यञ्जना है।। - अभिधा केवल सङ्केतित अर्थ का बोध करवाकर विरत हो जाती है, अतः वस्तु, अलङ्कार, रसादि का बोध कराने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। और फिर रसादि तो सङ्केतित हो भी नहीं सकते, अत: अभिधावृत्ति के द्वारा उनका बोध भी सम्भव नहीं है। काव्य में प्रयुक्त पदों के द्वारा विभावादि का अभिधान होता है परन्तु विभावादि का अभिधान रसादि का अभिधान नहीं होता क्योंकि ये परस्पर भिन्न हैं। यद्यपि रसादि तथा शृङ्गारादि पद तत्तत् रस में सङ्केतित हैं परन्तु इनका कभी भी स्वशब्द से अभिधान नहीं किया जाता और यदि कहीं ऐसा हो तो उसे दोषकोटि में गिना जाता है बल्कि कहीं-कहीं स्वशब्द से अभिधान होने पर भी रसादि की प्रतीति नहीं होती। रस तो स्वयंप्रकाश है, अतः इसे अभिधा जैसी वृत्ति के द्वारा बोध्य नहीं माना जा सकता।
अभिहितान्वयवादियों के द्वारा स्वीकृत तात्पर्य नामक वृत्ति भी पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध को बोधित करके क्षीण हो जाती है, अतः उससे भी व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं कराया जा सकता पुनरपि आचार्य धनिक ने व्यञ्जना को तात्पर्य के सीमाविस्तार में ही समाहित करने का प्रयास किया है क्योंकि तात्पर्य कोई तराजू पर तौली हुई वस्तु नहीं है। इसे यावत्कार्यप्रसारी, अर्थात् जितने से प्रयोजन सिद्ध न हो जाये वहीं तक प्रसृत किया जा सकता है। अत: उससे व्यतिरिक्त कोई व्यञ्जकत्व अथवा ध्वनि मानने की आवश्यकता नहीं है परन्तु शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः के सिद्धान्त को मानने वाले आचार्यों को आचार्य धनिक का यह मत स्वीकार्य नहीं हो सका।