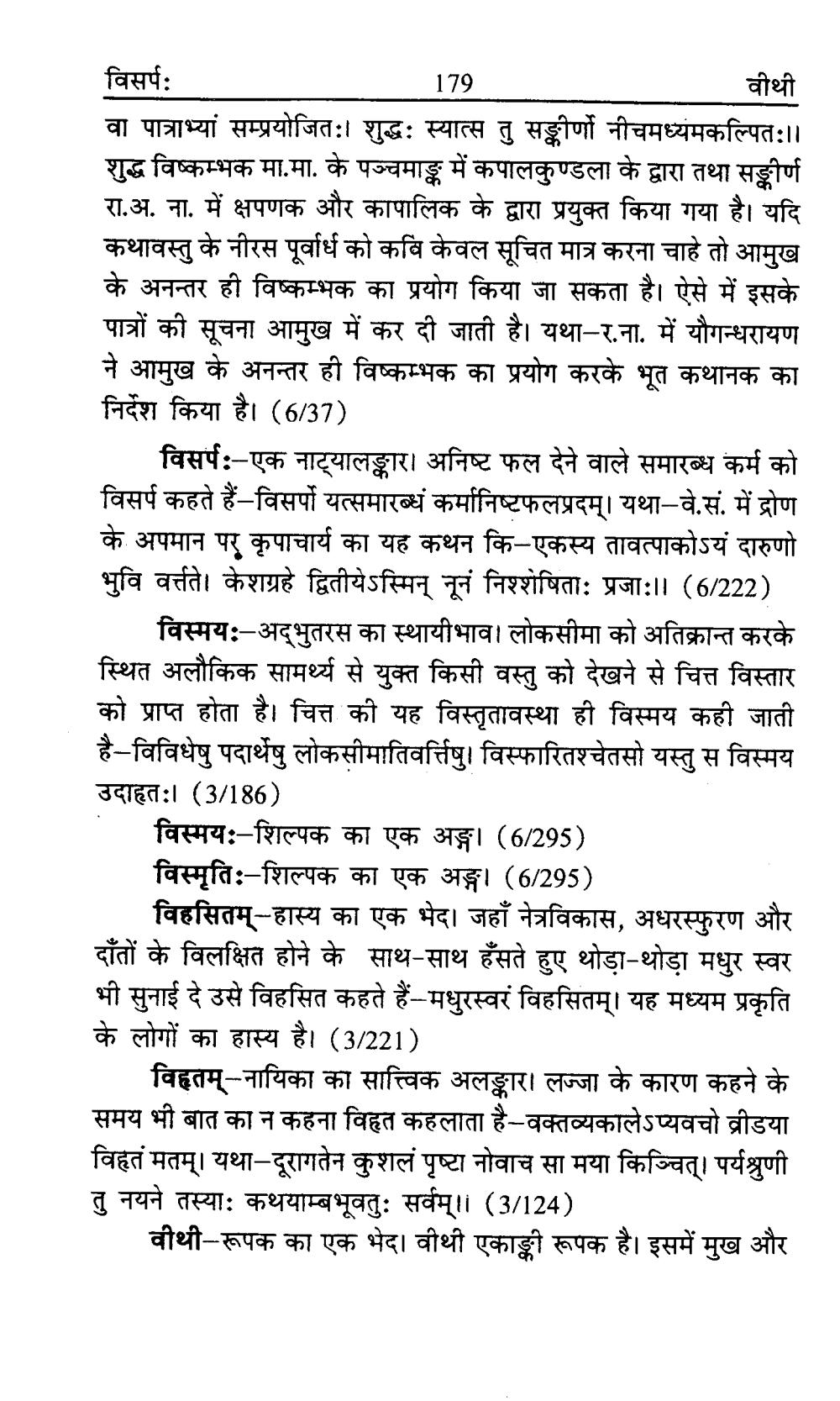________________
विसर्पः
वीथी
179
वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात्स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः।। शुद्ध विष्कम्भक मा.मा. के पञ्चमाङ्क में कपालकुण्डला के द्वारा तथा सङ्कीर्ण रा.अ. ना. में क्षपणक और कापालिक के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। यदि कथावस्तु के नीरस पूर्वार्ध को कवि केवल सूचित मात्र करना चाहे तो आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में इसके पात्रों की सूचना आमुख में कर दी जाती है । यथा - र.ना. में यौगन्धरायण ने आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक का प्रयोग करके भूत कथानक का निर्देश किया है। (6/37)
विसर्प :- एक नाट्यालङ्कार। अनिष्ट फल देने वाले समारब्ध कर्म को विसर्प कहते हैं-विसर्पो यत्समारब्धं कर्मानिष्टफलप्रदम् । यथा - वे.सं. में द्रोण के अपमान पर कृपाचार्य का यह कथन कि- एकस्य तावत्पाकोऽयं दारुणो भुवि वर्त्तते । केशग्रहे द्वितीयेऽस्मिन् नूनं निश्शेषिता: प्रजा: ।। ( 6 / 222)
विस्मय:- अद्भुतरस का स्थायीभाव | लोकसीमा को अतिक्रान्त करके स्थित अलौकिक सामर्थ्य से युक्त किसी वस्तु को देखने से चित्त विस्तार को प्राप्त होता है । चित्त की यह विस्तृतावस्था ही विस्मय कही जाती है - विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्त्तिषु । विस्फारितश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृत:। (3/186)
विस्मय:- शिल्पक का एक अङ्ग । (6/295) विस्मृति:- शिल्पक का एक अङ्ग । (6/295)
विहसितम् - हास्य का एक भेद । जहाँ नेत्रविकास, अधरस्फुरण और दाँतों के विलक्षित होने के साथ-साथ हँसते हुए थोड़ा-थोड़ा मधुर स्वर भी सुनाई दे उसे विहसित कहते हैं- मधुरस्वरं विहसितम् | यह मध्यम प्रकृति के लोगों का हास्य है । (3/221)
विहृतम् - नायिका का सात्त्विक अलङ्कार | लज्जा के कारण कहने के समय भी बात का न कहना विहृत कहलाता है-वक्तव्यकालेऽप्यवचो व्रीडया विहृतं मतम् । यथा- दूरागतेन कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किञ्चित् । पर्यश्रुणी तु नयने तस्याः कथयाम्बभूवतुः सर्वम् ।। (3/124)
वीथी - रूपक का एक भेद । वीथी एकाङ्की रूपक है। इसमें मुख और