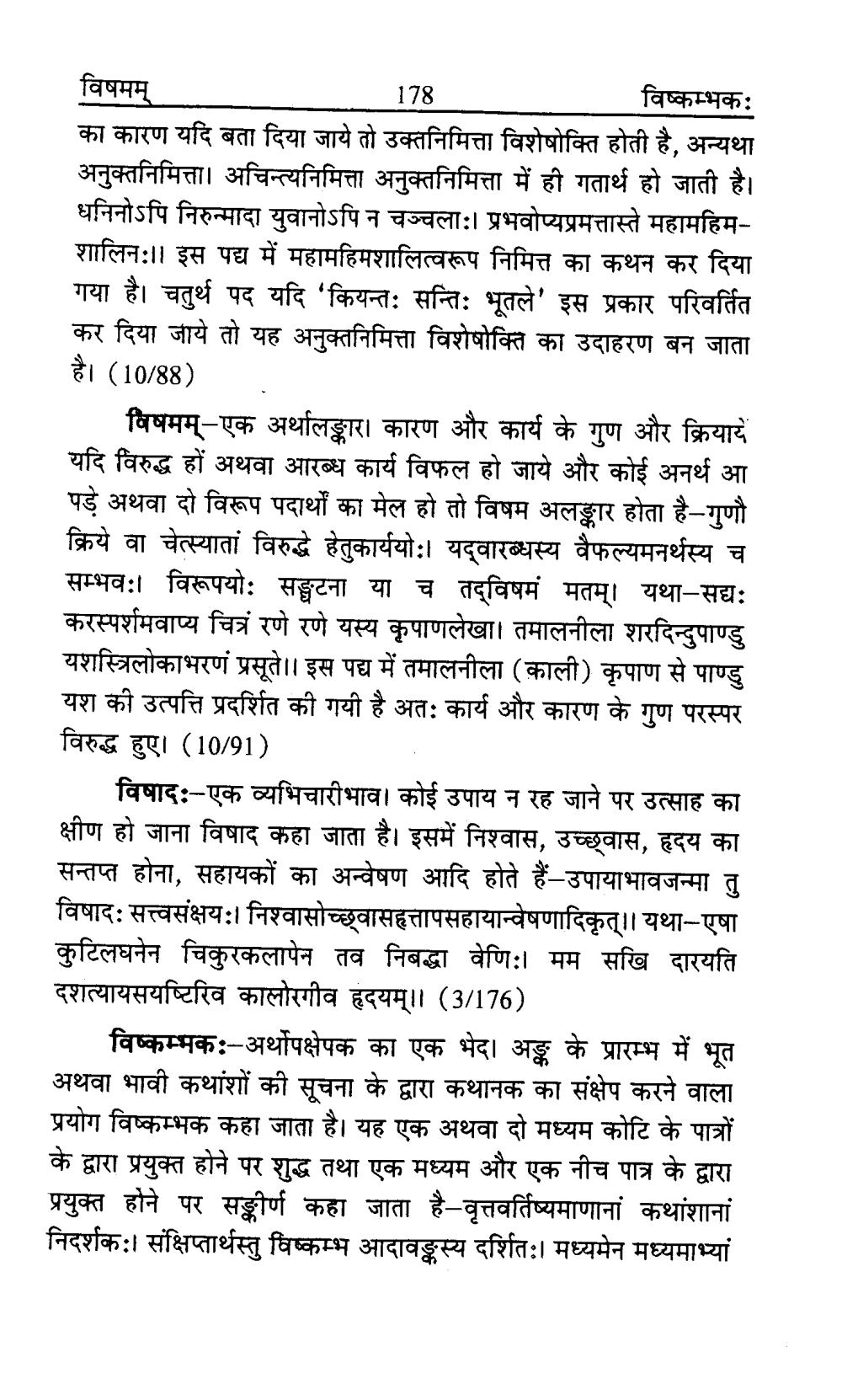________________
विषमम्
178
विष्कम्भकः
का कारण यदि बता दिया जाये तो उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है, अन्यथा अनुक्तनिमित्ता । अचिन्त्यनिमित्ता अनुक्तनिमित्ता में ही गतार्थ हो जाती है। धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः । प्रभवोप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः || इस पद्य में महामहिमशालित्वरूप निमित्त का कथन कर दिया गया है। चतुर्थ पद यदि 'कियन्तः सन्तिः भूतले' इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाये तो यह अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण बन जाता है। ( 10/88)
विषमम् - एक अर्थालङ्कार। कारण और कार्य के गुण और क्रियायें यदि विरुद्ध हों अथवा आरब्ध कार्य विफल हो जाये और कोई अनर्थ आ पड़े अथवा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो विषम अलङ्कार होता है - गुणौ क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः । यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च सम्भवः । विरूपयोः सङ्घटना या च तद्विषमं मतम् । यथा-सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोकाभरणं प्रसूते । । इस पद्य में तमालनीला (काली) कृपाण से पाण्डु यश की उत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है अतः कार्य और कारण के गुण परस्पर विरुद्ध हुए। (10/91)
विषादः - एक व्यभिचारी भाव। कोई उपाय न रह जाने पर उत्साह का क्षीण हो जाना विषाद कहा जाता है। इसमें निश्वास, उच्छ्वास, हृदय का सन्तप्त होना, सहायकों का अन्वेषण आदि होते हैं- उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसंक्षयः। निश्वासोच्छ्वासहृत्तापसहायान्वेषणादिकृत् ।। यथा - एषा कुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेणिः । मम सखि दारयति दशत्यायसयष्टिरिव कालोरगीव हृदयम् ।। (3/176)
विष्कम्भकः-अर्थोपक्षेपक का एक भेद । अङ्क के प्रारम्भ में भूत अथवा भावी कथांशों की सूचना के द्वारा कथानक का संक्षेप करने वाला प्रयोग विष्कम्भक कहा जाता है। यह एक अथवा दो मध्यम कोटि के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त होने पर शुद्ध तथा एक मध्यम और एक नीच पात्र के द्वारा प्रयुक्त होने पर सङ्कीर्ण कहा जाता है- वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः । मध्यमेन मध्यमाभ्यां