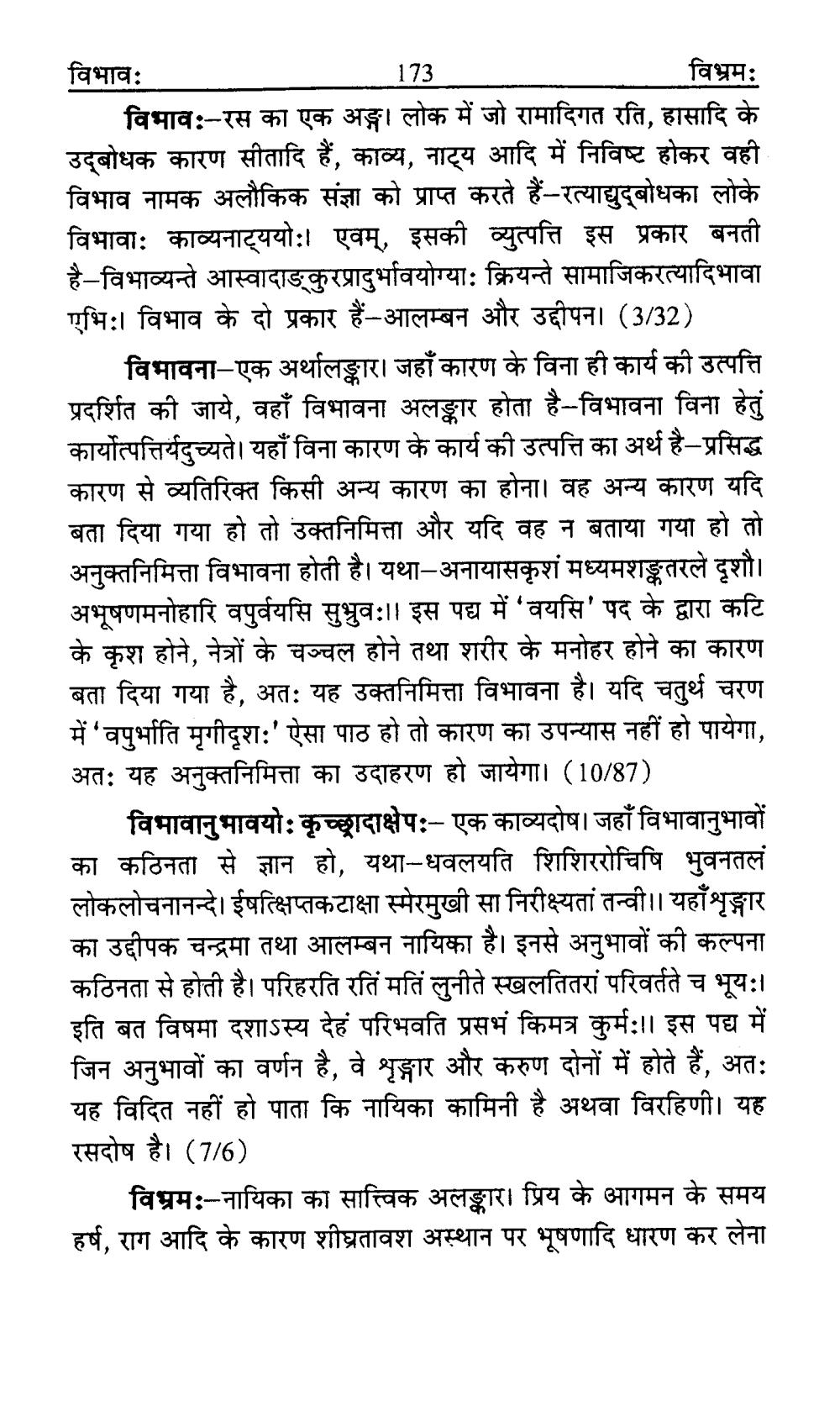________________
विभावः
173
विभ्रमः विभाव:-रस का एक अङ्ग। लोक में जो रामादिगत रति, हासादि के उद्बोधक कारण सीतादि हैं, काव्य, नाट्य आदि में निविष्ट होकर वही विभाव नामक अलौकिक संज्ञा को प्राप्त करते हैं-रत्याधुबोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः। एवम्, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बनती है-विभाव्यन्ते आस्वादाकुरप्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभिः। विभाव के दो प्रकार हैं-आलम्बन और उद्दीपन। (3/32)
विभावना-एक अर्थालङ्कार। जहाँ कारण के विना ही कार्य की उत्पत्ति प्रदर्शित की जाये, वहाँ विभावना अलङ्कार होता है-विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। यहाँ विना कारण के कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है-प्रसिद्ध कारण से व्यतिरिक्त किसी अन्य कारण का होना। वह अन्य कारण यदि बता दिया गया हो तो उक्तनिमित्ता और यदि वह न बताया गया हो तो अनुक्तनिमित्ता विभावना होती है। यथा-अनायासकृशं मध्यमशङ्कतरले दृशौ। अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुभ्रवः।। इस पद्य में 'वयसि' पद के द्वारा कटि के कृश होने, नेत्रों के चञ्चल होने तथा शरीर के मनोहर होने का कारण बता दिया गया है, अत: यह उक्तनिमित्ता विभावना है। यदि चतुर्थ चरण में वपुर्भाति मृगीदृशः' ऐसा पाठ हो तो कारण का उपन्यास नहीं हो पायेगा, अतः यह अनुक्तनिमित्ता का उदाहरण हो जायेगा। (10/87)
विभावानुभावयोः कृच्छादाक्षेपः- एक काव्यदोष। जहाँ विभावानुभावों का कठिनता से ज्ञान हो, यथा-धवलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे। ईषत्क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्वी।। यहाँशृङ्गार का उद्दीपक चन्द्रमा तथा आलम्बन नायिका है। इनसे अनुभावों की कल्पना कठिनता से होती है। परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलतितरां परिवर्तते च भूयः। इति बत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुर्मः।। इस पद्य में जिन अनुभावों का वर्णन है, वे शृङ्गार और करुण दोनों में होते हैं, अतः यह विदित नहीं हो पाता कि नायिका कामिनी है अथवा विरहिणी। यह रसदोष है। (7/6)
विभ्रमः-नायिका का सात्त्विक अलङ्कार। प्रिय के आगमन के समय हर्ष, राग आदि के कारण शीघ्रतावश अस्थान पर भूषणादि धारण कर लेना