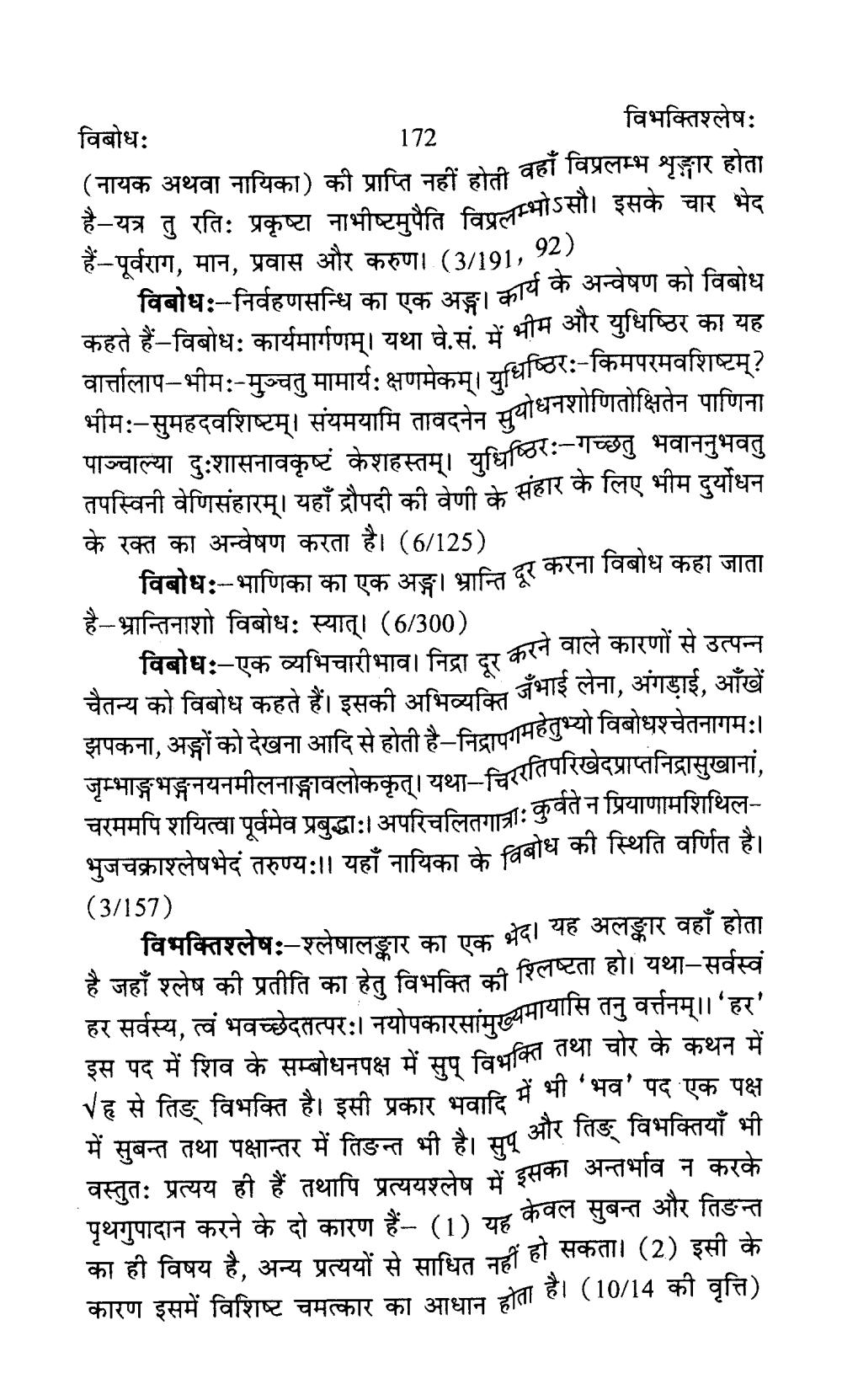________________
विबोध:
विभक्तिश्लेषः
172
(नायक अथवा नायिका) की प्राप्ति नहीं होती वहाँ विप्रलम्भ शृङ्गार होता है-यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ । इसके चार भेद हैं- पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण । (3 / 191,
92)
विबोधः-निर्वहणसन्धि का एक अङ्ग । कार्य के अन्वेषण को विबोध कहते हैं—विबोधः कार्यमार्गणम् । यथा वे.सं. में भीम और युधिष्ठिर का यह वार्त्तालाप - भीम: - मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्। युधिष्ठिरः- किमपरमवशिष्टम् ? भीमः-सुमहदवशिष्टम्। संयमयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्। युधिष्ठिरः- गच्छतु भवाननुभवतु तपस्विनी वेणिसंहारम्। यहाँ द्रौपदी की वेणी के संहार के लिए भीम दुर्योधन के रक्त का अन्वेषण करता है । (6/125)
विबोधः-भाणिका का एक अङ्ग । भ्रान्ति दूर करना विबोध कहा जाता है - भ्रान्तिनाशो विबोध: स्यात् । (6/300)
विबोधः-एक व्यभिचारीभाव । निद्रा दर करने वाले कारणों से उत्पन्न चैतन्य को विबोध कहते हैं। इसकी अभिव्यक्ति जँभाई लेना, अंगड़ाई, आँखें झपकना, अङ्गों को देखना आदि से होती है-निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागमः। जृम्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत्। यथा-चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां, चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः। अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणामशिथिलभुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्यः।। यहाँ नायिका के विबोध की स्थिति वर्णित है। (3/157)
विभक्तिश्लेष :- श्लेषालङ्कार का एक भेद। यह अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ श्लेष की प्रतीति का हेतु विभक्ति की श्लिष्टता हो। यथा-सर्वस्वं हर सर्वस्य, त्वं भवच्छेदतत्परः । नयोपकारसांमुख्यमायासि तनु वर्त्तनम्।। 'हर' इस पद में शिव के सम्बोधनपक्ष में सुप् विभक्ति तथा चोर के कथन में √हृ से तिङ् विभक्ति है। इसी प्रकार भवादि में भी 'भव' पद एक पक्ष और तिङ् विभक्तियाँ भी में सुबन्त तथा पक्षान्तर में तिङन्त भी है। सुप् वस्तुतः प्रत्यय ही हैं तथापि प्रत्ययश्लेष में इसका अन्तर्भाव न करके केवल सुबन्त और तिङन्त पृथगुपादान करने के दो कारण हैं- (1) यह का ही विषय है, अन्य प्रत्ययों से साधित नहीं हो सकता। (2) इसी के कारण इसमें विशिष्ट चमत्कार का आधान होता है। ( 10/14 की वृत्ति)