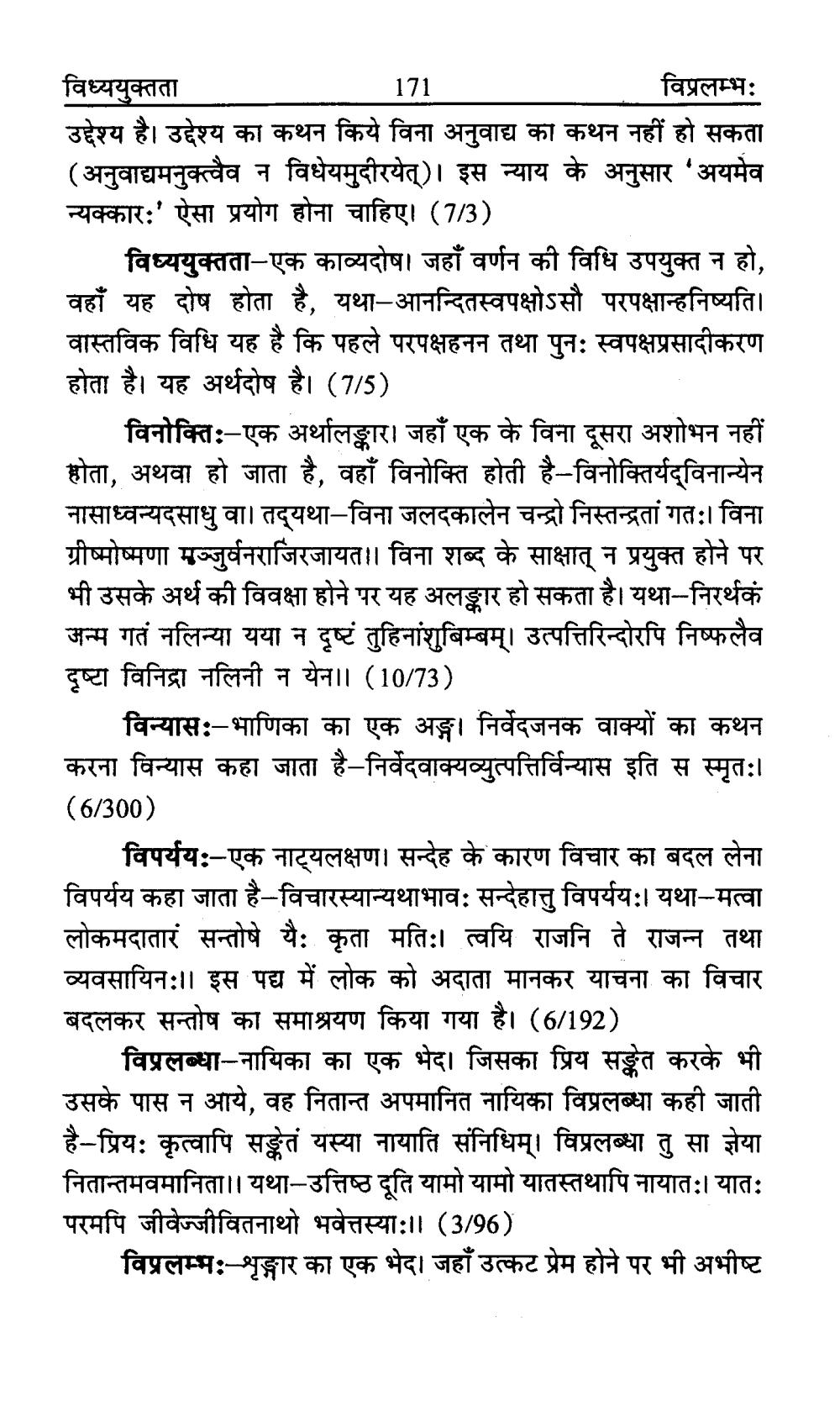________________
विध्ययुक्तता
171
विप्रलम्भ:
उद्देश्य है। उद्देश्य का कथन किये विना अनुवाद्य का कथन नहीं हो सकता (अनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत् ) । इस न्याय के अनुसार 'अयमेव न्यक्कार:' ऐसा प्रयोग होना चाहिए। (7/3)
विध्ययुक्तता - एक काव्यदोष । जहाँ वर्णन की विधि उपयुक्त न हो, वहाँ यह दोष होता है, यथा-आनन्दितस्वपक्षोऽसौ परपक्षान्हनिष्यति । वास्तविक विधि यह है कि पहले परपक्षहनन तथा पुन: स्वपक्षप्रसादीकरण होता है। यह अर्थदोष है । (7/5)
विनोक्तिः - एक अर्थालङ्कार । जहाँ एक के विना दूसरा अशोभन नहीं होता, अथवा हो जाता है, वहाँ विनोक्ति होती है- विनोक्तिर्यद्विनान्येन नासाध्वन्यदसाधु वा । तद्यथा - विना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः । विना ग्रीष्मोष्मणा मञ्जुर्वनराजिरजायत ।। विना शब्द के साक्षात् न प्रयुक्त होने पर भी उसके अर्थ की विवक्षा होने पर यह अलङ्कार हो सकता है । यथा-निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम् । उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ।। ( 10/73)
विन्यास:- भाणिका का एक अङ्ग । निर्वेदजनक वाक्यों का कथन करना विन्यास कहा जाता है - निर्वेदवाक्यव्युत्पत्तिर्विन्यास इति स स्मृतः । (6/300)
विपर्ययः- एक नाट्यलक्षण । सन्देह के कारण विचार का बदल लेना विपर्यय कहा जाता है-विचारस्यान्यथाभावः सन्देहात्तु विपर्ययः । यथा - मत्वा लोकमदातारं सन्तोषे यैः कृता मतिः । त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः । । इस पद्य में लोक को अदाता मानकर याचना का विचार बदलकर सन्तोष का समाश्रयण किया गया है। (6/192)
विप्रलब्धा - नायिका का एक भेद । जिसका प्रिय सङ्केत करके भी उसके पास न आये, वह नितान्त अपमानित नायिका विप्रलब्धा कही जाती है- प्रियः कृत्वापि सङ्केतं यस्या नायाति संनिधिम्। विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता।। यथा-उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः। यातः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ।। (3/96)
विप्रलम्भ: शृङ्गार का एक भेद । जहाँ उत्कट प्रेम होने पर भी अभीष्ट