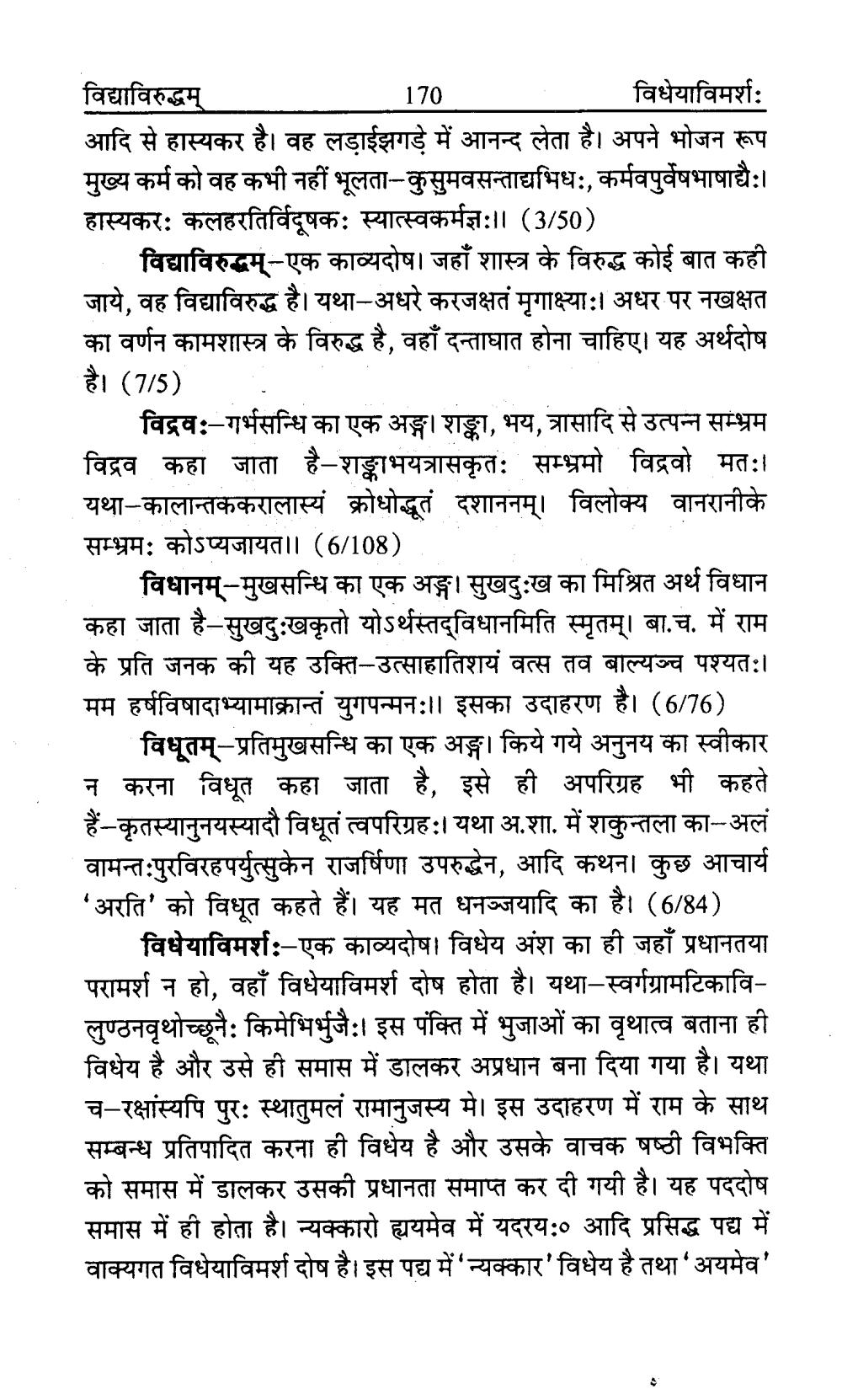________________
विद्याविरुद्धम्
170
विधेयाविमर्शः
आदि से हास्यकर है। वह लड़ाईझगड़े में आनन्द लेता है। अपने भोजन रूप मुख्य कर्म को वह कभी नहीं भूलता - कुसुमवसन्ताद्यभिधः, कर्मवपुर्वेष भाषाद्यैः । हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः || ( 3 / 50 )
विद्याविरुद्धम् - एक काव्यदोष । जहाँ शास्त्र के विरुद्ध कोई बात कही जाये, वह विद्याविरुद्ध है। यथा-अधरे करजक्षतं मृगाक्ष्याः । अधर पर नखक्षत का वर्णन कामशास्त्र के विरुद्ध है, वहाँ दन्ताघात होना चाहिए। यह अर्थदोष है। (715)
विद्रवः - गर्भसन्धि का एक अङ्ग । शङ्का, भय, त्रासादि से उत्पन्न सम्भ्रम विद्रव कहा जाता है- शङ्काभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः । यथा-कालान्तककरालास्यं क्रोधोद्धूतं दशाननम् । विलोक्य वानरानीके सम्भ्रमः कोऽप्यजायत ।। ( 6 / 108)
विधानम् - मुखसन्धि का एक अङ्ग । सुखदुःख का मिश्रित अर्थ विधान कहा जाता है- सुखदुःखकृतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम्। बा.च. में राम के प्रति जनक की यह उक्ति - उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यञ्च पश्यतः । मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः । । इसका उदाहरण है। (6/76)
विधूतम् - प्रतिमुखसन्धि का एक अङ्ग । किये गये अनुनय का स्वीकार न करना विधूत कहा जाता है, इसे ही अपरिग्रह भी कहते हैं- कृतस्यानुनयस्यादौ विधूतं त्वपरिग्रहः। यथा अ.शा. में शकुन्तला का-- - अलं वामन्तःपुरविरहपर्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन, आदि कथन। कुछ आचार्य 'अरति' को विधूत कहते हैं। यह मत धनञ्जयादि का है। (6/84)
4
विधेयाविमर्श: : - एक काव्यदोष । विधेय अंश का ही जहाँ प्रधानतया परामर्श न हो, वहाँ विधेयाविमर्श दोष होता है। यथा-स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः । इस पंक्ति में भुजाओं का वृथात्व बताना ही विधेय है और उसे ही समास में डालकर अप्रधान बना दिया गया है। यथा च - रक्षांस्यपि पुर: स्थातुमलं रामानुजस्य मे। इस उदाहरण में राम के साथ सम्बन्ध प्रतिपादित करना ही विधेय है और उसके वाचक षष्ठी विभक्ति को समास में डालकर उसकी प्रधानता समाप्त कर दी गयी है। यह पददोष समास में ही होता है । न्यक्कारो ह्ययमेव में यदरयः० आदि प्रसिद्ध पद्य में वाक्यगत विधेयाविमर्श दोष है। इस पद्य में 'न्यक्कार' विधेय है तथा 'अयमेव '