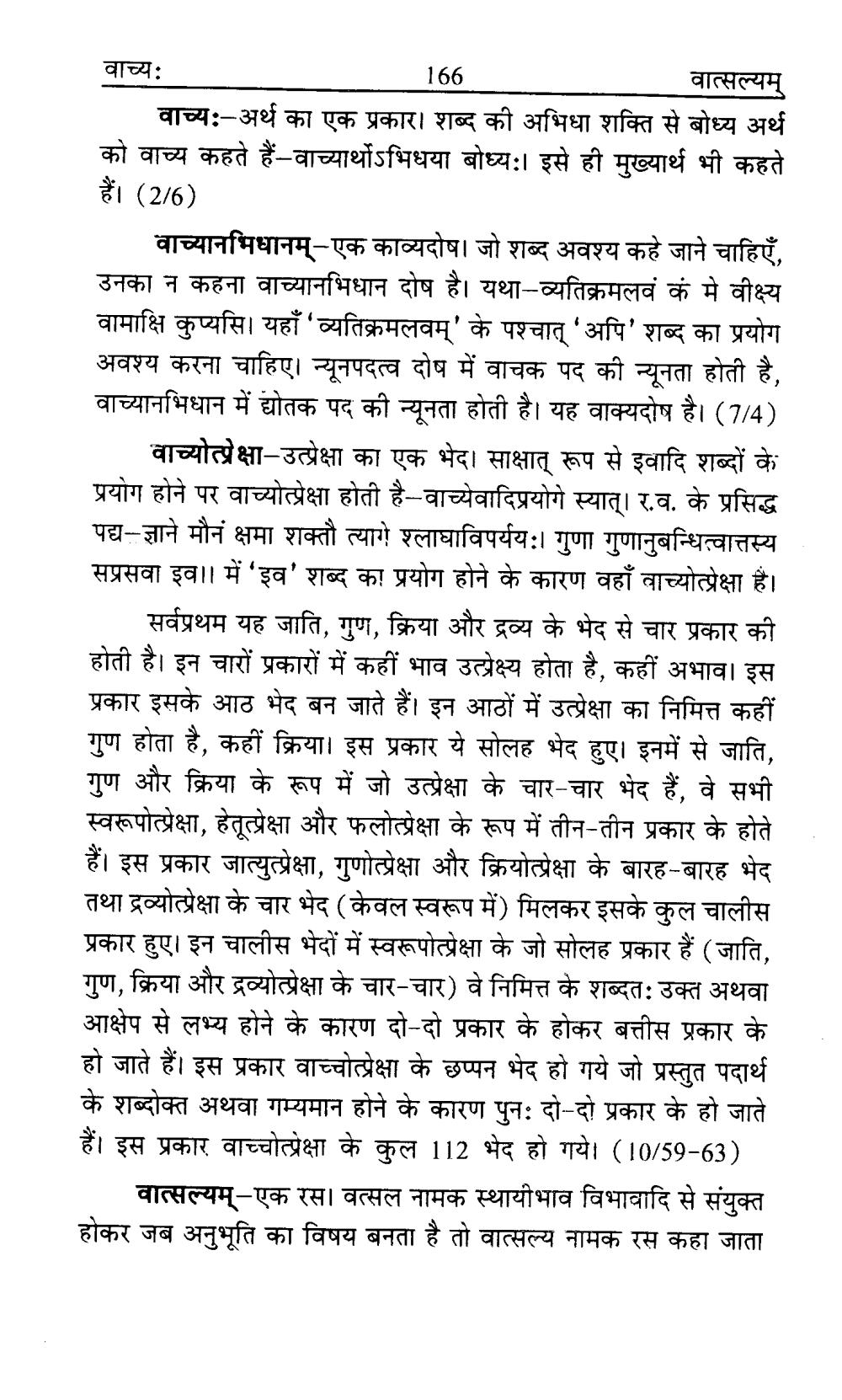________________
वाच्यः
166
वात्सल्यम्
वाच्यः - अर्थ का एक प्रकार । शब्द की अभिधा शक्ति से बोध्य अर्थ को वाच्य कहते हैं - वाच्यार्थोऽभिधया बोध्यः । इसे ही मुख्यार्थ भी कहते हैं। (2/6)
वाच्यानभिधानम् - एक काव्यदोष। जो शब्द अवश्य कहे जाने चाहिएँ, उनका न कहना वाच्यानभिधान दोष है। यथा - व्यतिक्रमलवं कं मे वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यसि । यहाँ ' व्यतिक्रमलवम्' के पश्चात् 'अपि' शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। न्यूनपदत्व दोष में वाचक पद की न्यूनता होती है, वाच्यानभिधान में द्योतक पद की न्यूनता होती है। यह वाक्यदोष है। (7/4)
वाच्योत्प्रेक्षा- उत्प्रेक्षा का एक भेद । साक्षात् रूप से इवादि शब्दों के प्रयोग होने पर वाच्योत्प्रेक्षा होती है-वाच्येवादिप्रयोगे स्यात् । र.व. के प्रसिद्ध पद्य-ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः । गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव । । में 'इव' शब्द का प्रयोग होने के कारण वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा है।
सर्वप्रथम यह जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के भेद से चार प्रकार की होती है। इन चारों प्रकारों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य होता है, कहीं अभाव। इस प्रकार इसके आठ भेद बन जाते हैं। इन आठों में उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं गुण होता है, कहीं क्रिया । इस प्रकार ये सोलह भेद हुए । इनमें से जाति, गुण और क्रिया के रूप में जो उत्प्रेक्षा के चार-चार भेद हैं, वे सभी स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा के रूप में तीन-तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जात्युत्प्रेक्षा, गुणोत्प्रेक्षा और क्रियोत्प्रेक्षा के बारह - बारह भेद तथा द्रव्योत्प्रेक्षा के चार भेद (केवल स्वरूप में) मिलकर इसके कुल चालीस प्रकार हुए। इन चालीस भेदों में स्वरूपोत्प्रेक्षा के जो सोलह प्रकार हैं (जाति, गुण, क्रिया और द्रव्योत्प्रेक्षा के चार-चार ) वे निमित्त के शब्दतः उक्त अथवा आक्षेप से लभ्य होने के कारण दो-दो प्रकार के होकर बत्तीस प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार वाच्चोत्प्रेक्षा के छप्पन भेद हो गये जो प्रस्तुत पदार्थ के शब्दोक्त अथवा गम्यमान होने के कारण पुनः दो-दो प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार वाच्चोत्प्रेक्षा के कुल 112 भेद हो गये । ( 10/59-63)
वात्सल्यम्–एक रस। वत्सल नामक स्थायीभाव विभावादि से संयुक्त होकर जब अनुभूति का विषय बनता है तो वात्सल्य नामक रस कहा जाता