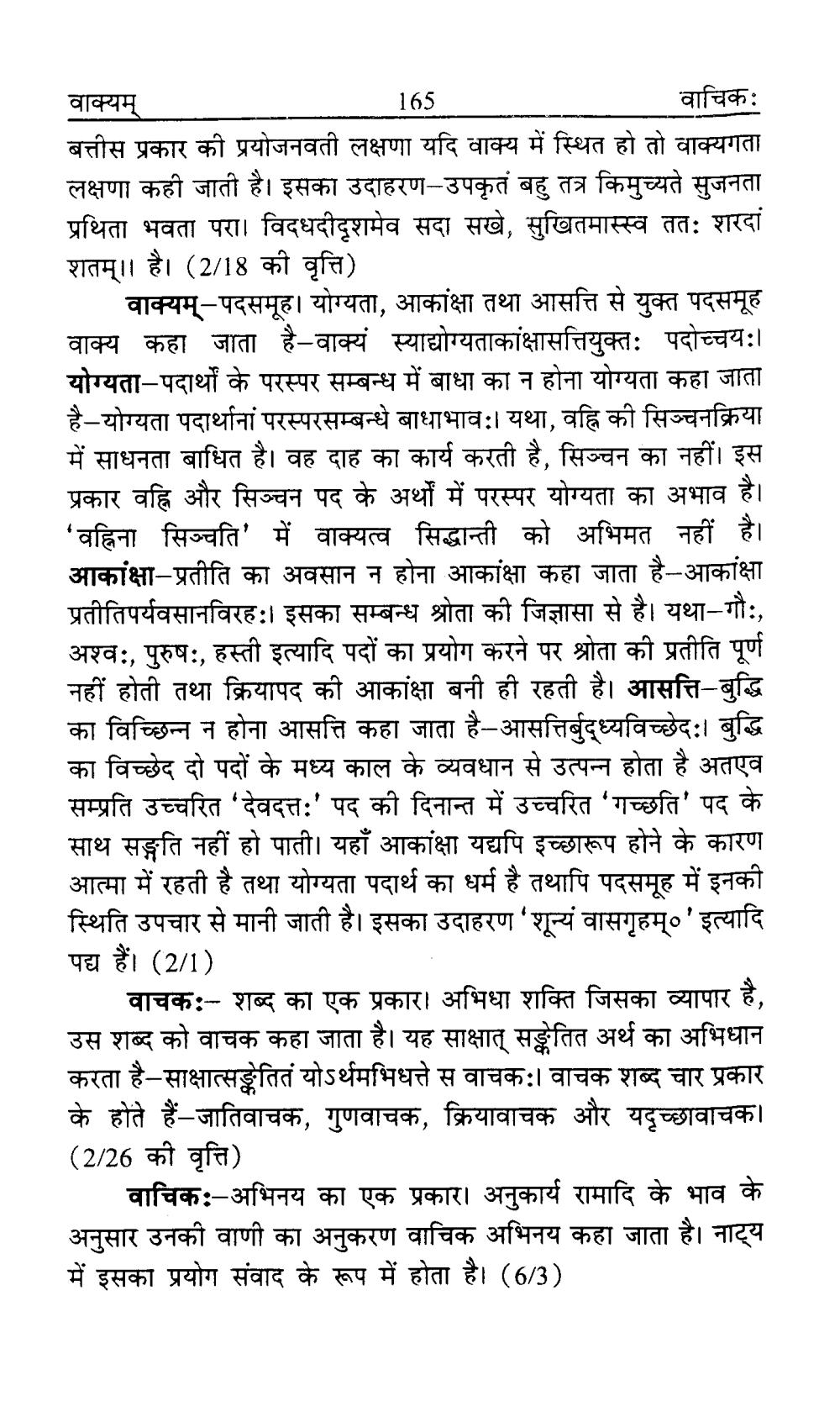________________
165
वाक्यम्
वाचिकः बत्तीस प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा यदि वाक्य में स्थित हो तो वाक्यगता लक्षणा कही जाती है। इसका उदाहरण-उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परा। विदधदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्।। है। (2/18 की वृत्ति)
वाक्यम्-पदसमूह। योग्यता, आकांक्षा तथा आसत्ति से युक्त पदसमूह वाक्य कहा जाता है-वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः। योग्यता-पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का न होना योग्यता कहा जाता है-योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः। यथा, वह्नि की सिञ्चनक्रिया में साधनता बाधित है। वह दाह का कार्य करती है, सिञ्चन का नहीं। इस प्रकार वह्नि और सिञ्चन पद के अर्थों में परस्पर योग्यता का अभाव है। 'वह्निना सिञ्चति' में वाक्यत्व सिद्धान्ती को अभिमत नहीं है। आकांक्षा-प्रतीति का अवसान न होना आकांक्षा कहा जाता है-आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः। इसका सम्बन्ध श्रोता की जिज्ञासा से है। यथा-गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती इत्यादि पदों का प्रयोग करने पर श्रोता की प्रतीति पूर्ण नहीं होती तथा क्रियापद की आकांक्षा बनी ही रहती है। आसत्ति-बुद्धि का विच्छिन्न न होना आसत्ति कहा जाता है-आसत्तिर्बुद्ध्यविच्छेदः। बुद्धि का विच्छेद दो पदों के मध्य काल के व्यवधान से उत्पन्न होता है अतएव सम्प्रति उच्चरित 'देवदत्तः' पद की दिनान्त में उच्चरित 'गच्छति' पद के साथ सङ्गति नहीं हो पाती। यहाँ आकांक्षा यद्यपि इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती है तथा योग्यता पदार्थ का धर्म है तथापि पदसमूह में इनकी स्थिति उपचार से मानी जाती है। इसका उदाहरण 'शून्यं वासगृहम् ' इत्यादि पद्य हैं। (2/1)
वाचकः- शब्द का एक प्रकार। अभिधा शक्ति जिसका व्यापार है, उस शब्द को वाचक कहा जाता है। यह साक्षात् सङ्केतित अर्थ का अभिधान करता है-साक्षात्सङ्केतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः। वाचक शब्द चार प्रकार के होते हैं-जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छावाचक। (2/26 की वृत्ति)
वाचिक:-अभिनय का एक प्रकार। अनुकार्य रामादि के भाव के अनुसार उनकी वाणी का अनुकरण वाचिक अभिनय कहा जाता है। नाट्य में इसका प्रयोग संवाद के रूप में होता है। (6/3)