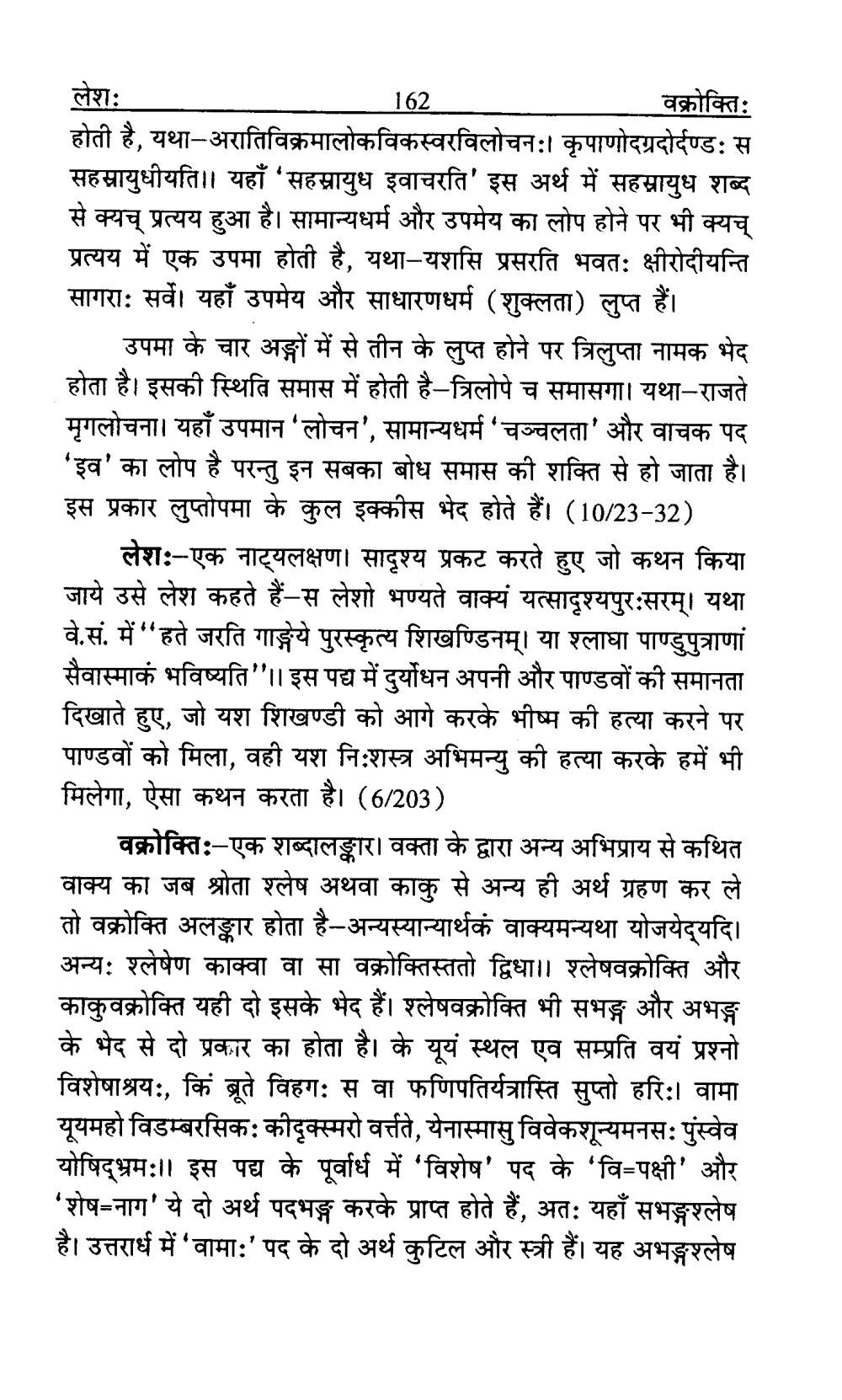________________
162
लेशः
वक्रोक्तिः होती है, यथा-अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः। कृपाणोदग्रदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति।। यहाँ 'सहस्रायुध इवाचरति' इस अर्थ में सहस्रायुध शब्द से क्यच् प्रत्यय हुआ है। सामान्यधर्म और उपमेय का लोप होने पर भी क्यच् प्रत्यय में एक उपमा होती है, यथा-यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे। यहाँ उपमेय और साधारणधर्म (शुक्लता) लुप्त हैं।
उपमा के चार अङ्गों में से तीन के लुप्त होने पर त्रिलुप्ता नामक भेद होता है। इसकी स्थिति समास में होती है-त्रिलोपे च समासगा। यथा-राजते मृगलोचना। यहाँ उपमान 'लोचन', सामान्यधर्म 'चञ्चलता' और वाचक पद 'इव' का लोप है परन्तु इन सबका बोध समास की शक्ति से हो जाता है। इस प्रकार लुप्तोपमा के कुल इक्कीस भेद होते हैं। (10/23-32)
लेशः-एक नाट्यलक्षण। सादृश्य प्रकट करते हुए जो कथन किया जाये उसे लेश कहते हैं-स लेशो भण्यते वाक्यं यत्सादृश्यपुरःसरम्। यथा वे.सं. में "हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां सैवास्माकं भविष्यति"।। इस पद्य में दुर्योधन अपनी और पाण्डवों की समानता दिखाते हुए, जो यश शिखण्डी को आगे करके भीष्म की हत्या करने पर पाण्डवों को मिला, वही यश निःशस्त्र अभिमन्यु की हत्या करके हमें भी मिलेगा, ऐसा कथन करता है। (6/203)
वक्रोक्तिः -एक शब्दालङ्कार। वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य का जब श्रोता श्लेष अथवा काकु से अन्य ही अर्थ ग्रहण कर ले तो वक्रोक्ति अलङ्कार होता है-अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि। अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। श्लेषवक्रोक्ति और काकुवक्रोक्ति यही दो इसके भेद हैं। श्लेषवक्रोक्ति भी सभङ्ग और अभङ्ग के भेद से दो प्रकार का होता है। के यूयं स्थल एव सम्प्रति वयं प्रश्नो विशेषाश्रयः, किं ब्रूते विहगः स वा फणिपतिर्यत्रास्ति सुप्तो हरिः। वामा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक्स्मरो वर्त्तते, येनास्मासु विवेकशून्यमनसः पुंस्वेव योषिभ्रमः।। इस पद्य के पूर्वार्ध में 'विशेष' पद के 'विपक्षी' और 'शेष-नाग' ये दो अर्थ पदभङ्ग करके प्राप्त होते हैं, अतः यहाँ सभङ्गश्लेष है। उत्तरार्ध में 'वामाः' पद के दो अर्थ कुटिल और स्त्री हैं। यह अभङ्गश्लेष