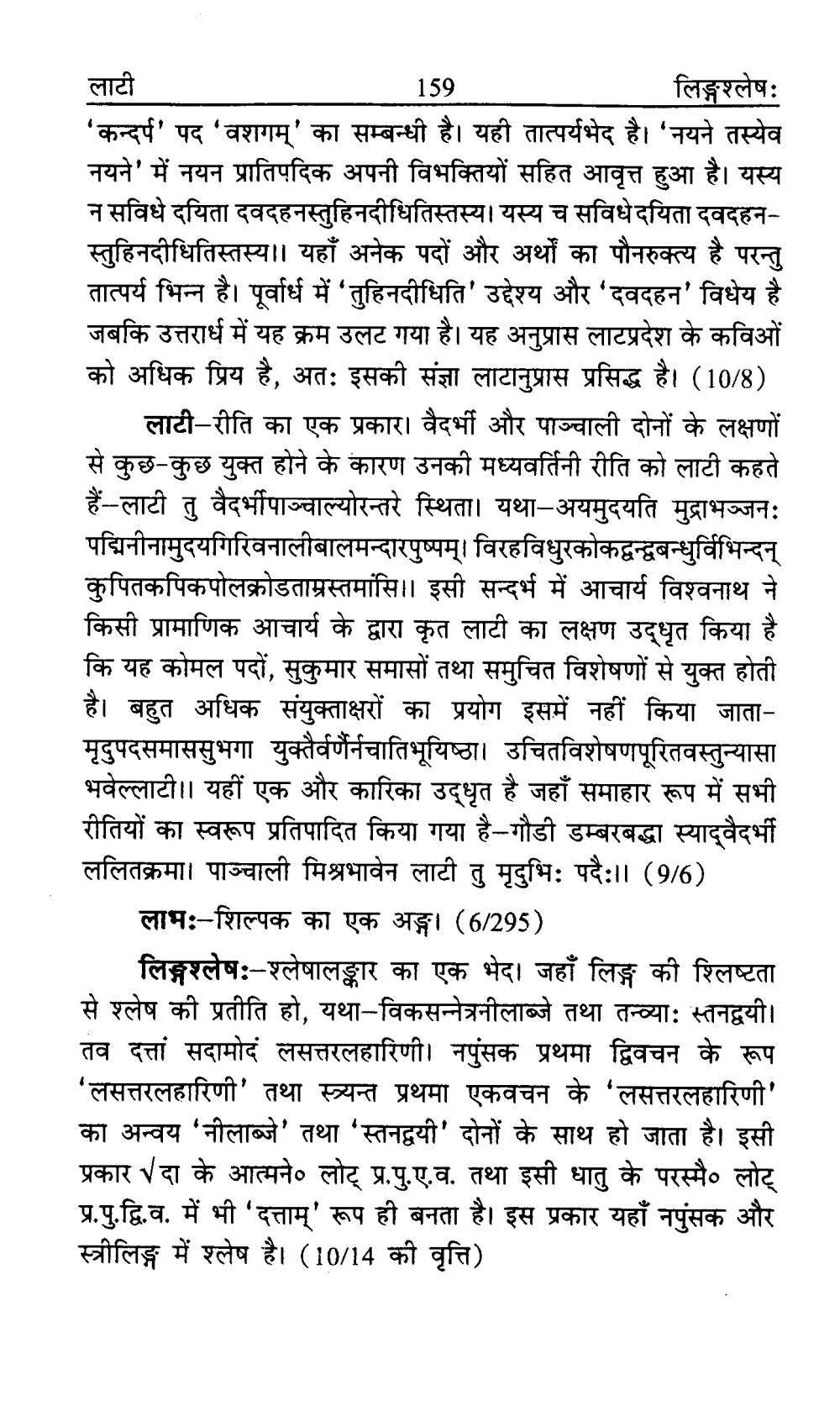________________
लाटी
159
लिङ्गश्लेषः 'कन्दर्प' पद ‘वशगम्' का सम्बन्धी है। यही तात्पर्यभेद है। 'नयने तस्येव नयने' में नयन प्रातिपदिक अपनी विभक्तियों सहित आवृत्त हुआ है। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। यस्य च सविधेदयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य।। यहाँ अनेक पदों और अर्थों का पौनरुक्त्य है परन्तु तात्पर्य भिन्न है। पूर्वार्ध में 'तुहिनदीधिति' उद्देश्य और 'दवदहन' विधेय है जबकि उत्तरार्ध में यह क्रम उलट गया है। यह अनुप्रास लाटप्रदेश के कविओं को अधिक प्रिय है, अतः इसकी संज्ञा लाटानुप्रास प्रसिद्ध है। (10/8)
लाटी-रीति का एक प्रकार। वैदर्भी और पाञ्चाली दोनों के लक्षणों से कुछ-कुछ युक्त होने के कारण उनकी मध्यवर्तिनी रीति को लाटी कहते हैं-लाटी तु वैदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता। यथा-अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्। विरहविधुरकोकद्वन्द्वबन्धुर्विभिन्दन् कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि।। इसी सन्दर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने किसी प्रामाणिक आचार्य के द्वारा कृत लाटी का लक्षण उद्धृत किया है कि यह कोमल पदों, सुकुमार समासों तथा समुचित विशेषणों से युक्त होती है। बहुत अधिक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं किया जातामृदुपदसमाससुभगा युक्तैर्वर्णैर्नचातिभूयिष्ठा। उचितविशेषणपूरितवस्तुन्यासा भवेल्लाटी।। यहीं एक और कारिका उद्धृत है जहाँ समाहार रूप में सभी रीतियों का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है-गौडी डम्बरबद्धा स्याद्वैदर्भी ललितक्रमा। पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदैः।। (9/6)
लामः-शिल्पक का एक अङ्ग। (6/295) ।
लिङ्गश्लेषः-श्लेषालङ्कार का एक भेद। जहाँ लिङ्ग की श्लिष्टता से श्लेष की प्रतीति हो, यथा-विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी। तव दत्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी। नपुंसक प्रथमा द्विवचन के रूप 'लसत्तरलहारिणी' तथा स्त्र्यन्त प्रथमा एकवचन के 'लसत्तरलहारिणी' का अन्वय 'नीलाब्जे' तथा 'स्तनद्वयी' दोनों के साथ हो जाता है। इसी प्रकार / दा के आत्मने० लोट् प्र.पु.ए.व. तथा इसी धातु के परस्मै० लोट प्र.पु.द्वि.व. में भी 'दत्ताम्' रूप ही बनता है। इस प्रकार यहाँ नपुंसक और स्त्रीलिङ्ग में श्लेष है। (10/14 की वृत्ति)