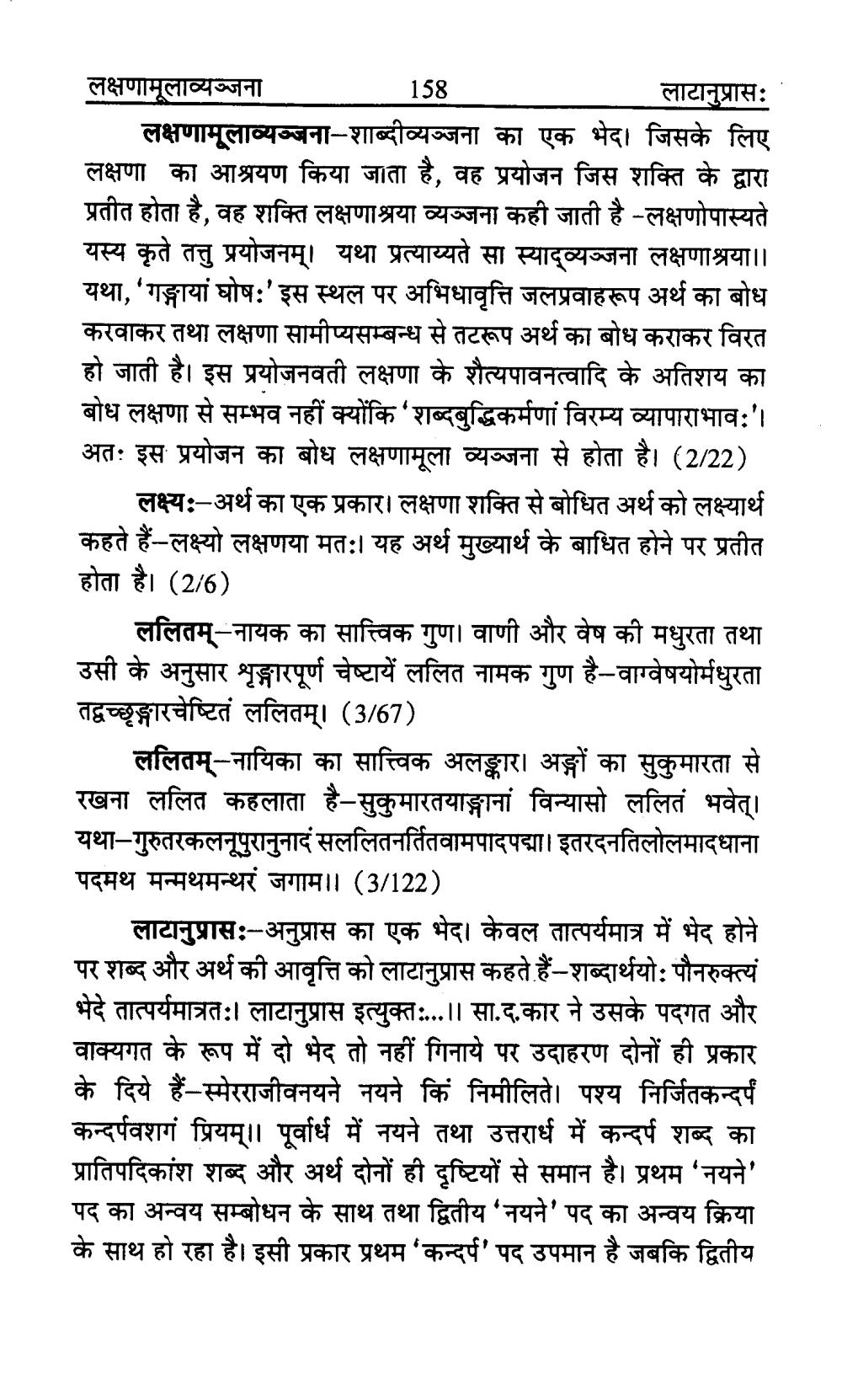________________
लक्षणामूलाव्यञ्जना
158
लाटानुप्रासः
लक्षणामूलाव्यञ्जना - शाब्दीव्यञ्जना का एक भेद। जिसके लिए लक्षणा का आश्रयण किया जाता है, वह प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है, वह शक्ति लक्षणाश्रया व्यञ्जना कही जाती है - लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम् । यथा प्रत्याय्यते सा स्याद्व्यञ्जना लक्षणाश्रया ।। यथा, 'गङ्गायां घोष:' इस स्थल पर अभिधावृत्ति जलप्रवाहरूप अर्थ का बोध करवाकर तथा लक्षणा सामीप्यसम्बन्ध से तटरूप अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाती है। इस प्रयोजनवती लक्षणा के शैत्यपावनत्वादि के अतिशय का बोध लक्षणा से सम्भव नहीं क्योंकि ' शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः '। अतः इस प्रयोजन का बोध लक्षणामूला व्यञ्जना से होता है। (2/22)
लक्ष्यः-अर्थ का एक प्रकार। लक्षणा शक्ति से बोधित अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं-लक्ष्यो लक्षणया मतः । यह अर्थ मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रतीत होता है। (2/6)
ललितम् - नायक का सात्त्विक गुण । वाणी और वेष की मधुरता तथा उसी के अनुसार शृङ्गारपूर्ण चेष्टायें ललित नामक गुण है- वाग्वेषयोर्मधुरता तद्वच्छृङ्गारचेष्टितं ललितम् । (3/67)
ललितम् - नायिका का सात्त्विक अलङ्कार । अङ्गों का सुकुमारता से रखना ललित कहलाता है - सुकुमारतयाङ्गानां विन्यासो ललितं भवेत् । यथा - गुरुतरकलनूपुरानुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा । इतरदनतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ।। (3/122)
लाटानुप्रासः - अनुप्रास का एक भेद । केवल तात्पर्यमात्र में भेद होने पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति को लाटानुप्रास कहते हैं-शब्दार्थयो: पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः। लाटानुप्रास इत्युक्तः:... ।। सा.द. कार ने उसके पदगत और वाक्यगत के रूप में दो भेद तो नहीं गिनाये पर उदाहरण दोनों ही प्रकार के दिये हैं- स्मेरराजीवनयने नयने किं निमीलिते । पश्य निर्जितकन्दर्पं कन्दर्पवशगं प्रियम् ।। पूर्वार्ध में नयने तथा उत्तरार्ध में कन्दर्प शब्द का प्रातिपदिकांश शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से समान है। प्रथम 'नयने ' पद का अन्वय सम्बोधन के साथ तथा द्वितीय 'नयने' पद का अन्वय क्रिया के साथ हो रहा है। इसी प्रकार प्रथम 'कन्दर्प' पद उपमान है जबकि द्वितीय