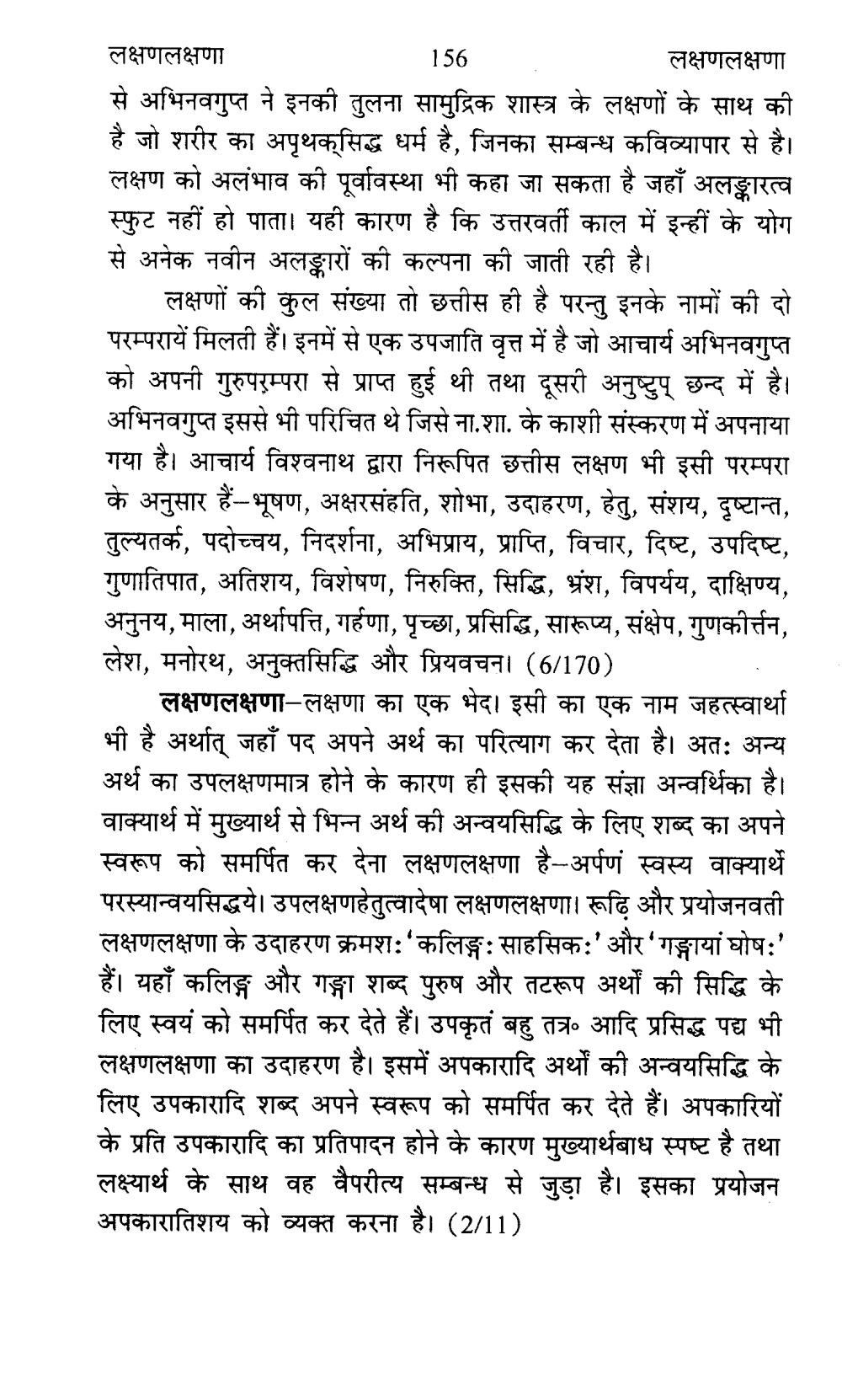________________
156
लक्षणलक्षणा
लक्षणलक्षणा से अभिनवगुप्त ने इनकी तुलना सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों के साथ की है जो शरीर का अपृथक्सिद्ध धर्म है, जिनका सम्बन्ध कविव्यापार से है। लक्षण को अलंभाव की पूर्वावस्था भी कहा जा सकता है जहाँ अलङ्कारत्व स्फुट नहीं हो पाता। यही कारण है कि उत्तरवर्ती काल में इन्हीं के योग से अनेक नवीन अलङ्कारों की कल्पना की जाती रही है। ___लक्षणों की कुल संख्या तो छत्तीस ही है परन्तु इनके नामों की दो परम्परायें मिलती हैं। इनमें से एक उपजाति वृत्त में है जो आचार्य अभिनवगुप्त को अपनी गुरुपरम्परा से प्राप्त हुई थी तथा दूसरी अनुष्टुप् छन्द में है। अभिनवगुप्त इससे भी परिचित थे जिसे ना.शा. के काशी संस्करण में अपनाया गया है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा निरूपित छत्तीस लक्षण भी इसी परम्परा के अनुसार हैं-भूषण, अक्षरसंहति, शोभा, उदाहरण, हेतु, संशय, दृष्टान्त, तुल्यतर्क, पदोच्चय, निदर्शना, अभिप्राय, प्राप्ति, विचार, दिष्ट, उपदिष्ट, गुणातिपात, अतिशय, विशेषण, निरुक्ति, सिद्धि, भ्रंश, विपर्यय, दाक्षिण्य, अनुनय, माला, अर्थापत्ति, गर्हणा, पृच्छा, प्रसिद्धि, सारूप्य, संक्षेप, गुणकीर्तन, लेश, मनोरथ, अनुक्तसिद्धि और प्रियवचन। (6/170)
लक्षणलक्षणा-लक्षणा का एक भेद। इसी का एक नाम जहत्स्वार्था भी है अर्थात् जहाँ पद अपने अर्थ का परित्याग कर देता है। अतः अन्य अर्थ का उपलक्षणमात्र होने के कारण ही इसकी यह संज्ञा अन्वर्थिका है। वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ की अन्वयसिद्धि के लिए शब्द का अपने स्वरूप को समर्पित कर देना लक्षणलक्षणा है-अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये। उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा। रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा के उदाहरण क्रमशः कलिङ्गः साहसिकः' और 'गङ्गायां घोषः' हैं। यहाँ कलिङ्ग और गङ्गा शब्द पुरुष और तटरूप अर्थों की सिद्धि के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उपकृतं बहु तत्र० आदि प्रसिद्ध पद्य भी लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। इसमें अपकारादि अर्थों की अन्वयसिद्धि के लिए उपकारादि शब्द अपने स्वरूप को समर्पित कर देते हैं। अपकारियों के प्रति उपकारादि का प्रतिपादन होने के कारण मुख्यार्थबाध स्पष्ट है तथा लक्ष्यार्थ के साथ वह वैपरीत्य सम्बन्ध से जुड़ा है। इसका प्रयोजन अपकारातिशय को व्यक्त करना है। (2/11)