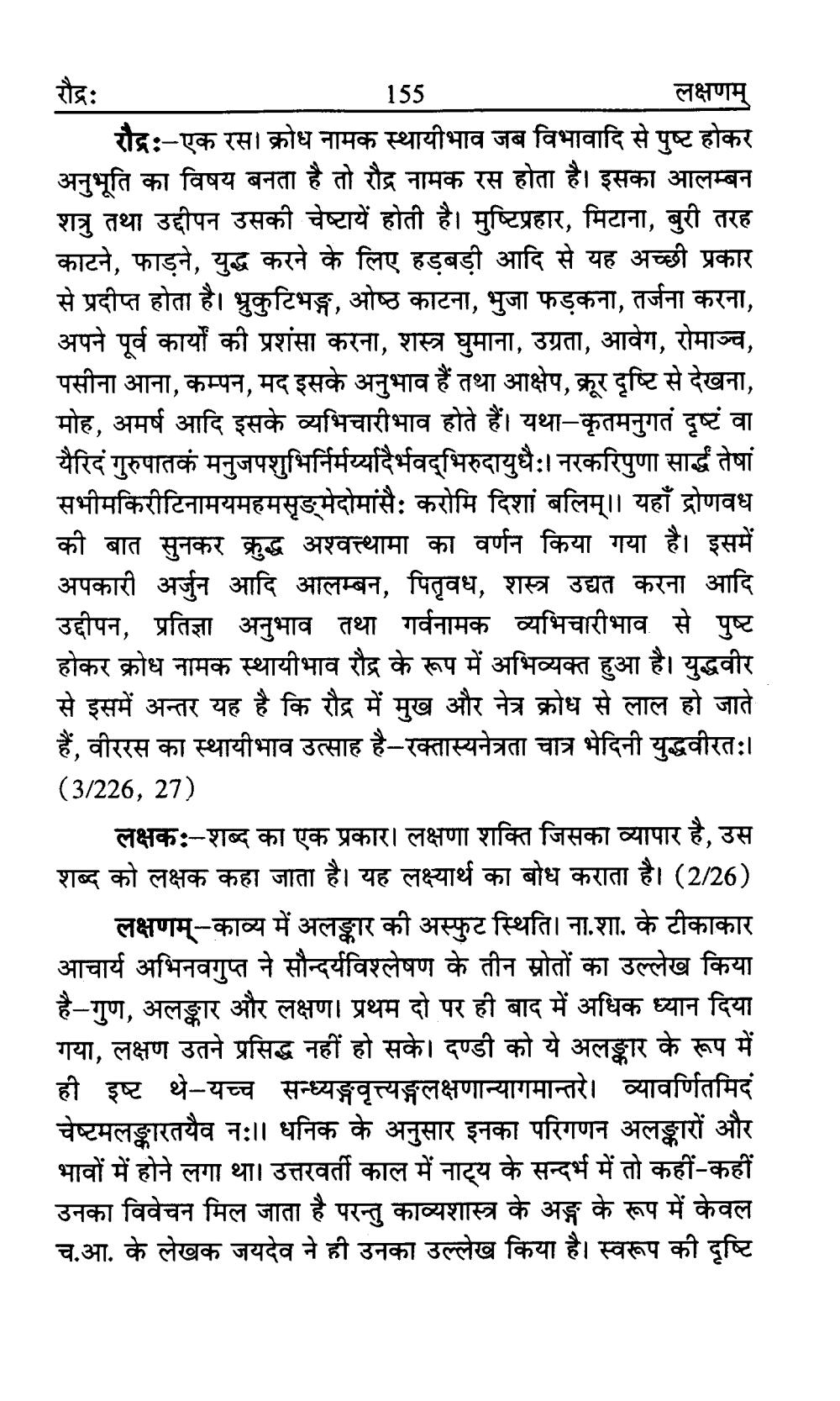________________
रौद्रः
155
लक्षणम्
होकर
रौद्र::- एक रस । क्रोध नामक स्थायीभाव जब विभावादि से पुष्ट अनुभूति का विषय बनता है तो रौद्र नामक रस होता है। इसका आलम्बन शत्रु तथा उद्दीपन उसकी चेष्टायें होती है। मुष्टिप्रहार, मिटाना, बुरी तरह काटने, फाड़ने, युद्ध करने के लिए हड़बड़ी आदि से यह अच्छी प्रकार
प्रदीप्त होता है । भ्रुकुटिभङ्ग, ओष्ठ काटना, भुजा फड़कना, तर्जना करना, अपने पूर्व कार्यों की प्रशंसा करना, शस्त्र घुमाना, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, पसीना आना, कम्पन, मद इसके अनुभाव हैं तथा आक्षेप, क्रूर दृष्टि से देखना, मोह, अमर्ष आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। यथा- कृतमनुगतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं मनुजपशुभिर्निर्मर्य्यादैर्भवद्भिरुदायुधैः । नरकरिपुणा सार्द्धं तेषां सभीमकिरीटिनामयमहमसृङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम् । यहाँ द्रोणवध की बात सुनकर क्रुद्ध अश्वत्थामा का वर्णन किया गया है। इसमें अपकारी अर्जुन आदि आलम्बन, पितृवध, शस्त्र उद्यत करना आदि उद्दीपन, प्रतिज्ञा अनुभाव तथा गर्वनामक व्यभिचारीभाव से पुष्ट होकर क्रोध नामक स्थायीभाव रौद्र के रूप में अभिव्यक्त हुआ है । युद्धवीर से इसमें अन्तर यह है कि रौद्र में मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो जाते हैं, वीररस का स्थायीभाव उत्साह है - रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः । (3/226, 27)
लक्षक:- शब्द का एक प्रकार। लक्षणा शक्ति जिसका व्यापार है, उस शब्द को लक्षक कहा जाता है। यह लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। (2/26)
लक्षणम्-काव्य में अलङ्कार की अस्फुट स्थिति । ना.शा. के टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त ने सौन्दर्यविश्लेषण के तीन स्रोतों का उल्लेख किया है - गुण, अलङ्कार और लक्षण । प्रथम दो पर ही बाद में अधिक ध्यान दिया गया, लक्षण उतने प्रसिद्ध नहीं हो सके। दण्डी को ये अलङ्कार के रूप में ही इष्ट थे- यच्च सन्ध्यङ्गवृत्त्यङ्गलक्षणान्यागमान्तरे । व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः।। धनिक के अनुसार इनका परिगणन अलङ्कारों और भावों में होने लगा था। उत्तरवर्ती काल में नाट्य के सन्दर्भ में तो कहीं-कहीं उनका विवेचन मिल जाता है परन्तु काव्यशास्त्र के अङ्ग के रूप में केवल च. आ. के लेखक जयदेव ने ही उनका उल्लेख किया है। स्वरूप की दृष्टि