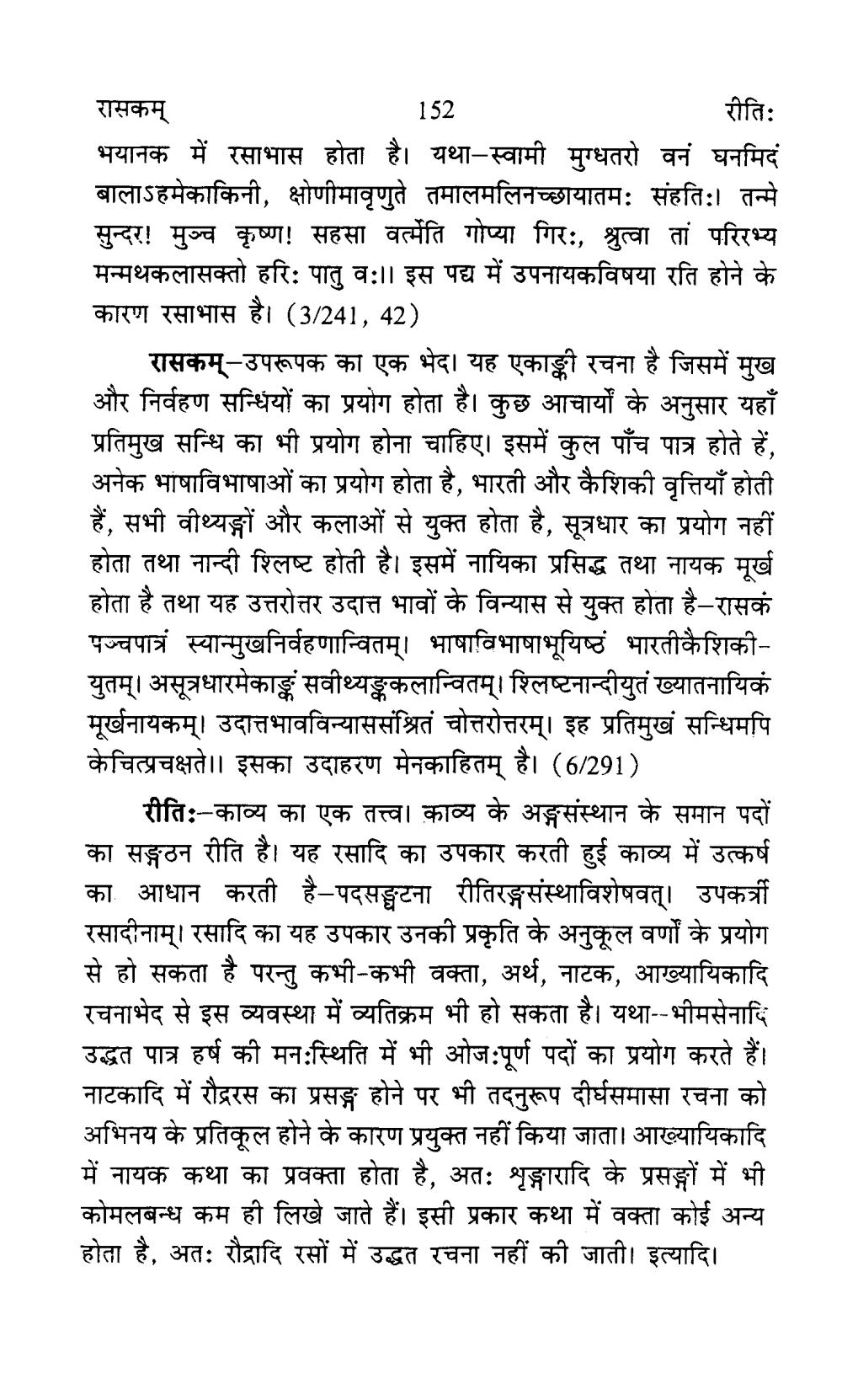________________
रासकम् 152
रीतिः भयानक में रसाभास होता है। यथा-स्वामी मुग्धतरो वनं घनमिदं बालाऽहमेकाकिनी, क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छायातमः संहतिः। तन्मे सुन्दर! मुञ्च कृष्ण! सहसा वर्मेति गोप्या गिरः, श्रुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः।। इस पद्य में उपनायकविषया रति होने के कारण रसाभास है। (3/241, 42)
रासकम्-उपरूपक का एक भेद। यह एकाङ्की रचना है जिसमें मुख और निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता है। कुछ आचार्यों के अनुसार यहाँ प्रतिमुख सन्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। इसमें कुल पाँच पात्र होते हैं, अनेक भाषाविभाषाओं का प्रयोग होता है, भारती और कैशिकी वृत्तियाँ होती हैं, सभी वीथ्यङ्गों और कलाओं से युक्त होता है, सूत्रधार का प्रयोग नहीं होता तथा नान्दी श्लिष्ट होती है। इसमें नायिका प्रसिद्ध तथा नायक मूर्ख होता है तथा यह उत्तरोत्तर उदात्त भावों के विन्यास से युक्त होता है-रासकं पञ्चपात्रं स्यान्मुखनिर्वहणान्वितम्। भाषाविभाषाभूयिष्ठं भारतीकैशिकीयुतम्। असूत्रधारमेकाङ्कं सवीथ्यङ्ककलान्वितम्। श्लिष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं मूर्खनायकम्। उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्। इह प्रतिमुखं सन्धिमपि केचित्प्रचक्षते।। इसका उदाहरण मेनकाहितम् है। (6/291)
रीतिः-काव्य का एक तत्त्व। काव्य के अङ्गसंस्थान के समान पदों का सङ्गठन रीति है। यह रसादि का उपकार करती हई काव्य में उत्कर्ष का आधान करती है-पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्। उपकी रसादीनाम्। रसादि का यह उपकार उनकी प्रकृति के अनुकूल वर्गों के प्रयोग से हो सकता है परन्तु कभी-कभी वक्ता, अर्थ, नाटक, आख्यायिकादि रचनाभेद से इस व्यवस्था में व्यतिक्रम भी हो सकता है। यथा--भीमसेनादि उद्धत पात्र हर्ष की मन:स्थिति में भी ओजःपूर्ण पदों का प्रयोग करते हैं। नाटकादि में रौद्ररस का प्रसङ्ग होने पर भी तदनुरूप दीर्घसमासा रचना को अभिनय के प्रतिकूल होने के कारण प्रयुक्त नहीं किया जाता। आख्यायिकादि में नायक कथा का प्रवक्ता होता है, अतः शृङ्गारादि के प्रसङ्गों में भी कोमलबन्ध कम ही लिखे जाते हैं। इसी प्रकार कथा में वक्ता कोई अन्य होता है, अतः रौद्रादि रसों में उद्धत रचना नहीं की जाती। इत्यादि।