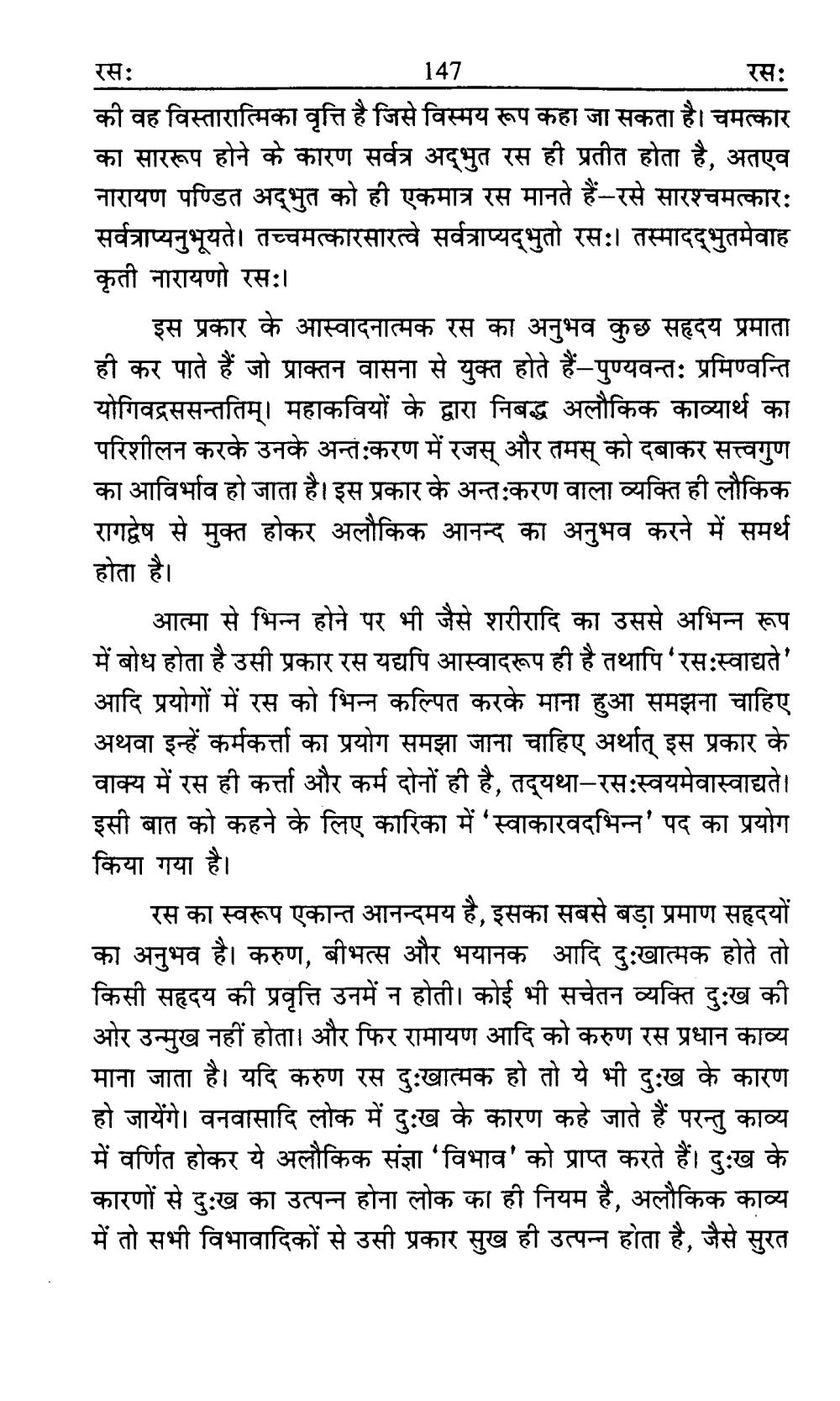________________
रसः 147
रसः की वह विस्तारात्मिका वृत्ति है जिसे विस्मय रूप कहा जा सकता है। चमत्कार का साररूप होने के कारण सर्वत्र अद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अतएव नारायण पण्डित अद्भुत को ही एकमात्र रस मानते हैं-रसे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसः।
इस प्रकार के आस्वादनात्मक रस का अनुभव कुछ सहृदय प्रमाता ही कर पाते हैं जो प्राक्तन वासना से युक्त होते हैं-पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्। महाकवियों के द्वारा निबद्ध अलौकिक काव्यार्थ का परिशीलन करके उनके अन्त:करण में रजस् और तमस् को दबाकर सत्त्वगुण का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार के अन्त:करण वाला व्यक्ति ही लौकिक रागद्वेष से मुक्त होकर अलौकिक आनन्द का अनुभव करने में समर्थ होता है।
आत्मा से भिन्न होने पर भी जैसे शरीरादि का उससे अभिन्न रूप में बोध होता है उसी प्रकार रस यद्यपि आस्वादरूप ही है तथापि रस:स्वाद्यते' आदि प्रयोगों में रस को भिन्न कल्पित करके माना हुआ समझना चाहिए अथवा इन्हें कर्मकर्ता का प्रयोग समझा जाना चाहिए अर्थात् इस प्रकार के वाक्य में रस ही कर्ता और कर्म दोनों ही है, तद्यथा-रस:स्वयमेवास्वाद्यते। इसी बात को कहने के लिए कारिका में 'स्वाकारवदभिन्न' पद का प्रयोग किया गया है।
रस का स्वरूप एकान्त आनन्दमय है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण सहृदयों का अनुभव है। करुण, बीभत्स और भयानक आदि दु:खात्मक होते तो किसी सहृदय की प्रवृत्ति उनमें न होती। कोई भी सचेतन व्यक्ति दु:ख की
ओर उन्मुख नहीं होता। और फिर रामायण आदि को करुण रस प्रधान काव्य माना जाता है। यदि करुण रस दुःखात्मक हो तो ये भी दु:ख के कारण हो जायेंगे। वनवासादि लोक में दु:ख के कारण कहे जाते हैं परन्तु काव्य में वर्णित होकर ये अलौकिक संज्ञा 'विभाव' को प्राप्त करते हैं। दु:ख के कारणों से दु:ख का उत्पन्न होना लोक का ही नियम है, अलौकिक काव्य में तो सभी विभावादिकों से उसी प्रकार सुख ही उत्पन्न होता है, जैसे सुरत