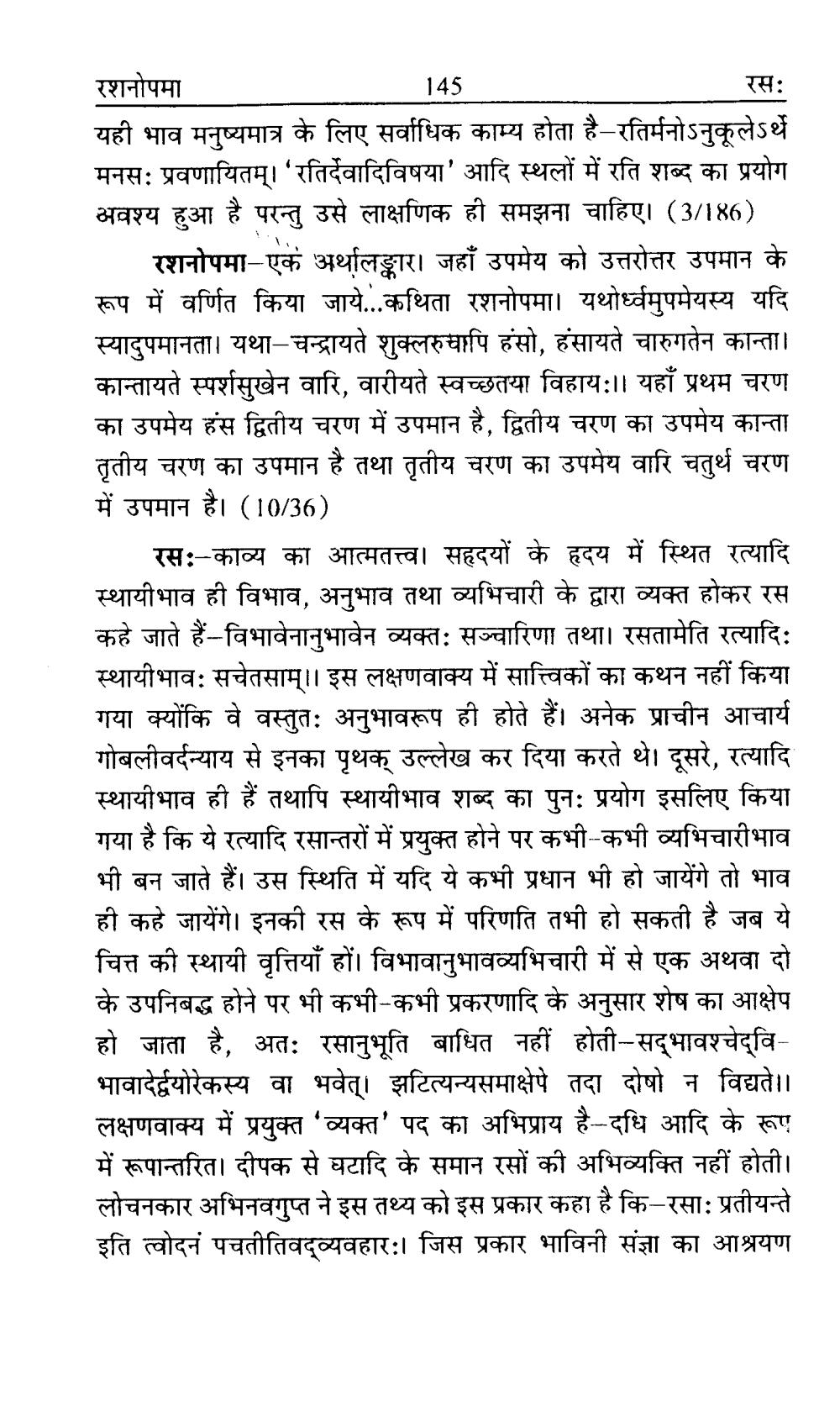________________
रशनोपमा
145
यही भाव मनुष्यमात्र के लिए सर्वाधिक काम्य होता है - रतिर्मनोऽनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्। 'रतिर्देवादिविषया' आदि स्थलों में रति शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है परन्तु उसे लाक्षणिक ही समझना चाहिए । ( 3 / 186 )
रसः
>
रशनोपमा एक अर्थालङ्कार । जहाँ उपमेय को उत्तरोत्तर उपमान के रूप में वर्णित किया जाये... कथिता रशनोपमा । यथोर्ध्वमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता। यथा-चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता । कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहायः ।। यहाँ प्रथम चरण का उपमेय हंस द्वितीय चरण में उपमान है, द्वितीय चरण का उपमेय कान्ता तृतीय चरण का उपमान है तथा तृतीय चरण का उपमेय वारि चतुर्थ चरण में उपमान है। ( 10/36)
रसः - काव्य का आत्मतत्त्व । सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायीभाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के द्वारा व्यक्त होकर रस कहे जाते हैं - विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम् । । इस लक्षणवाक्य में सात्त्विकों का कथन नहीं किया गया क्योंकि वे वस्तुत: अनुभावरूप ही होते हैं। अनेक प्राचीन आचार्य गोबलीवर्दन्याय से इनका पृथक् उल्लेख कर दिया करते थे। दूसरे, रत्यादि स्थायीभाव ही हैं तथापि स्थायीभाव शब्द का पुनः प्रयोग इसलिए किया गया है कि ये रत्यादि रसान्तरों में प्रयुक्त होने पर कभी-कभी व्यभिचारीभाव भी बन जाते हैं। उस स्थिति में यदि ये कभी प्रधान भी हो जायेंगे तो भाव ही कहे जायेंगे। इनकी रस के रूप में परिणति तभी हो सकती है जब ये चित्त की स्थायी वृत्तियाँ हों। विभावानुभावव्यभिचारी में से एक अथवा दो के उपनिबद्ध होने पर भी कभी-कभी प्रकरणादि के अनुसार शेष का आक्षेप हो जाता है, अतः रसानुभूति बाधित नहीं होती - सद्भावश्चेद्विभावादेर्द्वयोरेकस्य वा भवेत् । झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते । । लक्षणवाक्य में प्रयुक्त 'व्यक्त' पद का अभिप्राय है- दधि आदि के रूप में रूपान्तरित । दीपक से घटादि के समान रसों की अभिव्यक्ति नहीं होती । लोचनकार अभिनवगुप्त ने इस तथ्य को इस प्रकार कहा है कि- रसाः प्रतीयन्ते इति त्वोदनं पचतीतिवद्व्यवहारः । जिस प्रकार भाविनी संज्ञा का आश्रयण