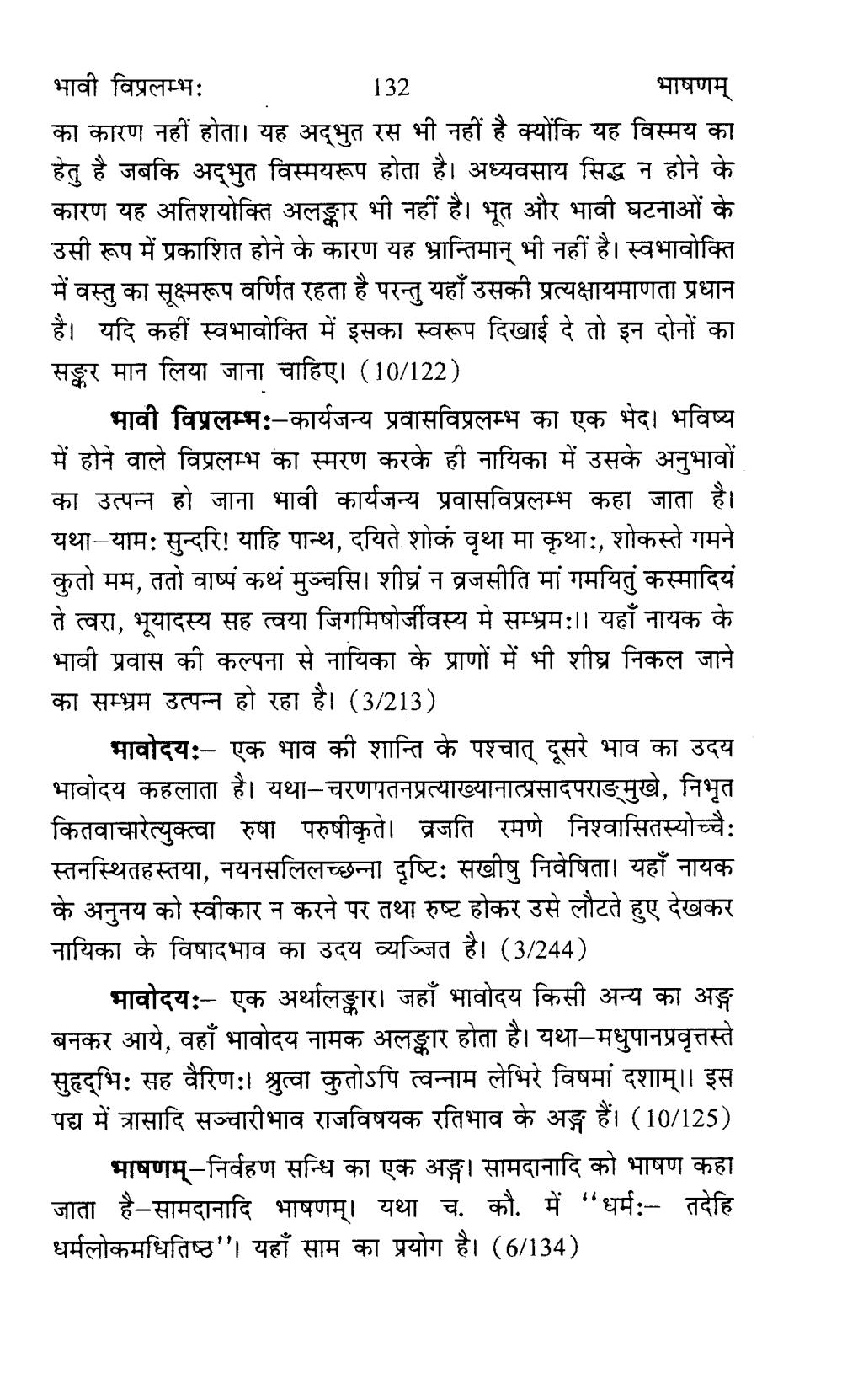________________
भावी विप्रलम्भः
132
भाषणम् का कारण नहीं होता। यह अद्भुत रस भी नहीं है क्योंकि यह विस्मय का हेतु है जबकि अद्भुत विस्मयरूप होता है। अध्यवसाय सिद्ध न होने के कारण यह अतिशयोक्ति अलङ्कार भी नहीं है। भूत और भावी घटनाओं के उसी रूप में प्रकाशित होने के कारण यह भ्रान्तिमान् भी नहीं है। स्वभावोक्ति में वस्तु का सूक्ष्मरूप वर्णित रहता है परन्तु यहाँ उसकी प्रत्यक्षायमाणता प्रधान है। यदि कहीं स्वभावोक्ति में इसका स्वरूप दिखाई दे तो इन दोनों का सङ्कर मान लिया जाना चाहिए। (10/122)
भावी विप्रलम्भः-कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ का एक भेद। भविष्य में होने वाले विप्रलम्भ का स्मरण करके ही नायिका में उसके अनुभावों का उत्पन्न हो जाना भावी कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ कहा जाता है। यथा-यामः सुन्दरि! याहि पान्थ, दयिते शोकं वृथा मा कृथाः, शोकस्ते गमने कुतो मम, ततो वाष्पं कथं मुञ्चसि। शीघ्रं न व्रजसीति मां गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा, भूयादस्य सह त्वया जिगमिषोर्जीवस्य मे सम्भ्रमः।। यहाँ नायक के भावी प्रवास की कल्पना से नायिका के प्राणों में भी शीघ्र निकल जाने का सम्भ्रम उत्पन्न हो रहा है। (3/213)
भावोदयः- एक भाव की शान्ति के पश्चात् दूसरे भाव का उदय भावोदय कहलाता है। यथा-चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराङ्मुखे, निभृत कितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते। व्रजति रमणे निश्वासितस्योच्चैः स्तनस्थितहस्तया, नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेषिता। यहाँ नायक के अनुनय को स्वीकार न करने पर तथा रुष्ट होकर उसे लौटते हुए देखकर नायिका के विषादभाव का उदय व्यञ्जित है। (3/244)
भावोदयः- एक अर्थालङ्कार। जहाँ भावोदय किसी अन्य का अङ्ग बनकर आये, वहाँ भावोदय नामक अलङ्कार होता है। यथा-मधुपानप्रवृत्तस्ते सुहृद्भिः सह वैरिणः। श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्।। इस पद्य में त्रासादि सञ्चारीभाव राजविषयक रतिभाव के अङ्ग हैं। (10/125)
भाषणम्-निर्वहण सन्धि का एक अङ्ग। सामदानादि को भाषण कहा जाता है-सामदानादि भाषणम्। यथा च. कौ. में "धर्म:- तदेहि धर्मलोकमधितिष्ठ'। यहाँ साम का प्रयोग है। (6/134)