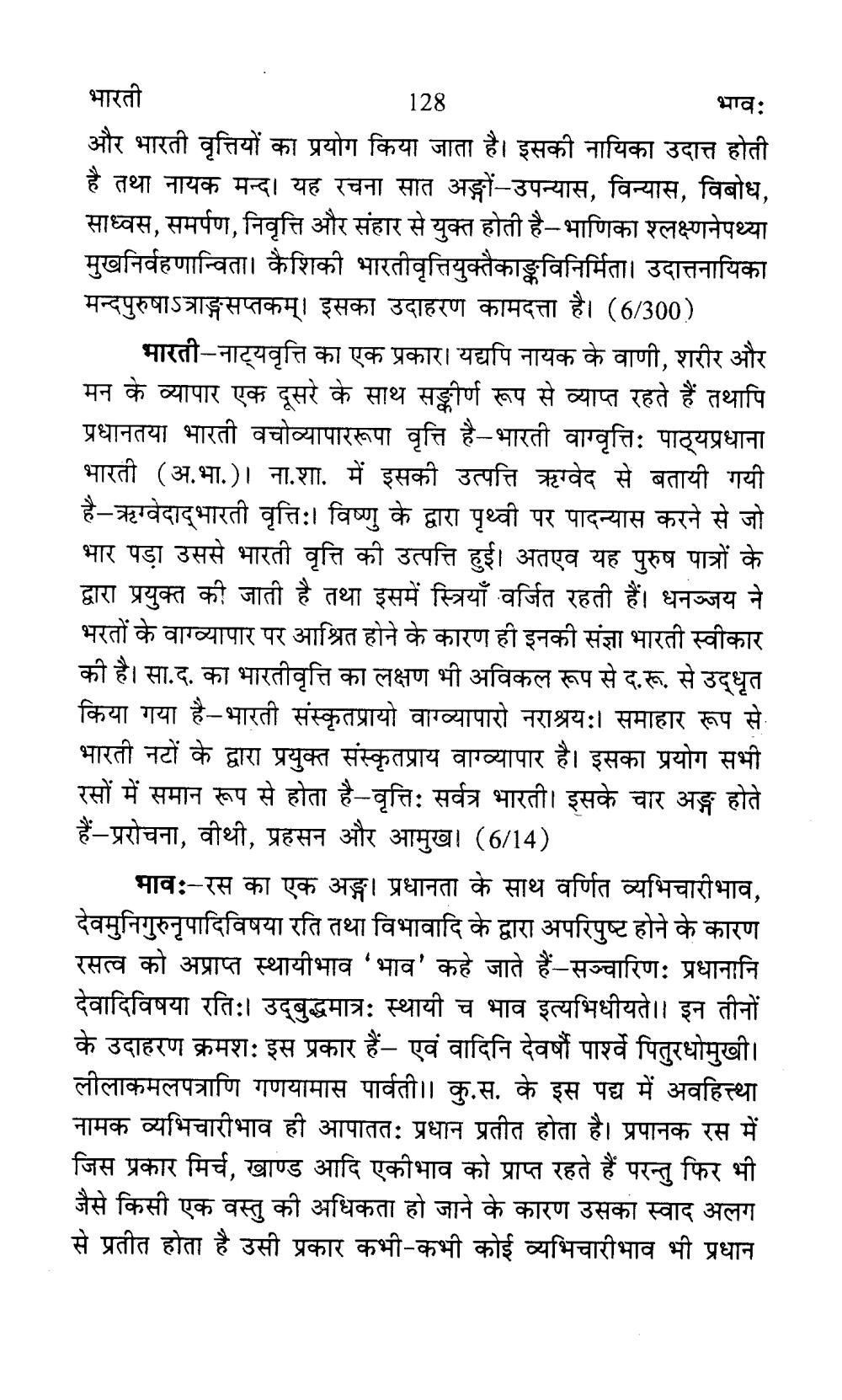________________
भारती
128
भाव:
और भारती वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी नायिका उदात्त होती है तथा नायक मन्द। यह रचना सात अङ्गों - उपन्यास, विन्यास, विबोध, साध्वस, समर्पण, निवृत्ति और संहार से युक्त होती है-भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्या मुखनिर्वहणान्विता । कैशिकी भारतीवृत्तियुक्तैकाङ्कविनिर्मिता । उदात्तनायिका मन्दपुरुषाऽत्राङ्गसप्तकम् । इसका उदाहरण कामदत्ता है। (6/300)
भारती - नाट्यवृत्ति का एक प्रकार । यद्यपि नायक के वाणी, शरीर और मन के व्यापार एक दूसरे के साथ सङ्कीर्ण रूप से व्याप्त रहते हैं तथापि प्रधानतया भारती वचोव्यापाररूपा वृत्ति है- भारती वाग्वृत्तिः पाठ्यप्रधाना भारती ( अ.भा.) । ना.शा. में इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से बतायी गयी है - ऋग्वेदाद्भारती वृत्तिः । विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर पादन्यास करने से जो भार पड़ा उससे भारती वृत्ति की उत्पत्ति हुई । अतएव यह पुरुष पात्रों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है तथा इसमें स्त्रियाँ वर्जित रहती हैं। धनञ्जय ने भरतों के वाग्व्यापार पर आश्रित होने के कारण ही इनकी संज्ञा भारती स्वीकार की है। सा.द. का भारतीवृत्ति का लक्षण भी अविकल रूप से द.रू. से उद्धृत किया गया है - भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः । समाहार रूप से भारती नटों के द्वारा प्रयुक्त संस्कृतप्राय वाग्व्यापार है। इसका प्रयोग सभी रसों में समान रूप से होता है - वृत्तिः सर्वत्र भारती । इसके चार अङ्ग होते हैं- प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख | ( 6/14)
भावः- रस का एक अङ्ग । प्रधानता के साथ वर्णित व्यभिचारीभाव, देवमुनिगुरुनृपादिविषया रति तथा विभावादि के द्वारा अपरिपुष्ट होने के कारण रसत्व को अप्राप्त स्थायीभाव 'भाव' कहे जाते हैं- सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । उबुद्धमात्र ः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । । इन तीनों के उदाहरण क्रमश: इस प्रकार हैं- एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी । लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।। कु.स. के इस पद्य में अवहित्त्था नामक व्यभिचारीभाव ही आपाततः प्रधान प्रतीत होता है। प्रपानक रस में जिस प्रकार मिर्च, खाण्ड आदि एकीभाव को प्राप्त रहते हैं परन्तु फिर भी जैसे किसी एक वस्तु की अधिकता हो जाने के कारण उसका स्वाद अलग से प्रतीत होता है उसी प्रकार कभी-कभी कोई व्यभिचारीभाव भी प्रधान