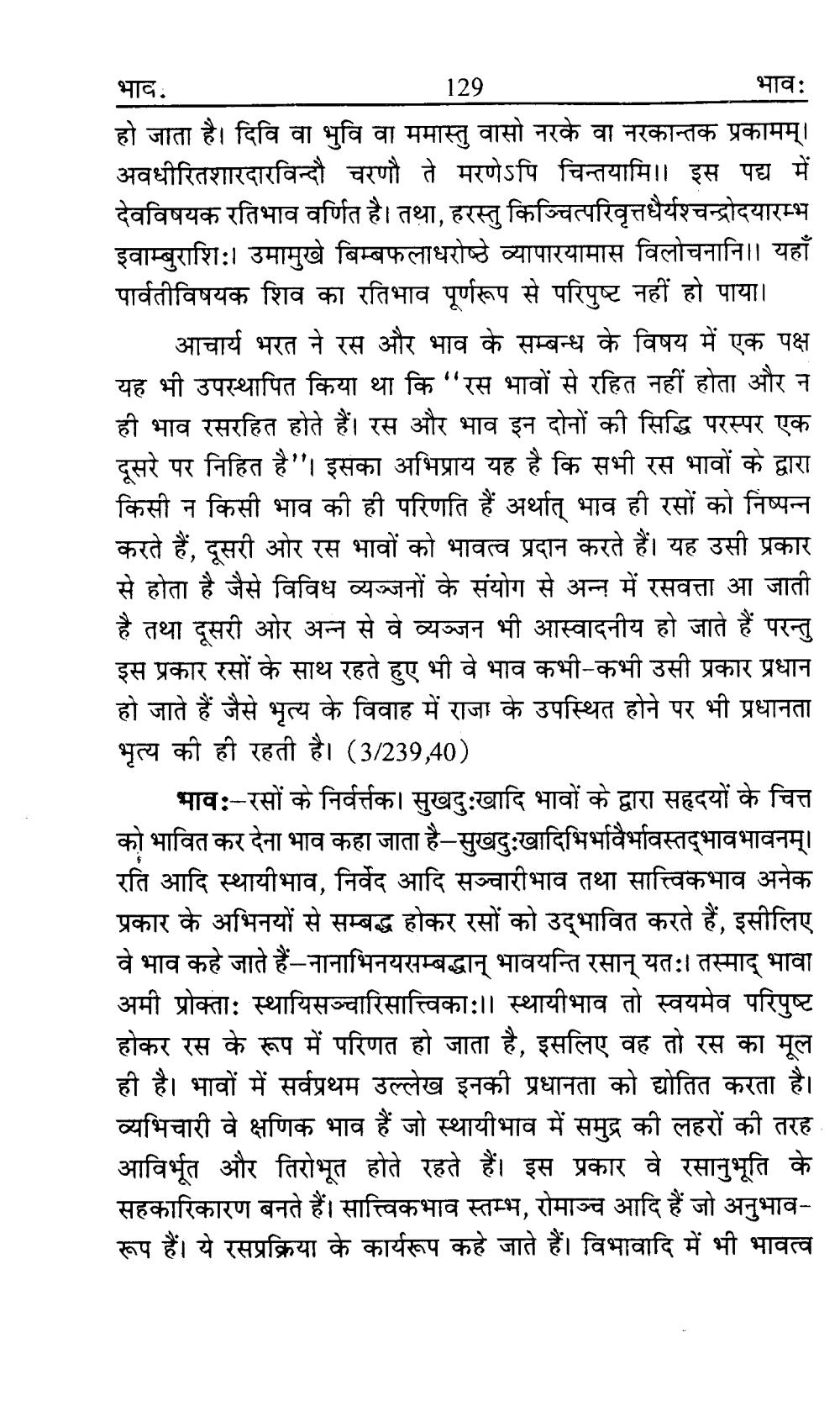________________
भाव.
129
भाव:
हो जाता है। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्। अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि।। इस पद्य में देवविषयक रतिभाव वर्णित है। तथा, हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि।। यहाँ पार्वतीविषयक शिव का रतिभाव पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीं हो पाया।
आचार्य भरत ने रस और भाव के सम्बन्ध के विषय में एक पक्ष यह भी उपस्थापित किया था कि "रस भावों से रहित नहीं होता और न ही भाव रसरहित होते हैं। रस और भाव इन दोनों की सिद्धि परस्पर एक दूसरे पर निहित है'। इसका अभिप्राय यह है कि सभी रस भावों के द्वारा किसी न किसी भाव की ही परिणति हैं अर्थात् भाव ही रसों को निष्पन्न करते हैं, दूसरी ओर रस भावों को भावत्व प्रदान करते हैं। यह उसी प्रकार से होता है जैसे विविध व्यञ्जनों के संयोग से अन्न में रसवत्ता आ जाती है तथा दूसरी ओर अन्न से वे व्यञ्जन भी आस्वादनीय हो जाते हैं परन्तु इस प्रकार रसों के साथ रहते हुए भी वे भाव कभी-कभी उसी प्रकार प्रधान हो जाते हैं जैसे भृत्य के विवाह में राजा के उपस्थित होने पर भी प्रधानता भृत्य की ही रहती है। (3/239,40) ___ भाव:-रसों के निर्वर्त्तक। सुखदुःखादि भावों के द्वारा सहृदयों के चित्त को भावित कर देना भाव कहा जाता है-सुखदुःखादिभिर्भावैर्भावस्तद्भावभावनम्। रति आदि स्थायीभाव, निर्वेद आदि सञ्चारीभाव तथा सात्त्विकभाव अनेक प्रकार के अभिनयों से सम्बद्ध होकर रसों को उद्भावित करते हैं, इसीलिए वे भाव कहे जाते हैं-नानाभिनयसम्बद्धान् भावयन्ति रसान् यतः। तस्माद् भावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसञ्चारिसात्त्विकाः।। स्थायीभाव तो स्वयमेव परिपुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए वह तो रस का मूल ही है। भावों में सर्वप्रथम उल्लेख इनकी प्रधानता को द्योतित करता है। व्यभिचारी वे क्षणिक भाव हैं जो स्थायीभाव में समुद्र की लहरों की तरह आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। इस प्रकार वे रसानुभूति के सहकारिकारण बनते हैं। सात्त्विकभाव स्तम्भ, रोमाञ्च आदि हैं जो अनुभावरूप हैं। ये रसप्रक्रिया के कार्यरूप कहे जाते हैं। विभावादि में भी भावत्व