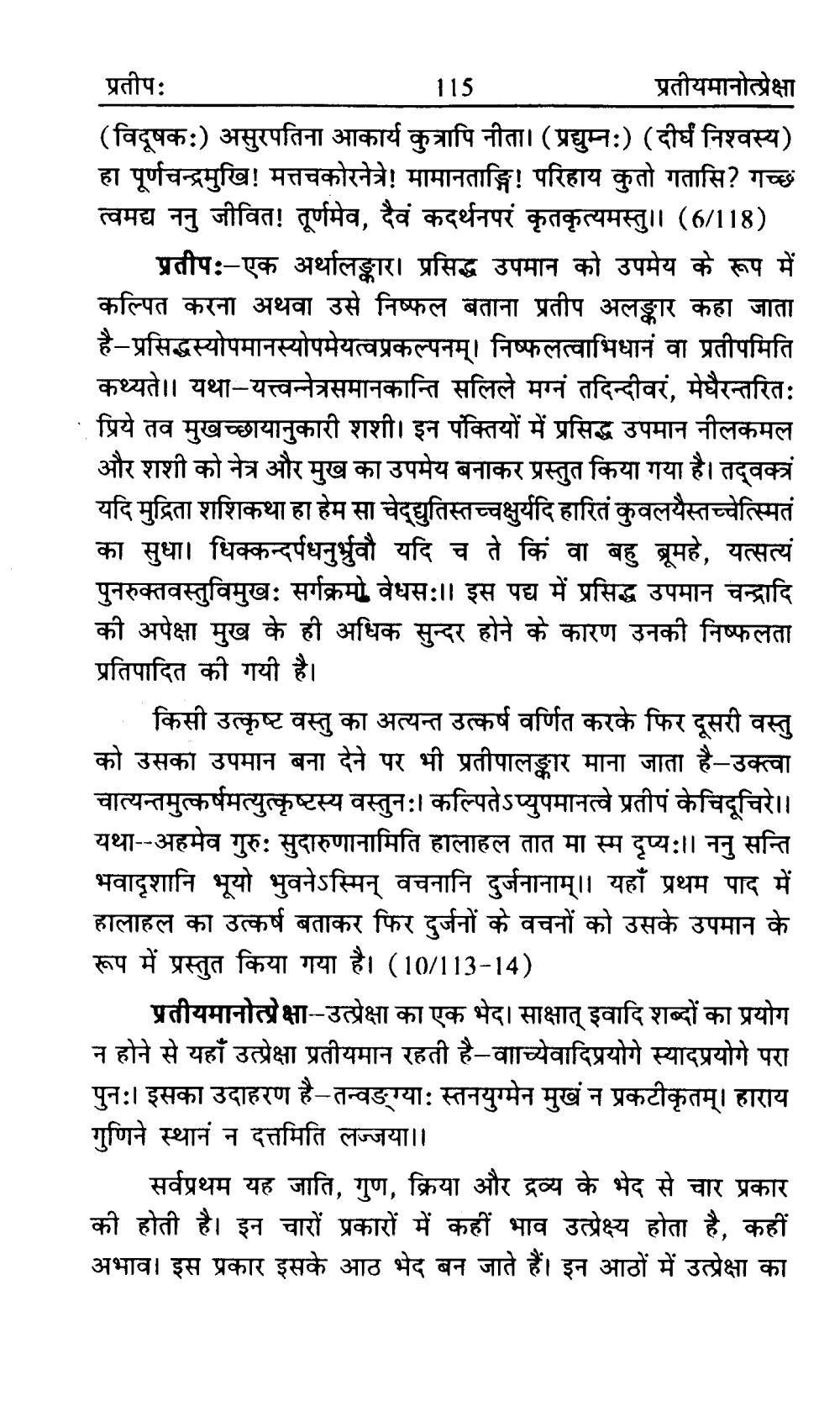________________
115
प्रतीप:
प्रतीयमानोत्प्रेक्षा (विदूषकः) असुरपतिना आकार्य कुत्रापि नीता। (प्रद्युम्नः) (दीर्घ निश्वस्य) हा पूर्णचन्द्रमुखि! मत्तचकोरनेत्रे! मामानताङ्गि! परिहाय कुतो गतासि? गच्छ त्वमद्य ननु जीवित! तूर्णमेव, दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु।। (6/118)
प्रतीप:-एक अर्थालङ्कार। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित करना अथवा उसे निष्फल बताना प्रतीप अलङ्कार कहा जाता है-प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्। निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते।। यथा-यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं, मेधैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध उपमान नीलकमल
और शशी को नेत्र और मुख का उपमेय बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तद्वक्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्द्युतिस्तच्चक्षुर्यदि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्स्मितं का सुधा। धिक्कन्दर्पधनुर्भुवौ यदि च ते किं वा बहु ब्रूमहे, यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमो वेधसः।। इस पद्य में प्रसिद्ध उपमान चन्द्रादि की अपेक्षा मुख के ही अधिक सुन्दर होने के कारण उनकी निष्फलता प्रतिपादित की गयी है।
किसी उत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वर्णित करके फिर दूसरी वस्तु को उसका उपमान बना देने पर भी प्रतीपालङ्कार माना जाता है-उक्त्वा चात्यन्तमुत्कर्षमत्युत्कृष्टस्य वस्तुनः। कल्पितेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे।। यथा--अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म दृप्यः।। ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम्।। यहाँ प्रथम पाद में हालाहल का उत्कर्ष बताकर फिर दुर्जनों के वचनों को उसके उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (10/113-14)
प्रतीयमानोत्प्रेक्षा-उत्प्रेक्षा का एक भेद। साक्षात् इवादि शब्दों का प्रयोग न होने से यहाँ उत्प्रेक्षा प्रतीयमान रहती है-वााच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः। इसका उदाहरण है-तन्वङ्ग्याः स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकटीकृतम्। हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया।।
सर्वप्रथम यह जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के भेद से चार प्रकार की होती है। इन चारों प्रकारों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य होता है, कहीं अभाव। इस प्रकार इसके आठ भेद बन जाते हैं। इन आठों में उत्प्रेक्षा का