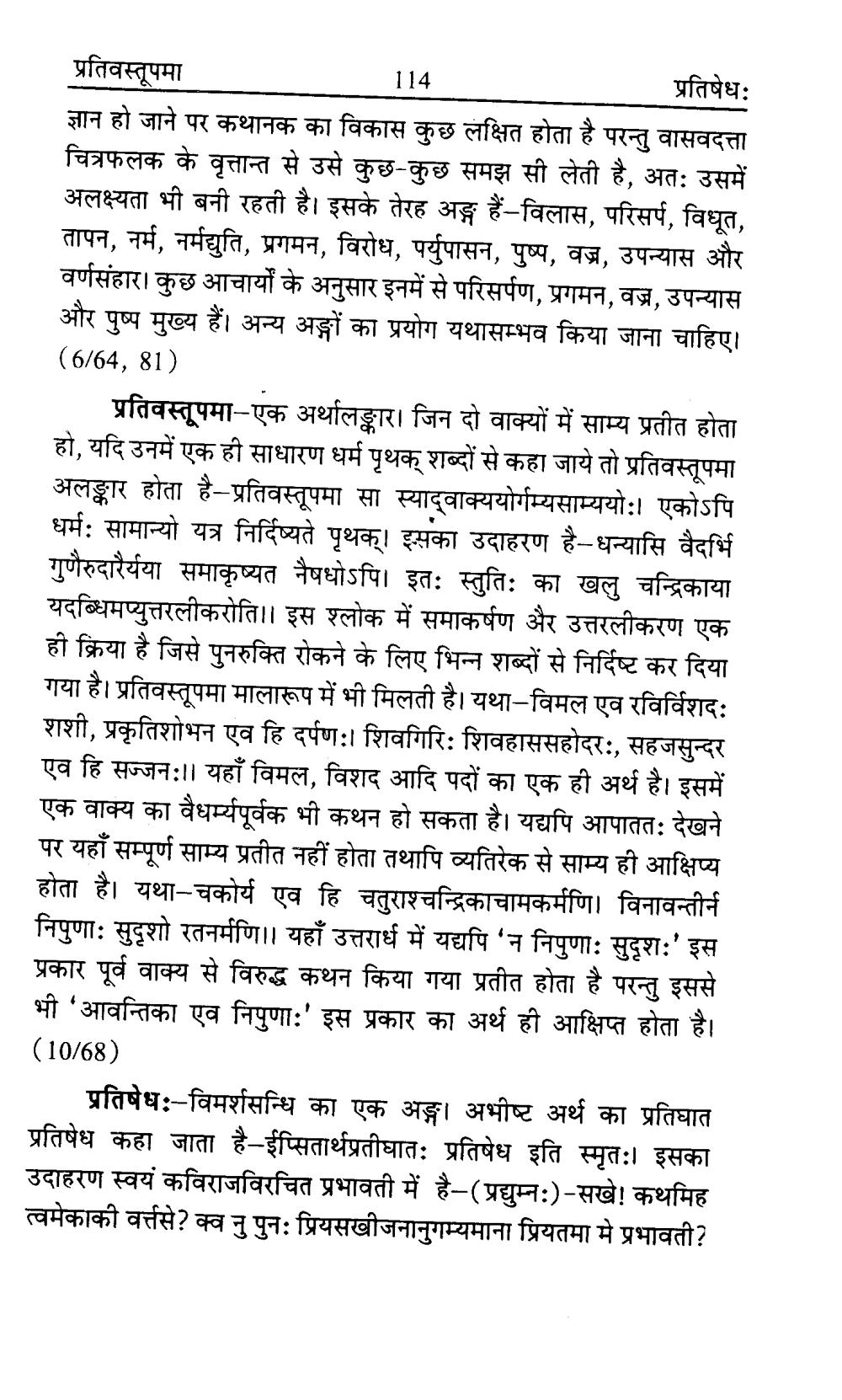________________
114
प्रतिवस्तूपमा
प्रतिषेधः ज्ञान हो जाने पर कथानक का विकास कुछ लक्षित होता है परन्तु वासवदत्ता चित्रफलक के वृत्तान्त से उसे कुछ-कुछ समझ सी लेती है, अतः उसमें अलक्ष्यता भी बनी रहती है। इसके तेरह अङ्ग हैं-विलास, परिसर्प, विधूत, तापन, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास और वर्णसंहार। कुछ आचार्यों के अनुसार इनमें से परिसर्पण, प्रगमन, वज्र, उपन्यास
और पुष्प मुख्य हैं। अन्य अङ्गों का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिए। (6/64, 81)
प्रतिवस्तूपमा-एक अर्थालङ्कार। जिन दो वाक्यों में साम्य प्रतीत होता हो, यदि उनमें एक ही साधारण धर्म पृथक् शब्दों से कहा जाये तो प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार होता है-प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोर्गम्यसाम्ययोः। एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिष्यते पृथक्। इसका उदाहरण है-धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारैर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि। इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति।। इस श्लोक में समाकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही क्रिया है जिसे पुनरुक्ति रोकने के लिए भिन्न शब्दों से निर्दिष्ट कर दिया गया है। प्रतिवस्तूपमा मालारूप में भी मिलती है। यथा-विमल एव रविर्विशदः शशी, प्रकृतिशोभन एव हि दर्पण:। शिवगिरिः शिवहाससहोदरः, सहजसुन्दर एव हि सज्जनः।। यहाँ विमल, विशद आदि पदों का एक ही अर्थ है। इसमें एक वाक्य का वैधर्म्यपूर्वक भी कथन हो सकता है। यद्यपि आपाततः देखने पर यहाँ सम्पूर्ण साम्य प्रतीत नहीं होता तथापि व्यतिरेक से साम्य ही आक्षिप्य होता है। यथा-चकोर्य एव हि चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि। विनावन्तीन निपुणाः सुदृशो रतनर्मणि।। यहाँ उत्तरार्ध में यद्यपि 'न निपुणाः सुदृशः' इस प्रकार पूर्व वाक्य से विरुद्ध कथन किया गया प्रतीत होता है परन्तु इससे भी 'आवन्तिका एव निपुणाः' इस प्रकार का अर्थ ही आक्षिप्त होता है। (10/68)
प्रतिषेधः-विमर्शसन्धि का एक अङ्ग। अभीष्ट अर्थ का प्रतिघात प्रतिषेध कहा जाता है-ईप्सितार्थप्रतीघातः प्रतिषेध इति स्मृतः। इसका उदाहरण स्वयं कविराजविरचित प्रभावती में है-(प्रद्युम्न:)-सखे! कथमिह त्वमेकाकी वर्त्तसे? क्व नु पुनः प्रियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती?