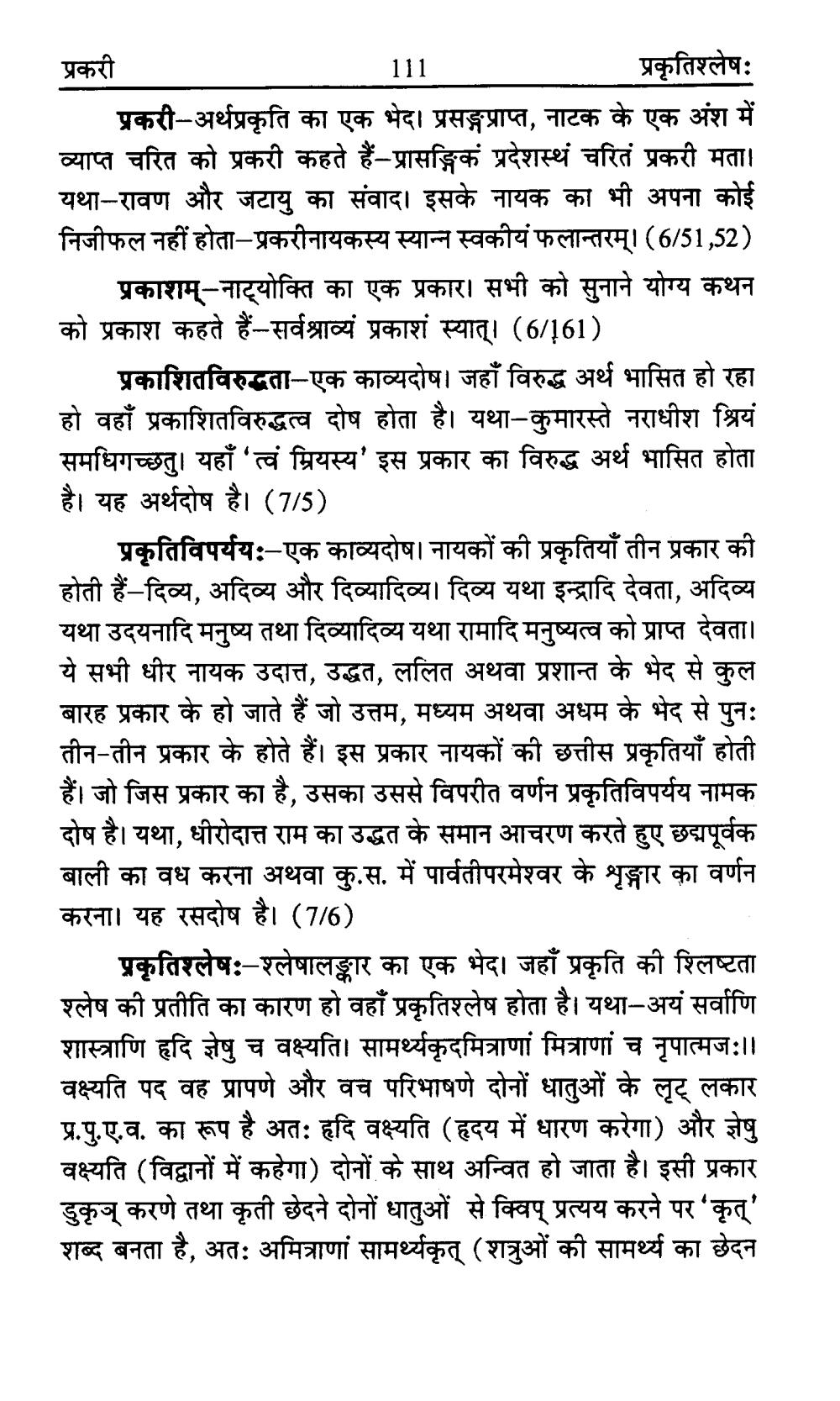________________
प्रकरी
111
प्रकृतिश्लेषः प्रकरी-अर्थप्रकृति का एक भेद। प्रसङ्गप्राप्त, नाटक के एक अंश में व्याप्त चरित को प्रकरी कहते हैं-प्रासङ्गिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता। यथा-रावण और जटायु का संवाद। इसके नायक का भी अपना कोई निजीफल नहीं होता-प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्। (6/51,52)
प्रकाशम्-नाट्योक्ति का एक प्रकार। सभी को सुनाने योग्य कथन को प्रकाश कहते हैं-सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्। (6/161)
प्रकाशितविरुद्धता-एक काव्यदोष। जहाँ विरुद्ध अर्थ भासित हो रहा हो वहाँ प्रकाशितविरुद्धत्व दोष होता है। यथा-कुमारस्ते नराधीश श्रियं समधिगच्छतु। यहाँ त्वं म्रियस्य' इस प्रकार का विरुद्ध अर्थ भासित होता है। यह अर्थदोष है। (7/5)
प्रकृतिविपर्ययः-एक काव्यदोष। नायकों की प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं-दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। दिव्य यथा इन्द्रादि देवता, अदिव्य यथा उदयनादि मनुष्य तथा दिव्यादिव्य यथा रामादि मनुष्यत्व को प्राप्त देवता। ये सभी धीर नायक उदात्त, उद्धत, ललित अथवा प्रशान्त के भेद से कुल बारह प्रकार के हो जाते हैं जो उत्तम, मध्यम अथवा अधम के भेद से पुनः तीन-तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार नायकों की छत्तीस प्रकृतियाँ होती हैं। जो जिस प्रकार का है, उसका उससे विपरीत वर्णन प्रकृतिविपर्यय नामक दोष है। यथा, धीरोदात्त राम का उद्धत के समान आचरण करते हुए छद्मपूर्वक बाली का वध करना अथवा कु.स. में पार्वतीपरमेश्वर के शृङ्गार का वर्णन करना। यह रसदोष है। (76)
प्रकृतिश्लेषः-श्लेषालङ्कार का एक भेद। जहाँ प्रकृति की श्लिष्टता श्लेष की प्रतीति का कारण हो वहाँ प्रकृतिश्लेष होता है। यथा-अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति। सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः।। वक्ष्यति पद वह प्रापणे और वच परिभाषणे दोनों धातुओं के लृट् लकार प्र.पु.ए.व. का रूप है अतः हृदि वक्ष्यति (हृदय में धारण करेगा) और ज्ञेषु वक्ष्यति (विद्वानों में कहेगा) दोनों के साथ अन्वित हो जाता है। इसी प्रकार डुकृञ् करणे तथा कृती छेदने दोनों धातुओं से क्विप् प्रत्यय करने पर कृत्' शब्द बनता है, अत: अमित्राणां सामर्थ्यकृत् (शत्रुओं की सामर्थ्य का छेदन