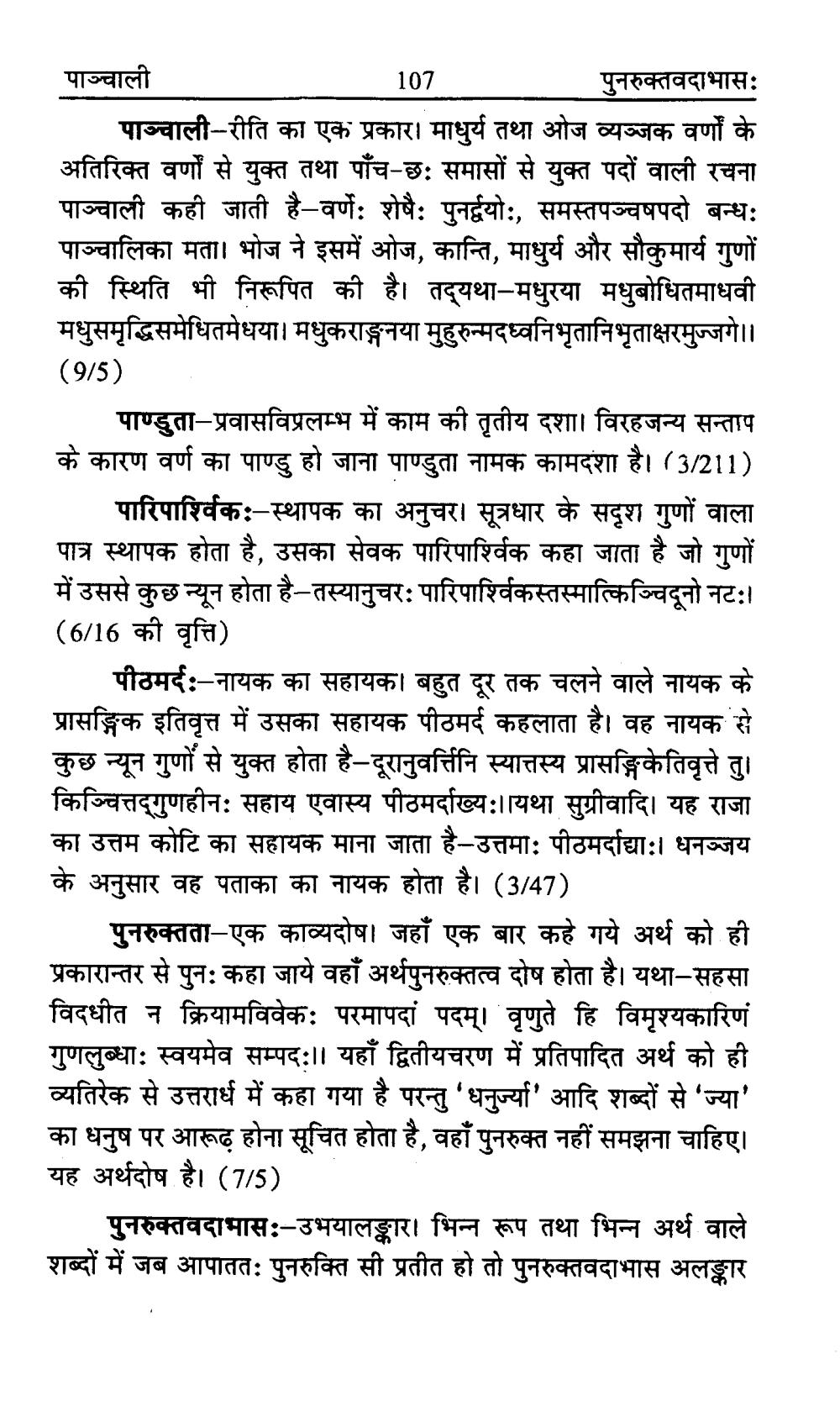________________
107
पाञ्चाली
पुनरुक्तवदाभासः पाञ्चाली-रीति का एक प्रकार। माधुर्य तथा ओज व्यञ्जक वर्गों के अतिरिक्त वर्णों से युक्त तथा पाँच-छ: समासों से युक्त पदों वाली रचना पाञ्चाली कही जाती है-वर्णेः शेषैः पुनर्द्वयोः, समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता। भोज ने इसमें ओज, कान्ति, माधुर्य और सौकुमार्य गुणों की स्थिति भी निरूपित की है। तद्यथा-मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया। मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृतानिभृताक्षरमुज्जगे।। (9/5)
पाण्डुता-प्रवासविप्रलम्भ में काम की तृतीय दशा। विरहजन्य सन्ताप के कारण वर्ण का पाण्डु हो जाना पाण्डुता नामक कामदंशा है। (3/211)
पारिपार्श्विकः-स्थापक का अनुचर। सूत्रधार के सदृश गुणों वाला पात्र स्थापक होता है, उसका सेवक पारिपार्श्विक कहा जाता है जो गुणों में उससे कुछ न्यून होता है-तस्यानुचरः पारिपार्श्विकस्तस्मात्किञ्चिदूनो नटः। (6/16 की वृत्ति)
पीठमर्द:-नायक का सहायक। बहुत दूर तक चलने वाले नायक के प्रासङ्गिक इतिवृत्त में उसका सहायक पीठमर्द कहलाता है। वह नायक से कुछ न्यून गुणों से युक्त होता है-दूरानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्रासङ्गिकेतिवृत्ते तु। किञ्चित्तद्गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमाख्यः। यथा सुग्रीवादि। यह राजा का उत्तम कोटि का सहायक माना जाता है-उत्तमाः पीठमर्दाद्याः। धनञ्जय के अनुसार वह पताका का नायक होता है। (3/47)
पुनरुक्तता-एक काव्यदोष। जहाँ एक बार कहे गये अर्थ को ही प्रकारान्तर से पुनः कहा जाये वहाँ अर्थपुनरुक्तत्व दोष होता है। यथा-सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्। वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः।। यहाँ द्वितीयचरण में प्रतिपादित अर्थ को ही व्यतिरेक से उत्तरार्ध में कहा गया है परन्तु 'धना' आदि शब्दों से 'ज्या' का धनुष पर आरूढ़ होना सूचित होता है, वहाँ पुनरुक्त नहीं समझना चाहिए। यह अर्थदोष है। (7/5)
पुनरुक्तवदाभासः-उभयालङ्कार। भिन्न रूप तथा भिन्न अर्थ वाले शब्दों में जब आपाततः पुनरुक्ति सी प्रतीत हो तो पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार