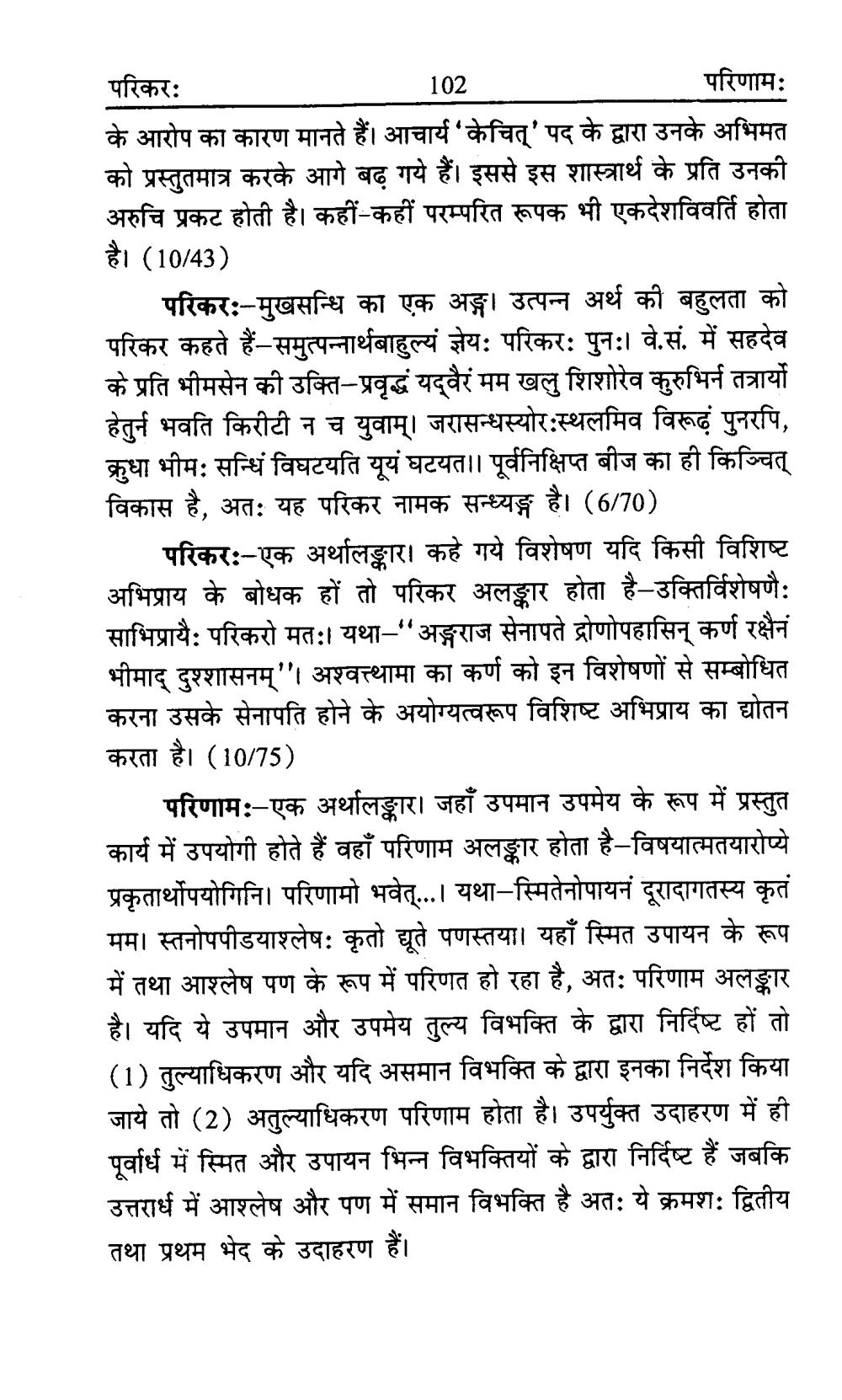________________
परिकरः
102
परिणामः
को
के आरोप का कारण मानते हैं। आचार्य ' केचित्' पद के द्वारा उनके अभिमत प्रस्तुतमात्र करके आगे बढ़ गये हैं। इससे इस शास्त्रार्थ के प्रति उनकी अरुचि प्रकट होती है। कहीं-कहीं परम्परित रूपक भी एकदेशविवर्ति होता है। (10/43)
परिकरः- मुखसन्धि का एक अङ्ग । उत्पन्न अर्थ की बहुलता को परिकर कहते हैं - समुत्पन्नार्थबाहुल्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः । वे.सं. में सहदेव के प्रति भीमसेन की उक्ति - प्रवृद्धं यद्वैरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिर्न तत्रार्यो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम् । जरासन्धस्योर:स्थलमिव विरूढं पुनरपि, क्रुधा भीमः सन्धिं विघटयति यूयं घटयत ।। पूर्वनिक्षिप्त बीज का ही किञ्चित् विकास है, अतः यह परिकर नामक सन्ध्यङ्ग है। (6/70)
परिकरः- एक अर्थालङ्कार । कहे गये विशेषण यदि किसी विशिष्ट अभिप्राय के बोधक हों तो परिकर अलङ्कार होता है- उक्तिर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः । यथा - " अङ्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन् कर्ण रक्षैनं भीमाद् दुश्शासनम्''। अश्वत्थामा का कर्ण को इन विशेषणों से सम्बोधित करना उसके सेनापति होने के अयोग्यत्वरूप विशिष्ट अभिप्राय का द्योतन करता है। ( 10/75)
परिणाम :- एक अर्थालङ्कार । जहाँ उपमान उपमेय के रूप में प्रस्तुत कार्य में उपयोगी होते हैं वहाँ परिणाम अलङ्कार होता है - विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि । परिणामो भवेत्... । यथा - स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृतं मम। स्तनोपपीडयाश्लेषः कृतो द्यूते पणस्तया । यहाँ स्मित उपायन के रूप में तथा आश्लेष पण के रूप में परिणत हो रहा है, अत: परिणाम अलङ्कार है। यदि ये उपमान और उपमेय तुल्य विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट हों तो (1) तुल्याधिकरण और यदि असमान विभक्ति के द्वारा इनका निर्देश किया जाये तो ( 2 ) अतुल्याधिकरण परिणाम होता है। उपर्युक्त उदाहरण में ही पूर्वार्ध में स्मित और उपायन भिन्न विभक्तियों के द्वारा निर्दिष्ट हैं जबकि उत्तरार्ध में आश्लेष और पण में समान विभक्ति है अतः ये क्रमशः द्वितीय तथा प्रथम भेद के उदाहरण हैं।