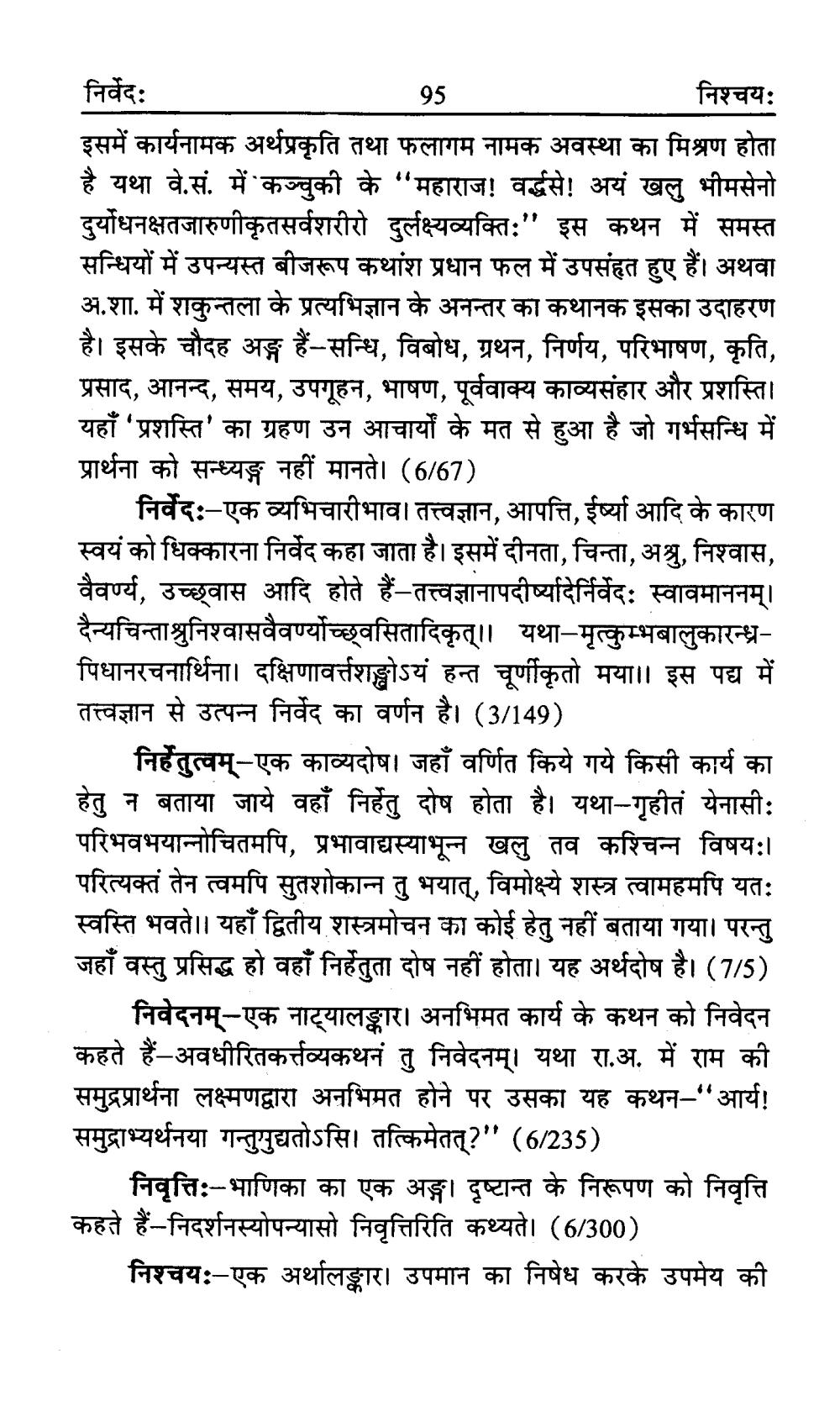________________
निर्वेद:
निश्चयः
95
इसमें कार्यनामक अर्थप्रकृति तथा फलागम नामक अवस्था का मिश्रण होता है यथा वे.सं. में कञ्चुकी के "महाराज ! वर्द्धसे ! अयं खलु भीमसेनो दुर्योधनक्षतजारुणीकृतसर्वशरीरो दुर्लक्ष्यव्यक्तिः " इस कथन में समस्त सन्धियों में उपन्यस्त बीजरूप कथांश प्रधान फल में उपसंहृत हुए हैं। अथवा अ.शा. में शकुन्तला के प्रत्यभिज्ञान के अनन्तर का कथानक इसका उदाहरण है। इसके चौदह अङ्ग हैं- सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, कृति, प्रसाद, आनन्द, समय, उपगूहन, भाषण, पूर्ववाक्य काव्यसंहार और प्रशस्ति । यहाँ 'प्रशस्ति' का ग्रहण उन आचार्यों के मत से हुआ है जो गर्भसन्धि में प्रार्थना को सन्ध्यङ्ग नहीं मानते। (6/67)
निर्वेद:- एक व्यभिचारी भाव । तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या आदि के कारण स्वयं को धिक्कारना निर्वेद कहा जाता है। इसमें दीनता, चिन्ता, अश्रु, निश्वास, वैवर्ण्य, उच्छ्वास आदि होते हैं - तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यादेर्निर्वेदः स्वावमाननम् । दैन्यचिन्ताश्रुनिश्वासवैवर्ण्योच्छ्वसितादिकृत् ।। यथा—मृत्कुम्भबालुकारन्ध्रपिधानरचनार्थिना । दक्षिणावर्त्तशङ्खोऽयं हन्त चूर्णीकृतो मया । । इस पद्य में तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद का वर्णन है । (3/149)
निर्हेतुत्वम् - एक काव्यदोष । जहाँ वर्णित किये गये किसी कार्य का हेतु न बताया जाये वहाँ निर्हेतु दोष होता है। यथा - गृहीतं येनासी: परिभवभयान्नोचितमपि, प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः । परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भयात्, विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ।। यहाँ द्वितीय शस्त्रमोचन का कोई हेतु नहीं बताया गया। परन्तु जहाँ वस्तु प्रसिद्ध हो वहाँ निर्हेतुता दोष नहीं होता। यह अर्थदोष है । (7/5)
निवेदनम्-एक नाट्यालङ्कार। अनभिमत कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं-अवधीरितकर्त्तव्यकथनं तु निवेदनम् । यथा रा.अ. में राम की समुद्रप्रार्थना लक्ष्मणद्वारा अनभिमत होने पर उसका यह कथन - " आर्य! समुद्राभ्यर्थनया गन्तुमुद्यतोऽसि । तत्किमेतत् ?" (6/235)
निवृत्तिः- भाणिका का एक अङ्ग । दृष्टान्त के निरूपण को निवृत्ति कहते हैं - निदर्शनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते । (6/300)
निश्चय :- एक अर्थालङ्कार । उपमान का निषेध करके उपमेय की