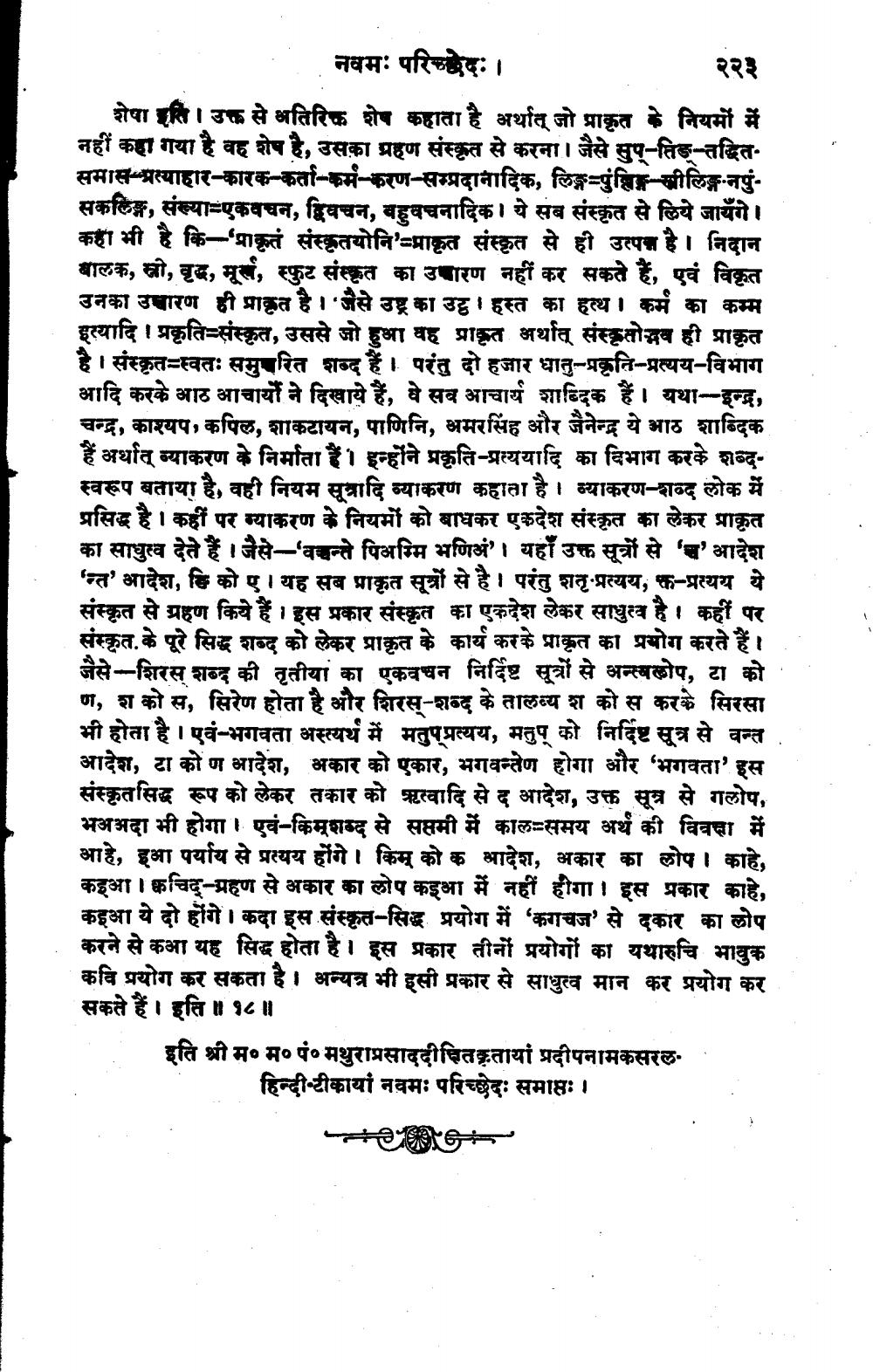________________
२२३
- नवमः परिच्छेदः। शेषा इति । उक्त से अतिरिक्त शेष कहाता है अर्थात् जो प्राकृत के नियमों में नहीं कहा गया है वह शेष है, उसका ग्रहण संस्कृत से करना। जैसे सुप-तिङ्-तद्धितसमास प्रत्याहार-कारक कर्ता-कर्म-करण-सम्प्रदानादिक, लिङ्ग-पुंलिङ्ग-सीलिङ्ग-नपुं. सकलिङ्ग, संख्या एकवचन, द्विवचन, बहुवचनादिक। ये सब संस्कृत से लिये जायेंगे। कहा भी है कि-'प्राकृतं संस्कृतयोनि' प्राकृत संस्कृत से ही उत्पन है। निदान बालक, नो, वृद्ध, मूर्ख, स्फुट संस्कृत का उचारण नहीं कर सकते हैं, एवं विकृत उनका उच्चारण ही प्राकृत है। जैसे उष्ट्र का उह । हस्त का हत्थ। कर्म का कम्म इत्यादि । प्रकृति-संस्कृत, उससे जो हुआ वह प्राकृत अर्थात् संस्कृतोद्भव ही प्राकृत है। संस्कृत-स्वतः समुपरित शब्द हैं। परंतु दो हजार धातु-प्रकृति-प्रत्यय-विभाग आदि करके आठ आचार्यों ने दिखाये हैं, वे सब आचार्य शाब्दिक हैं। यथा-इन्द्र, चन्द्र, काश्यप, कपिल, शाकटायन, पाणिनि, अमरसिंह और जैनेन्द्र ये आठ शाब्दिक हैं अर्थात् व्याकरण के निर्माता हैं। इन्होंने प्रकृति-प्रत्ययादि का विभाग करके शब्दस्वरूप बताया है, वही नियम सूत्रादि व्याकरण कहाता है। व्याकरण-शब्द लोक में प्रसिद्ध है। कहीं पर व्याकरण के नियमों को बाधकर एकदेश संस्कृत का लेकर प्राकृत का साधुत्व देते हैं । जैसे-'वञ्चन्ते पिअम्मि भणि'। यहाँ उक्त सूत्रों से 'च' आदेश 'न्त' आदेश, हि को ए। यह सब प्राकृत सूत्रों से है। परंतु शतृ प्रत्यय, क-प्रत्यय ये संस्कृत से ग्रहण किये हैं। इस प्रकार संस्कृत का एकदेश लेकर साधुत्व है। कहीं पर संस्कृत.के पूरे सिद्ध शब्द को लेकर प्राकृत के कार्य करके प्राकृत का प्रयोग करते हैं। जैसे-शिरस शब्द की तृतीया का एकवचन निर्दिष्ट सूत्रों से अन्त्यलोप, टा को .. ण, श को स, सिरेण होता है और शिरस्-शब्द के तालव्य श को स करके सिरसा भी होता है । एवं-भगवता अस्त्यर्थ में मतुपप्रत्यय, मतुप को निर्दिष्ट सूत्र से वन्त . आदेश, टा को ण आदेश, अकार को एकार, भगवन्तण होगा और 'भगवता' इस संस्कृतसिद्ध रूप को लेकर तकार को ऋत्वादि से द आदेश, उक्त सूत्र से गलोप, भअअदा भी होगा। एवं-किमशब्द से सप्तमी में कालम्समय अर्थ की विवक्षा में आहे, इा पर्याय से प्रत्यय होंगे। किम् को क आदेश, अकार का लोप। काहे, कहा। कचिद्-ग्रहण से अकार का लोप कइआ में नहीं होगा। इस प्रकार काहे, कइआ ये दो होंगे। कदा इस संस्कृत-सिद्ध प्रयोग में 'कगचज' से दकार का लोप करने से का यह सिद्ध होता है। इस प्रकार तीनों प्रयोगों का यथारुचि भावुक कवि प्रयोग कर सकता है। अन्यत्र भी इसी प्रकार से साधुत्व मान कर प्रयोग कर सकते हैं। इति ॥ १८॥ इति श्रीम०म०६० मथुराप्रसाददीक्षितकृतायां प्रदीपनामकसरल. हिन्दी-टीकायां नवमः परिच्छेदः समाप्तः ।
+ G