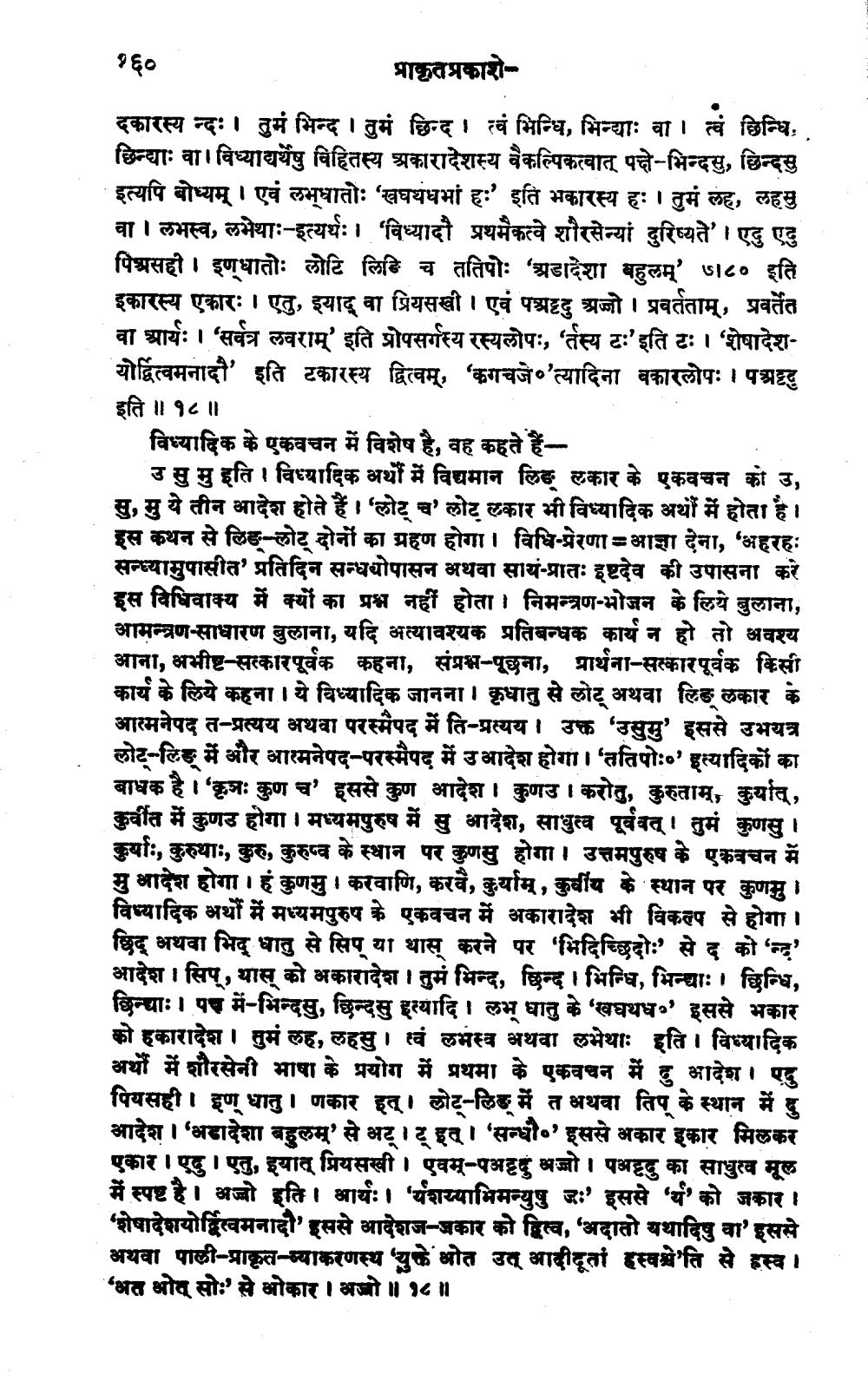________________
१६०
प्राकृतप्रकाशेदकारस्य न्दः। तुम भिन्द । तुमं छिन्द । त्वं भिन्धि, भिन्द्याः वा। त्वं छिन्धि, , छिन्द्याः वा। विध्याद्यर्थेषु विहितस्य प्रकारादेशस्य वैकल्पिकत्वात् पक्ष-भिन्दसु, छिन्दसु इत्यपि बोध्यम् । एवं लभ्धातोः 'खघयधभां हः' इति भकारस्य हः । तुम लह, लहसु वा । लभस्व, लभेथाः-इत्यर्थः। “विध्यादौ प्रथमैकत्वे शौरसेन्यां दुरिष्यते' । एदु एदु पिअसही। इणधातोः लोटि लिङि च ततिपोः 'अडादेशा बहुलम' ७८० इति इकारस्य एकारः । एतु, इयाद् वा प्रियसखी । एवं पट्टदु अज्जो । प्रवर्तताम्, प्रवर्तेत वा आर्यः । 'सर्वत्र लवराम्' इति प्रोपसर्गस्य रस्यलोपः, 'तस्य टः' इति टः । 'शेषादेशयोद्वित्वमनादौ' इति टकारस्य द्वित्वम्, 'कगचजे०'त्यादिना वकारलोपः । पअदु इति ॥१८॥
विध्यादिक के एकवचन में विशेष है, वह कहते हैं
उसुमु इति । विध्यादिक अर्थों में विद्यमान लिङ्ग लकार के एकवचन को उ, सु, मु ये तीन आदेश होते हैं । 'लोट् च' लोट लकार भी विध्यादिक अर्थों में होता है। इस कथन से लिङ्ग-लोट् दोनों का ग्रहण होगा। विधि-प्रेरणा=आज्ञा देना, 'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' प्रतिदिन सन्धयोपासन अथवा सायं-प्रातः इष्टदेव की उपासना करे इस विधिवाक्य में क्यों का प्रश्न नहीं होता। निमन्त्रण-भोजन के लिये बुलाना, आमन्त्रण-साधारण बुलाना, यदि अत्यावश्यक प्रतिबन्धक कार्य न हो तो अवश्य आना, अभीष्ट-सत्कारपूर्वक कहना, संप्रश्न-पूछना, प्रार्थना-सत्कारपूर्वक किसी कार्य के लिये कहना । ये विध्यादिक जानना । कृधातु से लोट् अथवा लिङ् लकार के आत्मनेपद त-प्रत्यय अथवा परस्मैपद में ति-प्रत्यय । उक्त 'उसुमु' इससे उभयत्र लोट-लिड में और आरमनेपद-परस्मैपद में उआदेश होगा। 'ततिपोः' इत्यादिकों का बाधक है । 'कृतः कुण च' इससे कुण आदेश । कुणउ । करोतु, कुरुताम्, कुर्यात् , कुर्वीत में कुणउ होगा। मध्यमपुरुष में सु आदेश, साधुत्व पूर्ववत् । तुमं कुणसु । कुर्याः, कुरुथाः, कुरु, कुरुष्व के स्थान पर कुणसु होगा। उत्तमपुरुष के एकवचन में मु आदेश होगा। हं कुणमु । करवाणि, करवै, कुर्याम् , कुर्वीय के स्थान पर कुणमु । विध्यादिक अर्थों में मध्यमपुरुप के एकवचन में अकारादेश भी विकल्प से होगा। छिद् अथवा मिद् धातु से सिप या थास् करने पर 'भिदिच्छिदोः' से द को 'न्द' आदेश । सिप, थास् को अकारादेश । तुम मिन्द, छिन्द । भिन्धि, भिन्द्याः। छिन्धि, छिन्याः। पर में-भिन्दसु, छिन्दसु इत्यादि । लभ धातु के 'खघयधः' इससे भकार को हकारादेश । सुमं लह, लहसु। त्वं लभस्व अथवा लभेथाः इति । विध्यादिक अर्थों में शौरसेनी भाषा के प्रयोग में प्रथमा के एकवचन में दु आदेश । एदु पियसही। इण धातु । णकार इत्। लोट-लिङ्ग में त अथवा तिप के स्थान में दु आदेश । 'अडादेशा बहुलम्' से अट् । ट् इत् । 'सन्धी०' इससे अकार इकार मिलकर एकार । एदु । एतु, इयात् प्रियसखी। एवम्-पअदृदु जो । पअदृदु का साधुत्व मूल में स्पष्ट है। अजो इति । आर्यः। 'यशय्यामिमन्युषु उ.' इससे 'य' को जकार। 'शेषादेशयोईिवमनादौ' इससे आदेशज-जकार को द्वित्व, 'अदातो यथादिषु वा' इससे अथवा पाली-प्राकृत-व्याकरणस्थ युके पोत उत् आदीदूतां हस्वधेति से हस्व । 'भत ओत् सो से मोकार । अजो ॥१८॥