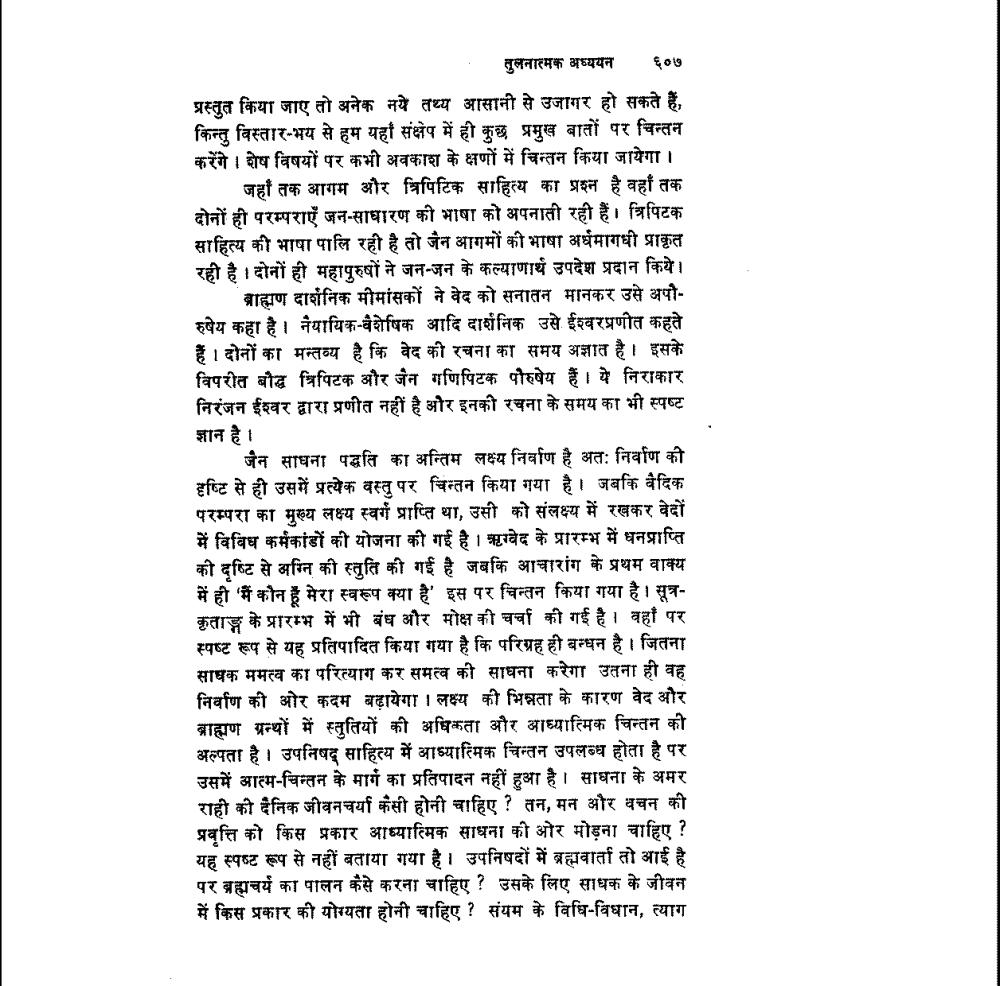________________
६०७
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए तो अनेक नये तथ्य आसानी से उजागर हो सकते हैं, किन्तु विस्तार भय से हम यहाँ संक्षेप में ही कुछ प्रमुख बातों पर चिन्तन करेंगे। शेष विषयों पर कभी अवकाश के क्षणों में चिन्तन किया जायेगा ।
जहाँ तक आगम और त्रिपिटक साहित्य का प्रश्न है वहाँ तक दोनों ही परम्पराएँ जन साधारण की भाषा को अपनाती रही हैं। त्रिपिटक साहित्य की भाषा पालि रही है तो जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी प्राकृत रही है। दोनों ही महापुरुषों ने जन-जन के कल्याणार्थ उपदेश प्रदान किये। ब्राह्मण दार्शनिक मीमांसकों ने वेद को सनातन मानकर उसे अपीरुषेय कहा है । नैयायिक-वैशेषिक आदि दार्शनिक उसे ईश्वरप्रणीत कहते हैं। दोनों का मन्तव्य है कि वेद की रचना का समय अज्ञात है। इसके विपरीत बौद्ध त्रिपिटक और जैन गणिपिटक पौरुषेय हैं। ये निराकार निरंजन ईश्वर द्वारा प्रणीत नहीं है और इनकी रचना के समय का भी स्पष्ट ज्ञान है ।
जैन साधना पद्धति का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण है अतः निर्वाण की दृष्टि से ही उसमें प्रत्येक वस्तु पर चिन्तन किया गया है। जबकि वैदिक परम्परा का मुख्य लक्ष्य स्वर्गं प्राप्ति था, उसी को संलक्ष्य में रखकर वेदों में विविध कर्मकांडों की योजना की गई है। ऋग्वेद के प्रारम्भ में धनप्राप्ति की दृष्टि से अग्नि की स्तुति की गई है जबकि आचारांग के प्रथम वाक्य में ही 'मैं कौन हूँ मेरा स्वरूप क्या है' इस पर चिन्तन किया गया है। सूत्र कृताङ्ग के प्रारम्भ में भी बंध और मोक्ष की चर्चा की गई है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि परिग्रह ही बन्धन है । जितना साधक ममत्व का परित्याग कर समत्व की साधना करेगा उतना ही वह निर्वाण की ओर कदम बढ़ायेगा । लक्ष्य की भिन्नता के कारण वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में स्तुतियों की अधिकता और आध्यात्मिक चिन्तन की अल्पता है । उपनिषद् साहित्य में आध्यात्मिक चिन्तन उपलब्ध होता है पर उसमें आत्म-चिन्तन के मार्ग का प्रतिपादन नहीं हुआ है। साधना के अमर राही को दैनिक जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए ? तन, मन और वचन की प्रवृत्ति को किस प्रकार आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना चाहिए ? यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। उपनिषदों में ब्रह्मवार्ता तो आई है पर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए ? उसके लिए साधक के जीवन में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए ? संयम के विधि-विधान, त्याग