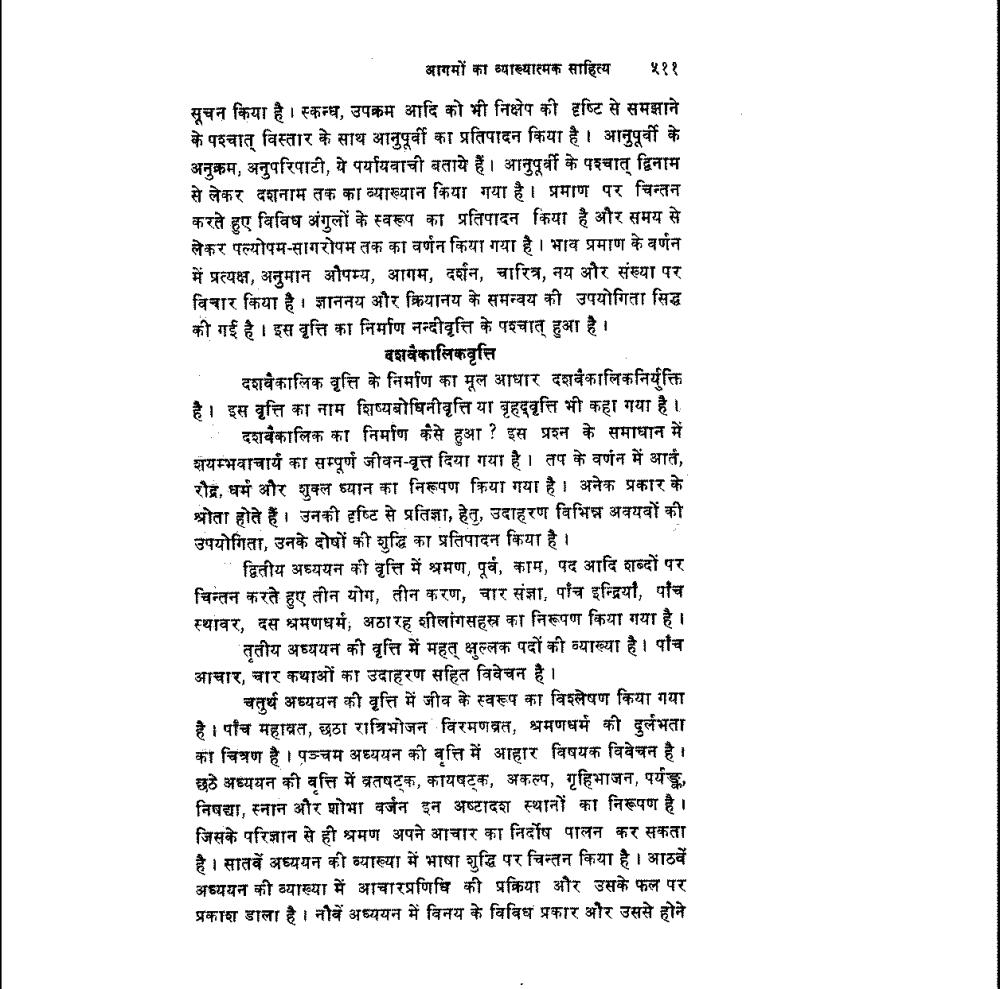________________
आगमों का व्याख्यात्मक साहित्य ५११ सूचन किया है। स्कन्ध, उपक्रम आदि को भी निक्षेप की दृष्टि से समझाने के पश्चात् विस्तार के साथ आनुपूर्वी का प्रतिपादन किया है। आनुपूर्वी के अनुक्रम, अनुपरिपाटी, ये पर्यायवाची बताये हैं। आनुपूर्वी के पश्चात् द्विनाम से लेकर दशनाम तक का व्याख्यान किया गया है। प्रमाण पर चिन्तन करते हुए विविध अंगुलों के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और समय से लेकर पल्योपम-सागरोपम तक का वर्णन किया गया है । भाव प्रमाण के वर्णन में प्रत्यक्ष, अनुमान औपम्य, आगम, दर्शन, चारित्र, नय और संख्या पर विचार किया है। ज्ञाननय और क्रियानय के समन्वय की उपयोगिता सिद्ध की गई है। इस वृत्ति का निर्माण नन्दीवृत्ति के पश्चात् हआ है।
दशवकालिकवृत्ति दशवकालिक वृत्ति के निर्माण का मूल आधार दशवकालिकनियुक्ति है। इस वृत्ति का नाम शिष्यबोधिनीवृत्ति या बृहवृत्ति भी कहा गया है।
दशवकालिक का निर्माण कैसे हुआ? इस प्रश्न के समाधान में शयम्भवाचार्य का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त दिया गया है। तप के वर्णन में आतं, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के श्रोता होते हैं। उनकी दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेत, उदाहरण विभिन्न अवयवों की उपयोगिता, उनके दोषों की शुद्धि का प्रतिपादन किया है।
द्वितीय अध्ययन की वृत्ति में श्रमण, पूर्व, काम, पद आदि शब्दों पर चिन्तन करते हुए तीन योग, तीन करण, चार संज्ञा, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच स्थावर, दस श्रमणधर्म, अठारह शीलांगसहस्र का निरूपण किया गया है।
तृतीय अध्ययन की वृत्ति में महत् क्षुल्लक पदों की व्याख्या है। पांच आचार, चार कथाओं का उदाहरण सहित विवेचन है।
चतुर्थ अध्ययन की वृत्ति में जीव के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। पांच महावत, छठा रात्रिभोजन विरमणव्रत, श्रमणधर्म की दुर्लभता का चित्रण है। पञ्चम अध्ययन की वृत्ति में आहार विषयक विवेचन है। छठे अध्ययन की वृत्ति में व्रतषट्क, कायषट्क, अकल्प, गृहिभाजन, पर्यङ्क, निषद्या, स्नान और शोभा बर्जन इन अष्टादश स्थानों का निरूपण है। जिसके परिज्ञान से ही श्रमण अपने आचार का निर्दोष पालन कर सकता है। सातवें अध्ययन की व्याख्या में भाषा शूद्धि पर चिन्तन किया है। आठवें अध्ययन की व्याख्या में आचारप्रणिधि की प्रक्रिया और उसके फल पर प्रकाश डाला है। नौवें अध्ययन में विनय के विविध प्रकार और उससे होने