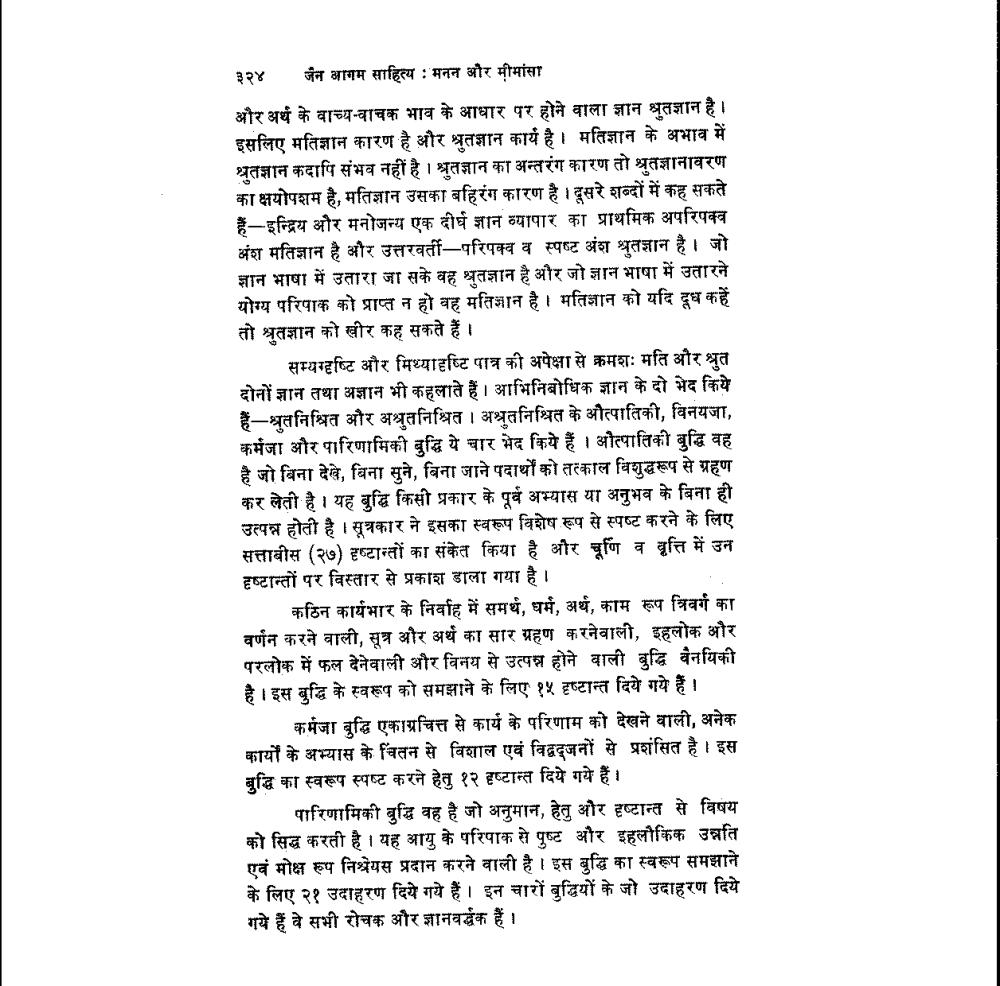________________
३२४
जैन आगम साहित्य : मनन और मीमांसा
और अर्थ के वाच्य वाचक भाव के आधार पर होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । इसलिए मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान कार्य है । मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान कदापि संभव नहीं है। श्रुतज्ञान का अन्तरंग कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है, मतिज्ञान उसका बहिरंग कारण है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं - इन्द्रिय और मनोजन्य एक दीर्घ ज्ञान व्यापार का प्राथमिक अपरिपक्व अंश मतिज्ञान है और उत्तरवर्ती - परिपक्व व स्पष्ट अंश श्रुतज्ञान है। जो ज्ञान भाषा में उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान है और जो ज्ञान भाषा में उतारने योग्य परिपाक को प्राप्त न हो वह मतिज्ञान है । मतिज्ञान को यदि दूध कहें तो श्रुतज्ञान को खीर कह सकते हैं।
सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि पात्र की अपेक्षा से क्रमशः मति और श्रुत दोनों ज्ञान तथा अज्ञान भी कहलाते हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान के दो भेद किये हैं- श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित । अश्रुतनिश्रित के औत्पातिकी, विनयजा, कर्मजा और पारिणामिकी बुद्धि ये चार भेद किये हैं । औत्पातिकी बुद्धि वह है जो बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने पदार्थों को तत्काल विशुद्धरूप से ग्रहण कर लेती है । यह बुद्धि किसी प्रकार के पूर्व अभ्यास या अनुभव के बिना ही उत्पन्न होती है । सूत्रकार ने इसका स्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए सत्तावीस (२७) दृष्टान्तों का संकेत किया है और चूर्णि व वृत्ति में उन दृष्टान्तों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है ।
कठिन कार्यभार के निर्वाह में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का वर्णन करने वाली, सूत्र और अर्थ का सार ग्रहण करनेवाली, इहलोक और परलोक में फल देनेवाली और विनय से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वैनयिकी है। इस बुद्धि के स्वरूप को समझाने के लिए १५ दृष्टान्त दिये गये हैं ।
कर्मजा बुद्धि एकाग्रचित्त से कार्य के परिणाम को देखने वाली, अनेक कार्यों के अभ्यास के चितन से विशाल एवं विद्वद्जनों से प्रशंसित है। इस बुद्धि का स्वरूप स्पष्ट करने हेतु १२ दृष्टान्त दिये गये हैं ।
पारिणामिकी बुद्धि वह है जो अनुमान, हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करती है । यह आयु के परिपाक से पुष्ट और इहलौकिक उन्नति एवं मोक्ष रूप निश्रेयस प्रदान करने वाली है। इस बुद्धि का स्वरूप समझाने के लिए २१ उदाहरण दिये गये हैं। इन चारों बुद्धियों के जो उदाहरण दिये गये हैं वे सभी रोचक और ज्ञानवर्द्धक हैं ।