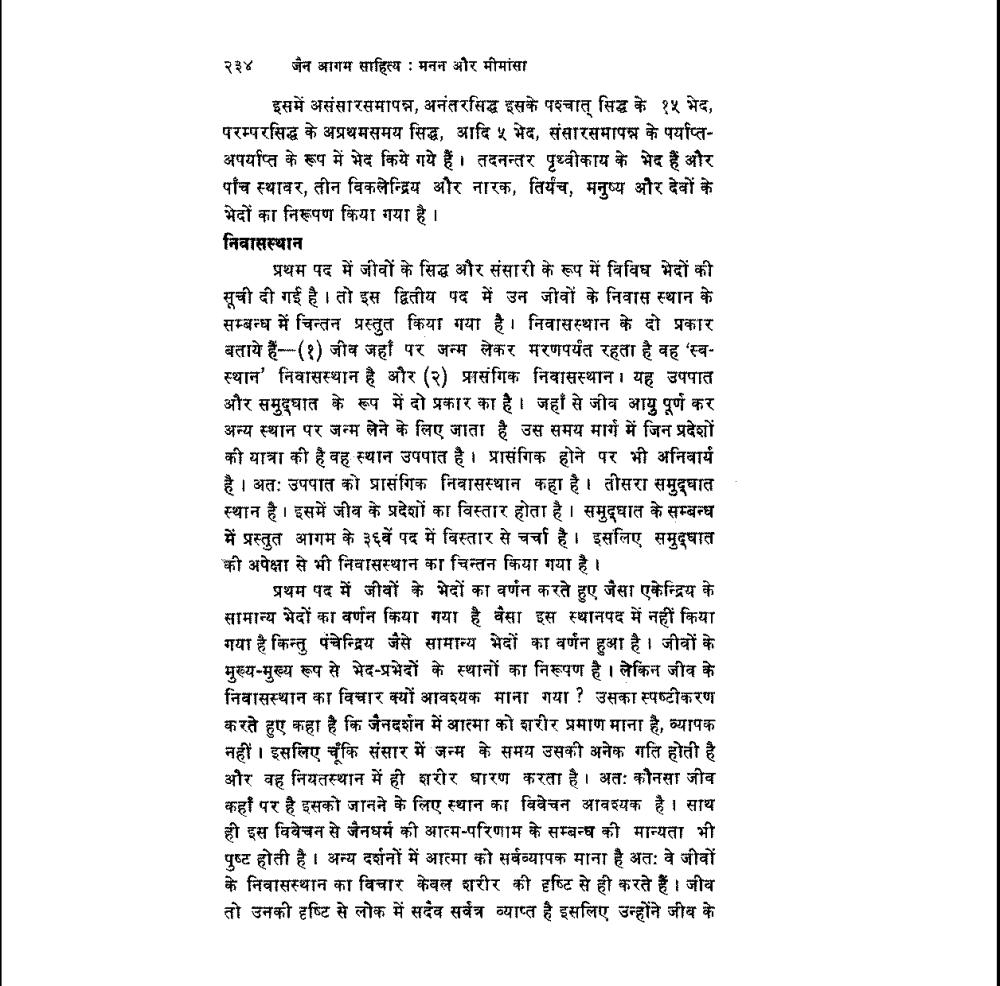________________
२३४ जैन आगम साहित्य : मनन और मीमांसा
इसमें असंसारसमापन्न, अनंतरसिद्ध इसके पश्चात् सिद्ध के १५ भेद, परम्परसिद्ध के अप्रथमसमय सिद्ध, आदि ५ भेद, संसारसमापन के पर्याप्तअपर्याप्त के रूप में भेद किये गये हैं। तदनन्तर पृथ्वीकाय के भेद हैं और पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवों के भेदों का निरूपण किया गया है। निवासस्थान
प्रथम पद में जीवों के सिद्ध और संसारी के रूप में विविध भेदों की सूची दी गई है । तो इस द्वितीय पद में उन जीवों के निवास स्थान के सम्बन्ध में चिन्तन प्रस्तुत किया गया है। निवासस्थान के दो प्रकार बताये हैं--(१) जीव जहाँ पर जन्म लेकर मरणपर्यंत रहता है वह 'स्वस्थान' निवासस्थान है और (२) प्रासंगिक निवासस्थान। यह उपपात और समुद्घात के रूप में दो प्रकार का है। जहाँ से जीव आयु पूर्ण कर अन्य स्थान पर जन्म लेने के लिए जाता है उस समय मार्ग में जिन प्रदेशों की यात्रा की है वह स्थान उपपात है। प्रासंगिक होने पर भी अनिवार्य है। अत: उपपात को प्रासंगिक निवासस्थान कहा है। तीसरा समुद्घात स्थान है। इसमें जीव के प्रदेशों का विस्तार होता है। समुद्घात के सम्बन्ध में प्रस्तुत आगम के ३६३ पद में विस्तार से चर्चा है। इसलिए समुद्घात की अपेक्षा से भी निवासस्थान का चिन्तन किया गया है।
प्रथम पद में जीवों के भेदों का वर्णन करते हए जैसा एकेन्द्रिय के सामान्य भेदों का वर्णन किया गया है वैसा इस स्थानपद में नहीं किया गया है किन्तु पंचेन्द्रिय जैसे सामान्य भेदों का वर्णन हुआ है। जीवों के मुख्य-मुख्य रूप से भेद-प्रभेदों के स्थानों का निरूपण है । लेकिन जीव के निवासस्थान का विचार क्यों आवश्यक माना गया? उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जनदर्शन में आत्मा को शरीर प्रमाण माना है, व्यापक नहीं। इसलिए चुंकि संसार में जन्म के समय उसकी अनेक गति होती है और वह नियतस्थान में ही शरीर धारण करता है। अत: कौनसा जीव कहाँ पर है इसको जानने के लिए स्थान का विवेचन आवश्यक है। साथ ही इस विवेचन से जैनधर्म की आत्म-परिणाम के सम्बन्ध की मान्यता भी पृष्ट होती है। अन्य दर्शनों में आत्मा को सर्वव्यापक माना है अत: वे जीवों के निवासस्थान का विचार केवल शरीर की दृष्टि से ही करते हैं। जीव तो उनकी दृष्टि से लोक में सदैव सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उन्होंने जीव के