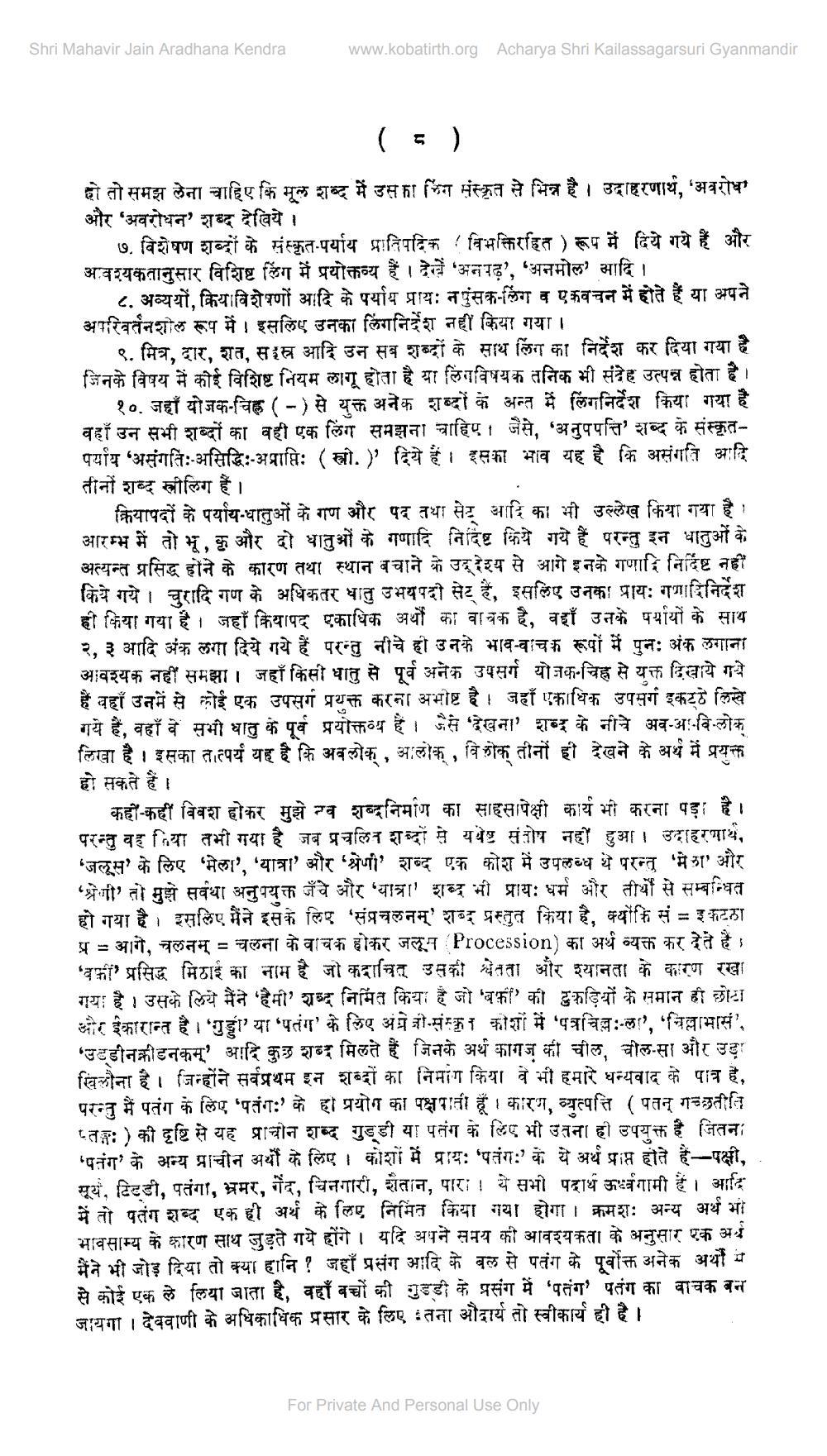________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
(
=)
हो तो समझ लेना चाहिए कि मूल शब्द में उसका लिंग संस्कृत से भिन्न है । उदाहरणार्थ, 'अवरोध' और 'अवरोधन' शब्द देखिये ।
७. विशेषण शब्दों के संस्कृत-पर्याय प्रातिपदिक विभक्तिरहित ) रूप में दिये गये हैं और आवश्यकतानुसार विशिष्ट लिंग में प्रयोक्तव्य हैं । देखें 'अनपढ़', 'अनमोल' आदि ।
८. अव्ययों, क्रियाविशेषणों आदि के पर्याय प्रायः नपुंसक लिंग व एकवचन में होते हैं या अपने अपरिवर्तनशील रूप में। इसलिए उनका लिंगनिर्देश नहीं किया गया ।
९. मित्र, दार, शत, सहस्र आदि उन सब शब्दों के साथ लिंग का निर्देश कर दिया गया है जिनके विषय में कोई विशिष्ट नियम लागू होता है या लिंगविषयक तनिक भी संदेह उत्पन्न होता है। १०. जहाँ योजक- चिह्न ( - ) से युक्त अनेक शब्दों के अन्त में लिंगनिर्देश किया गया है वहाँ उन सभी शब्दों का वही एक लिंग समझना चाहिए। जैसे, 'अनुपपत्ति' शब्द के संस्कृतपर्याय 'असंगति:- असिद्धि: - अप्राप्तिः (स्त्री.)' दिये हैं। इसका भाव यह है कि असंगति आदि तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं ।
क्रियापदों के पर्याय धातुओं के गण और पद तथा सेट् आदि का भी उल्लेख किया गया है। आरम्भ में तो भू, कृ और दो धातुओं के गणादि निर्दिष्ट किये गये हैं परन्तु इन धातुओं के अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण तथा स्थान बचाने के उद्देश्य से आगे इनके गणादि निर्दिष्ट नहीं किये गये । चुरादि गण के अधिकतर धातु उभयपदी सेट हैं, इसलिए उनका प्रायः गणादिनिर्देश ही किया गया है। जहाँ क्रियापद एकाधिक अर्थों का वाचक है, वहाँ उनके पर्यायों के साथ २, ३ आदि अंक लगा दिये गये हैं परन्तु नीचे ही उनके भाव वाचक रूपों में पुनः अंक लगाना आवश्यक नहीं समझा। जहाँ किसी धातु से पूर्व अनेक उपसर्ग योजक चिह्न से युक्त दिखाये गये हैं वहाँ उनमें से कोई एक उपसर्ग प्रयुक्त करना अभीष्ट है। जहाँ एकाधिक उपसर्ग इकट्ठे लिखे गये हैं, वहाँ वे सभी धातु के पूर्व प्रयोक्तव्य हैं। जैसे 'देखना ' शब्द के नीचे अव- अ-वि-लोक् लिखा है । इसका तात्पर्य यह है कि अवलोक्, आलोक, विलोक्य तीनों ही देखने के अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं ।
कहीं-कहीं विवश होकर मुझे नव शब्दनिर्माण का साहसापेक्षी कार्य भी करना पड़ा है । परन्तु वह दिया तभी गया है जब प्रचलित शब्दों से यथेष्ट संतोष नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, 'जलूस' के लिए 'मेला', 'यात्रा' और 'श्रेणी' शब्द एक कोश में उपलब्ध थे परन्तु 'मेला' और 'श्रेणी' तो मुझे सर्वथा अनुपयुक्त जँचे और 'यात्रा' शब्द भी प्रायः धर्म और तीर्थों से सम्बन्धित हो गया है। इसलिए मैंने इसके लिए 'संप्रचलनम्' शब्द प्रस्तुत किया है, क्योंकि सं = इकटठा प्र = आगे, चलनम् = चलना के वाचक होकर जलूम (Procession) का अर्थ व्यक्त कर देते हैं। 'बी' प्रसिद्ध मिठाई का नाम है जो कदाचित् उसकी चेतता और श्यानता के कारण रखा गया है । उसके लिये मैंने 'हैमी' शब्द निर्मित किया है जो 'बर्फी' की टुकड़ियों के समान ही छोटा और ईकारान्त है । 'गुड्डी' या 'पतंग' के लिए अंग्रेजी संस्कृत कोशों में 'पत्रचिल्ल:-ला', 'चिल्लाभासं', 'उड्डीनक्रीडनकम्' आदि कुछ शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ कागज़ की चील, चील-सा और उड़ा खिलौना है । जिन्होंने सर्वप्रथम इन शब्दों का निर्माांग किया वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु मैं पतंग के लिए 'पतंग' के हो प्रयोग का पक्षपाती हूँ । कारण, व्युत्पत्ति (पतन् गच्छतीति पतङ्गः ) की दृष्टि से यह प्राचीन शब्द गुड्डी या पतंग के लिए भी उतना ही उपयुक्त है जितना 'पतंग' के अन्य प्राचीन अर्थों के लिए । कोशों में प्रायः 'पतंग' के ये अर्थ प्राप्त होते हैं -पक्षी, सूर्य, टिटडी, पतंगा, भ्रमर, गेंद, चिनगारी, शैतान, पारा। ये सभी पदार्थ ऊर्ध्वगामी हैं। आदि में तो पतंग शब्द एक ही अर्थ के लिए निर्मित किया गया होगा । क्रमशः अन्य अर्थ भी भावसाम्य के कारण साथ जुड़ते गये होंगे । यदि अपने समय की आवश्यकता के अनुसार एक अ मैंने भी जोड़ दिया तो क्या हानि ? जहाँ प्रसंग आदि के बल से पतंग के पूर्वोक्त अनेक अर्थों में से कोई एक ले लिया जाता है, वहाँ बच्चों की गुड्डी के प्रसंग में 'पतंग' पतंग का वाचक बन जायगा । देववाणी के अधिकाधिक प्रसार के लिए उतना औदार्य तो स्वीकार्य ही है ।
★
For Private And Personal Use Only