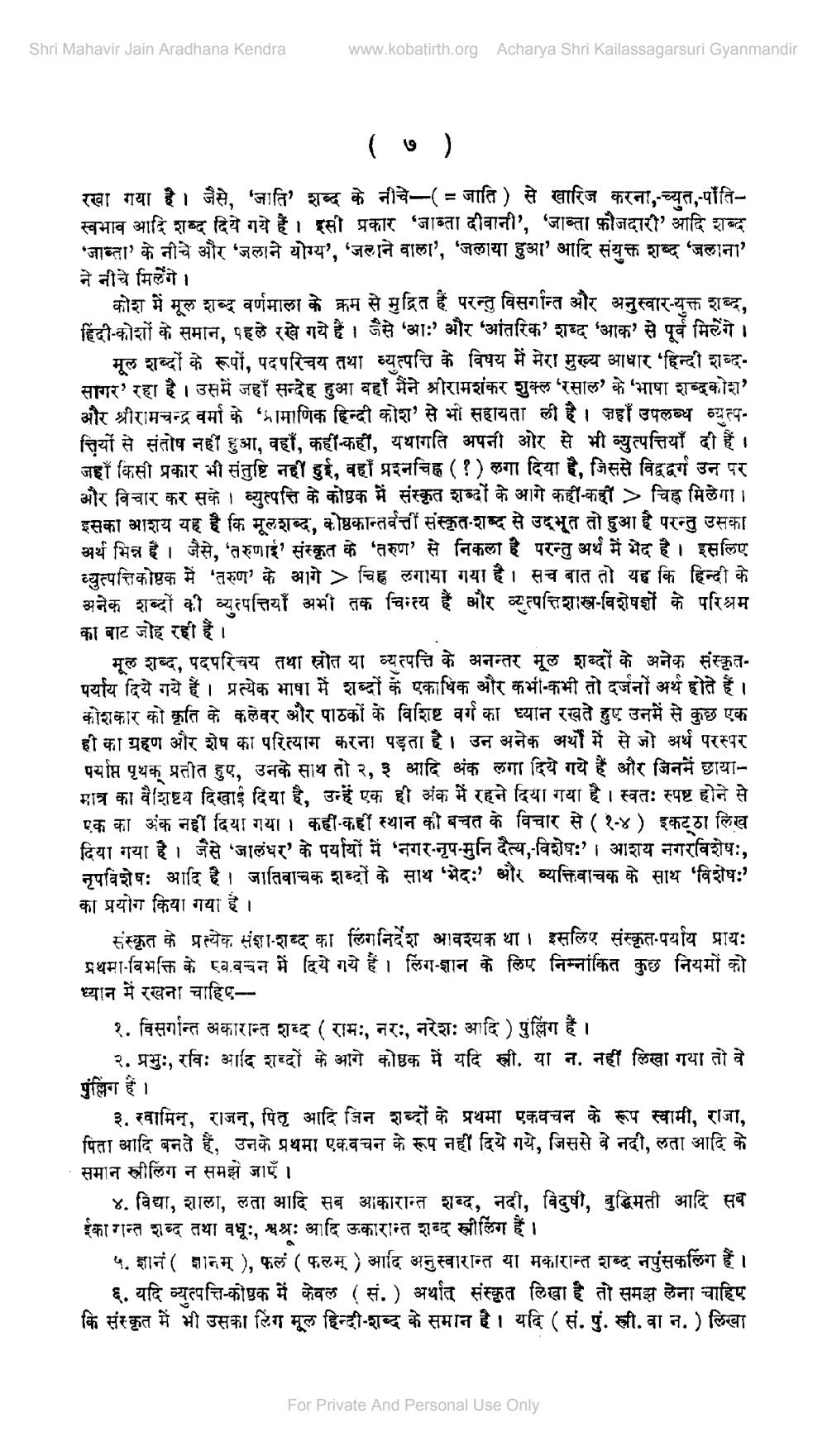________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
(
७
)
रखा गया है । जैसे, 'जाति' शब्द के नीचे - ( = जाति ) से खारिज करना, च्युत, प - पाँतिस्वभाव आदि शब्द दिये गये हैं । इसी प्रकार 'जाब्ता दीवानी', 'जाब्ता फ़ौजदारी' आदि शब्द 'जाब्ता' के नीचे और 'जलाने योग्य', 'जलाने वाला', 'जलाया हुआ' आदि संयुक्त शब्द 'जलाना ' ने नीचे मिलेंगे ।
कोश में मूल शब्द वर्णमाला के क्रम से मुद्रित हैं परन्तु विसर्गान्त और अनुस्वार-युक्त शब्द, हिंदी - कोशों के समान, पहले रखे गये हैं । जैसे 'आ' और 'आंतरिक ' शब्द 'आक' से पूर्व मिलेंगे ।
मूल शब्दों के रूपों, पदपरिचय तथा व्युत्पत्ति के विषय में मेरा मुख्य आधार 'हिन्दी शब्दसागर' रहा है । उसमें जहाँ सन्देह हुआ वहाँ मैंने श्रीरामशंकर शुक्ल 'रसाल' के 'भाषा शब्दकोश' और श्रीरामचन्द्र वर्मा के 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' से भी सहायता ली है । जहाँ उपलब्ध व्युत्पन तियों से संतोष नहीं हुआ, वहाँ, कहीं-कहीं, यथागति अपनी ओर से भी व्युत्पत्तियाँ दी हैं । जहाँ किसी प्रकार भी संतुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्रश्नचिह्न ( ? ) लगा दिया है, जिससे विद्वद्वर्ग उन पर और विचार कर सके । व्युत्पत्ति के कोष्ठक में संस्कृत शब्दों के आगे कहीं-कहीं > चिह्न मिलेगा । इसका आशय यह है कि मूलशब्द, कोष्ठकान्तर्वत्त संस्कृत शब्द से उद्भूत तो हुआ है परन्तु उसका अर्थ भिन्न है । जैसे, 'तरुणाई' संस्कृत के 'तरुण' से निकला है परन्तु अर्थ में भेद है । इसलिए व्युत्पत्तिकोष्ठक में 'तरुण' के आगे > चिह्न लगाया गया है। सच बात तो यह कि हिन्दी के अनेक शब्दों की व्युत्पत्तियाँ अभी तक चिन्त्य हैं और व्युत्पत्तिशास्त्र - विशेषज्ञों के परिश्रम का बाट जोह रही हैं।
मूल शब्द, पदपरिचय तथा स्रोत या व्युत्पत्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक संस्कृतपर्याय दिये गये हैं । प्रत्येक भाषा में शब्दों के एकाधिक और कभी-कभी तो दर्जनों अर्थ होते हैं । कोशकार को कृति के कलेवर और पाठकों के विशिष्ट वर्ग का ध्यान रखते हुए उनमें से कुछ एक ही का ग्रहण और शेष का परित्याग करना पड़ता है । उन अनेक अर्थों में से जो अर्थ परस्पर पर्याप्त पृथक् प्रतीत हुए, उनके साथ तो २, ३ आदि अंक लगा दिये गये हैं और जिनमें छायामात्र का वैशिष्टय दिखाई दिया है, उन्हें एक ही अंक में रहने दिया गया है । स्वतः स्पष्ट होने से एक का अंक नहीं दिया गया। कहीं कहीं स्थान की बचत के विचार से (१-४ ) इकट्ठा लिख दिया गया है । जैसे 'जालंधर' के पर्यायों में 'नगर- नृप - मुनि दैत्य, विशेष : ' । आशय नगरविशेषः, नृपविशेषः आदि है । जातिवाचक शब्दों के साथ 'भेद:' और व्यक्तिवाचक के साथ 'विशेषः ' का प्रयोग किया गया है ।
ܕ
संस्कृत के प्रत्येक संज्ञा-शब्द का लिंगनिर्देश आवश्यक था। इसलिए संस्कृत- पर्याय प्रायः प्रथमा विभक्ति के स्ववचन में दिये गये हैं । लिंग-ज्ञान के लिए निम्नांकित कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए—
२. विसर्गान्त अकारान्त शब्द ( रामः, नरः, नरेश: आदि) पुल्लिंग हैं ।
२. प्रभुः, रविः आदि शब्दों के आगे कोष्ठक में यदि स्त्री. या न नहीं लिखा गया तो वे पुल्लिंग हैं ।
३. स्वामिन, राजन, पितृ आदि जिन शब्दों के प्रथमा एकवचन के रूप स्वामी, राजा, पिता आदि बनते हैं, उनके प्रथमा एकवचन के रूप नहीं दिये गये, जिससे वे नदी, लता आदि के समान स्त्रीलिंग न समझे जाएँ ।
४. विद्या, शाला, लता आदि सब आकारान्त शब्द, नदी, विदुषी, बुद्धिमती आदि सब ईकारान्त शब्द तथा वधूः, श्वश्रः आदि उकारान्त शब्द स्त्रीलिंग हैं ।
५. ज्ञानं ( ज्ञानम् ), फलं ( फलम् ) आदि अनुस्वारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकलिंग हैं । ६. यदि व्युत्पत्ति कोष्ठक में केवल (सं.) अर्थात् संस्कृत लिखा है तो समझ लेना चाहिए कि संस्कृत में भी उसका लिंग मूल हिन्दी शब्द के समान है । यदि ( सं. पुं. स्त्री. वा न. ) लिखा
For Private And Personal Use Only