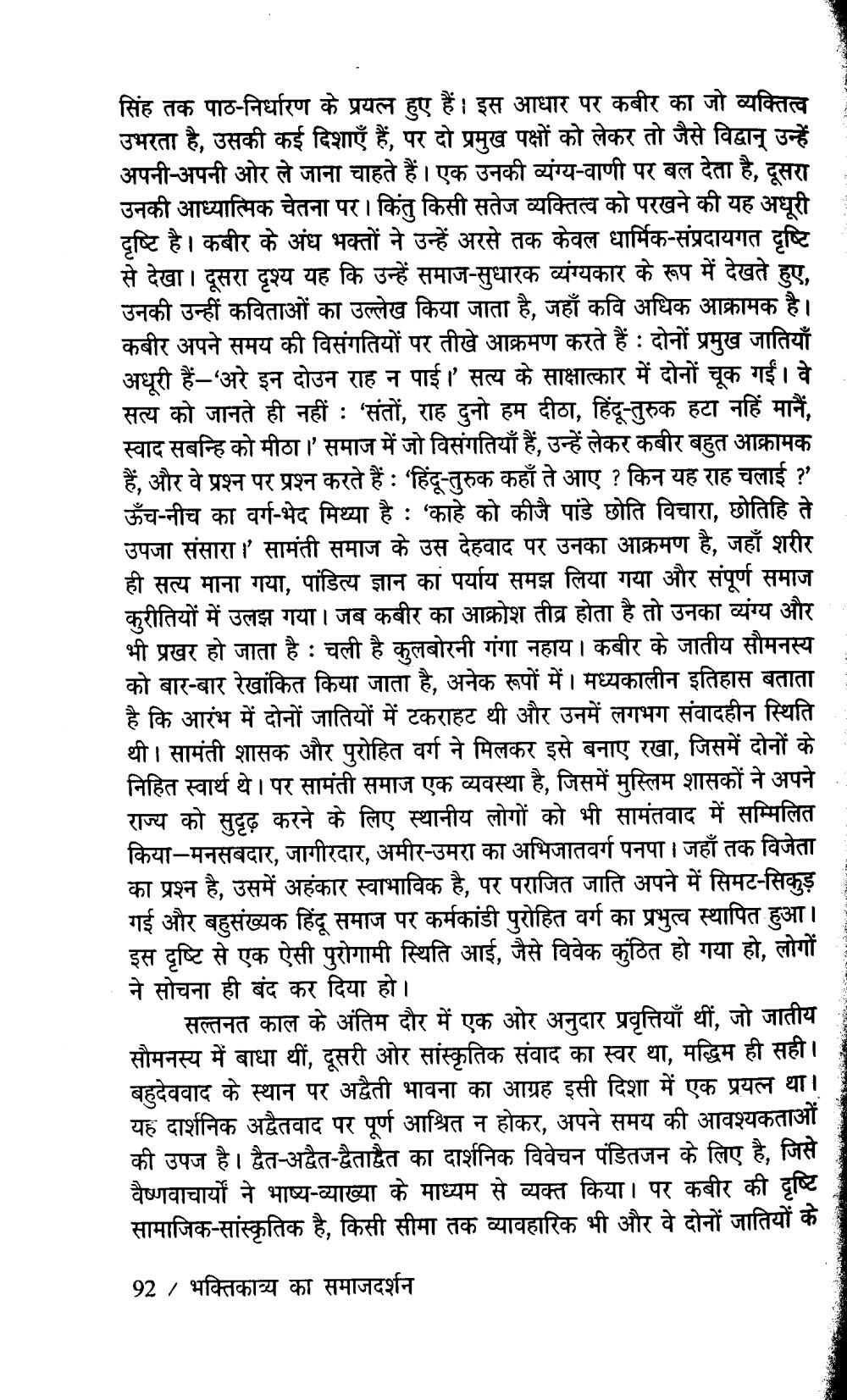________________
सिंह तक पाठ-निर्धारण के प्रयत्न हुए हैं। इस आधार पर कबीर का जो व्यक्तित्व उभरता है, उसकी कई दिशाएँ हैं, पर दो प्रमुख पक्षों को लेकर तो जैसे विद्वान उन्हें अपनी-अपनी ओर ले जाना चाहते हैं। एक उनकी व्यंग्य-वाणी पर बल देता है, दूसरा उनकी आध्यात्मिक चेतना पर। किंतु किसी सतेज व्यक्तित्व को परखने की यह अधूरी दृष्टि है। कबीर के अंध भक्तों ने उन्हें अरसे तक केवल धार्मिक-संप्रदायगत दृष्टि से देखा। दूसरा दृश्य यह कि उन्हें समाज-सुधारक व्यंग्यकार के रूप में देखते हुए, उनकी उन्हीं कविताओं का उल्लेख किया जाता है, जहाँ कवि अधिक आक्रामक है। कबीर अपने समय की विसंगतियों पर तीखे आक्रमण करते हैं : दोनों प्रमुख जातियाँ अधूरी हैं-'अरे इन दोउन राह न पाई। सत्य के साक्षात्कार में दोनों चूक गईं। वे सत्य को जानते ही नहीं : 'संतों, राह दुनो हम दीठा, हिंदू-तुरुक हटा नहिं मानें, स्वाद सबन्हि को मीठा।' समाज में जो विसंगतियाँ हैं, उन्हें लेकर कबीर बहुत आक्रामक हैं, और वे प्रश्न पर प्रश्न करते हैं : 'हिंदू-तुरुक कहाँ ते आए ? किन यह राह चलाई ? ऊँच-नीच का वर्ग-भेद मिथ्या है : 'काहे को कीजै पांडे छोति विचारा, छोतिहि ते उपजा संसारा।' सामंती समाज के उस देहवाद पर उनका आक्रमण है, जहाँ शरीर ही सत्य माना गया, पांडित्य ज्ञान का पर्याय समझ लिया गया और संपूर्ण समाज करीतियों में उलझ गया। जब कबीर का आक्रोश तीव्र होता है तो उनका व्यंग्य और भी प्रखर हो जाता है : चली है कुलबोरनी गंगा नहाय। कबीर के जातीय सौमनस्य को बार-बार रेखांकित किया जाता है, अनेक रूपों में। मध्यकालीन इतिहास बताता है कि आरंभ में दोनों जातियों में टकराहट थी और उनमें लगभग संवादहीन स्थिति थी। सामंती शासक और परोहित वर्ग ने मिलकर इसे बनाए रखा, जिसमें दोनों के निहित स्वार्थ थे। पर सामंती समाज एक व्यवस्था है, जिसमें मुस्लिम शासकों ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय लोगों को भी सामंतवाद में सम्मिलित किया-मनसबदार, जागीरदार, अमीर-उमरा का अभिजातवर्ग पनपा। जहाँ तक विजेता का प्रश्न है, उसमें अहंकार स्वाभाविक है, पर पराजित जाति अपने में सिमट-सिकुड़ गई और बहुसंख्यक हिंदू समाज पर कर्मकांडी पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस दृष्टि से एक ऐसी पुरोगामी स्थिति आई, जैसे विवेक कुंठित हो गया हो, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया हो।
सल्तनत काल के अंतिम दौर में एक ओर अनुदार प्रवृत्तियाँ थीं, जो जातीय सौमनस्य में बाधा थीं, दूसरी ओर सांस्कृतिक संवाद का स्वर था, मद्धिम ही सही।। बहुदेववाद के स्थान पर अद्वैती भावना का आग्रह इसी दिशा में एक प्रयत्न था। यह दार्शनिक अद्वैतवाद पर पूर्ण आश्रित न होकर, अपने समय की आवश्यकताओं की उपज है। द्वैत-अद्वैत-द्वैताद्वैत का दार्शनिक विवेचन पंडितजन के लिए है, जिसे । वैष्णवाचार्यों ने भाष्य-व्याख्या के माध्यम से व्यक्त किया। पर कबीर की दृष्टि सामाजिक-सांस्कृतिक है, किसी सीमा तक व्यावहारिक भी और वे दोनों जातियों के
ani
92 / भक्तिकाव्य का समाजदर्शन