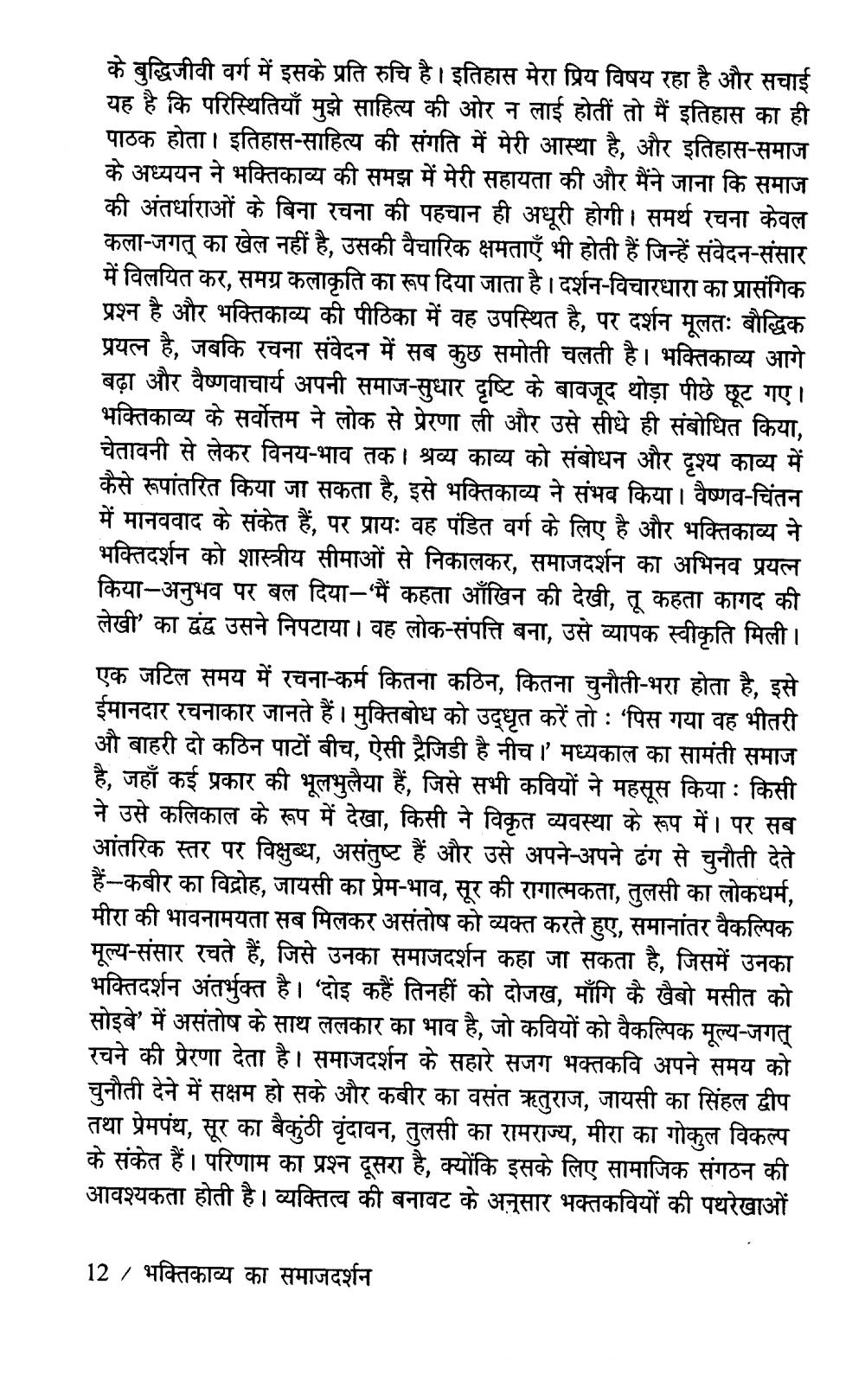________________
1
के बुद्धिजीवी वर्ग में इसके प्रति रुचि है । इतिहास मेरा प्रिय विषय रहा है और सचाई यह है कि परिस्थितियाँ मुझे साहित्य की ओर न लाई होतीं तो मैं इतिहास का ही पाठक होता । इतिहास - साहित्य की संगति में मेरी आस्था है, और इतिहास - समाज के अध्ययन ने भक्तिकाव्य की समझ में मेरी सहायता की और मैंने जाना कि समाज की अंतर्धाराओं के बिना रचना की पहचान ही अधूरी होगी । समर्थ रचना केवल कला - जगत् का खेल नहीं है, उसकी वैचारिक क्षमताएँ भी होती हैं जिन्हें संवेदन- संसार में विलयित कर, समग्र कलाकृति का रूप दिया जाता है। दर्शन- विचारधारा का प्रासंगिक प्रश्न है और भक्तिकाव्य की पीठिका में वह उपस्थित है, पर दर्शन मूलतः बौद्धिक प्रयत्न है, जबकि रचना संवेदन में सब कुछ समोती चलती है। भक्तिकाव्य आगे बढ़ा और वैष्णवाचार्य अपनी समाज-सुधार दृष्टि के बावजूद थोड़ा पीछे छूट गए । भक्तिकाव्य के सर्वोत्तम ने लोक से प्रेरणा ली और उसे सीधे ही संबोधित किया, चेतावनी से लेकर विनय भाव तक । श्रव्य काव्य को संबोधन और दृश्य काव्य में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, इसे भक्तिकाव्य ने संभव किया। वैष्णव- चिंतन में मानववाद के संकेत हैं, पर प्रायः वह पंडित वर्ग के लिए है और भक्तिकाव्य ने भक्तिदर्शन को शास्त्रीय सीमाओं से निकालकर, समाजदर्शन का अभिनव प्रयत्न किया - अनुभव पर बल दिया- 'मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी' का द्वंद्व उसने निपटाया । वह लोक-संपत्ति बना, उसे व्यापक स्वीकृति मिली ।
एक जटिल समय में रचना - कर्म कितना कठिन कितना चुनौती भरा होता है, इसे ईमानदार रचनाकार जानते हैं । मुक्तिबोध को उद्धृत करें तो : 'पिस गया वह भीतरी औ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रैजिडी है नीच ।' मध्यकाल का सामंती समाज है, जहाँ कई प्रकार की भूलभुलैया हैं, जिसे सभी कवियों ने महसूस किया : किसी ने उसे कलिकाल के रूप में देखा, किसी ने विकृत व्यवस्था के रूप में । पर सब आंतरिक स्तर पर विक्षुब्ध, असंतुष्ट हैं और उसे अपने-अपने ढंग से चुनौती देते हैं-कबीर का विद्रोह, जायसी का प्रेम-भाव, सूर की रागात्मकता, तुलसी का लोकधर्म, मीरा की भावनामयता सब मिलकर असंतोष को व्यक्त करते हुए, समानांतर वैकल्पिक मूल्य-संसार रचते हैं, जिसे उनका समाजदर्शन कहा जा सकता है, जिसमें उनका भक्तिदर्शन अंतर्भुक्त है । 'दोइ कहैं तिनहीं को दोजख, माँगि कै खैबो मसीत को सोइबे' में असंतोष के साथ ललकार का भाव है, जो कवियों को वैकल्पिक मूल्य-जगत् रचने की प्रेरणा देता है । समाजदर्शन के सहारे सजग भक्तकवि अपने समय को चुनौती देने में सक्षम हो सके और कबीर का वसंत ऋतुराज, जायसी का सिंहल द्वीप तथा प्रेमपंथ, सूर का बैकुंठी वृंदावन, तुलसी का रामराज्य, मीरा का गोकुल विकल्प के संकेत हैं। परिणाम का प्रश्न दूसरा है, क्योंकि इसके लिए सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार भक्तकवियों की पथरेखाओं
12 / भक्तिकाव्य का समाजदर्शन