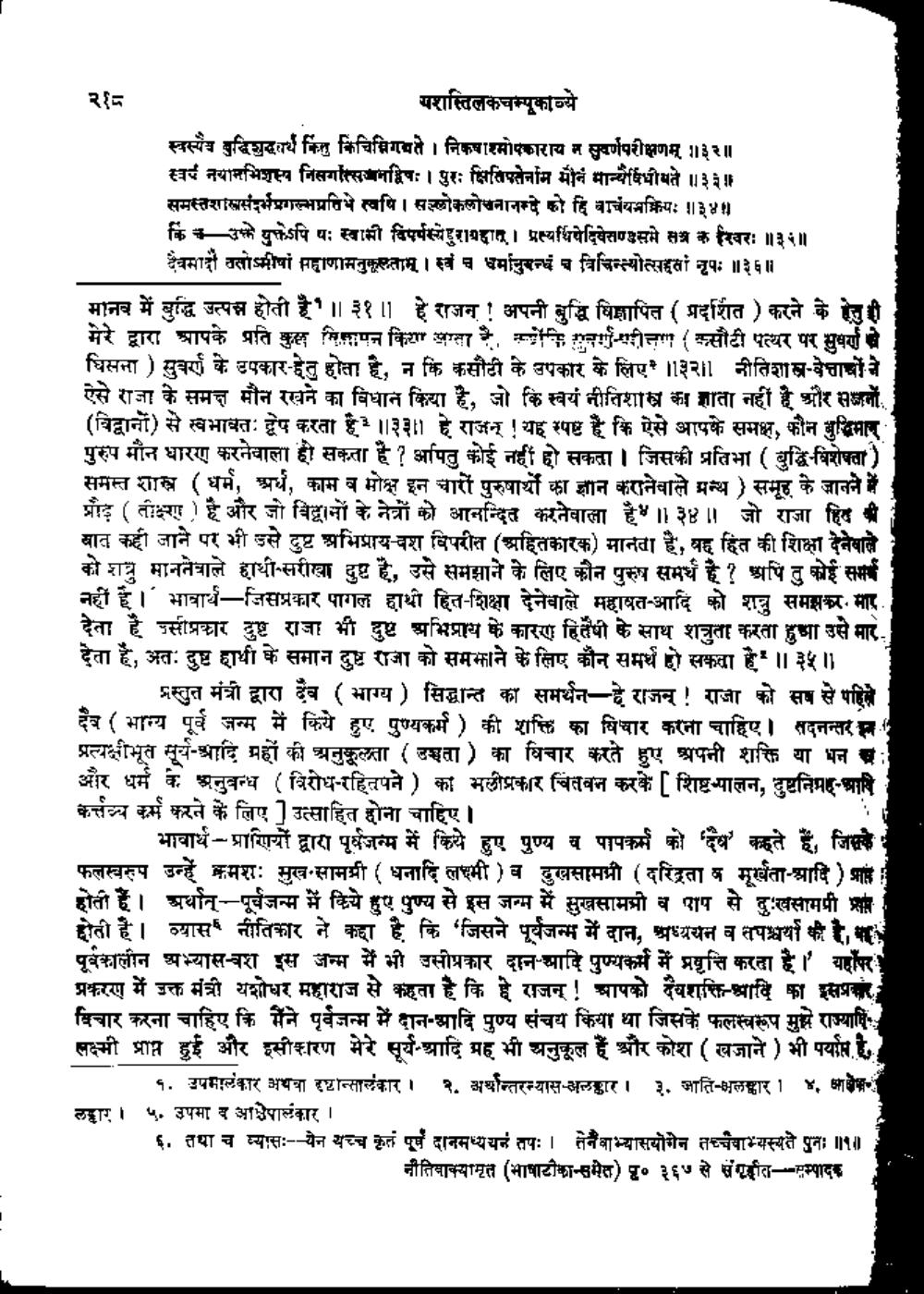________________
२१८
यशस्तिलकचम्पूकाव्ये
स्वस्य बुद्धिशुद्ध किंतु किंचिनिगद्यते । निकषाश्मोपकाराय न सुवर्णपरीक्षणम् ॥१३२॥ स्वयं नयामभिशस्य निसर्गास्मद्विषः । पुरः क्षितिपतेनाम मौनं मान्यविधीयते ॥ ३३ ॥ समस्तशास्त्रसंदर्भप्रगल्भ प्रतिभे स्वषि । सल्लोकलोचनानन्दे को हि वाचंयमक्रियः || ३४११ किं युक्तेऽपि यः स्वामी विपर्यस्येहुरा०द्वात् । प्रस्यधियेदिवेसण्डसमे सत्र के ईश्वरः ॥ ३२ ॥ arriadishti माणामनुकूलताम् । स्वं च धर्मानुबन्धं च विचिन्त्योत्सहसां नृपः ॥ ३६ ॥
मानव में बुद्धि उत्पन्न होती है' ॥ ३१ ॥ हे राजन! अपनी बुद्धि विज्ञापित ( प्रदर्शित ) करने के हेतु ही मेरे द्वारा आपके प्रति कुल विलापन किया जाता है की (कसौटी पत्थर पर सुवर्ण से घिसना ) सुवर्ण के उपकार हेतु होता है, न कि कसौटी के उपकार के लिए ||३२|| नीतिशास्त्र - वेताचों ने ऐसे राजा के समक्ष मौन रखने का विधान किया है, जो कि स्वयं नीतिशास्त्र का ज्ञाता नहीं है और जनों (विद्वानों) से स्वभावतः द्वेष करता है ||३३|| हे राजन् ! यह स्पष्ट है कि ऐसे आपके समक्ष, कौन बुद्धिमान् पुरुप मौन धारण करनेवाला हो सकता है ? अपितु कोई नहीं हो सकता। जिसकी प्रतिभा ( बुद्धि-विशेषता ) समस्त शास्त्र ( धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो का ज्ञान करानेवाले ग्रन्थ ) समूह के जानने में मौड़ ( तीक्ष्णा ) है और जो विद्वानों के नेत्रों को आनन्दित करनेवाला है ४ ॥ ३४ ॥ जो राजा हिंद की बात कही जाने पर भी उसे दुष्ट अभिप्रायवश विपरीत (अहितकारक ) मानता है, वह हिंत की शिक्षा देनेवाले को शत्रु माननेवाले हाथी - सरीखा दुष्ट है, उसे समझाने के लिए कौन पुरुष समर्थ है ? अपि तु कोई समर्थ नहीं है। भावार्थ - जिसप्रकार पागल हाथी हित-शिक्षा देनेवाले महावत आदि को शत्रु समझकर मार देता है उसीप्रकार दुष्ट राजा भी दुष्ट अभिप्राय के कारण हितैषी के साथ शत्रुता करता हुआ उसे मारदेता है, अतः दुष्ट हाथी के समान दुष्ट राजा को समझाने के लिए कौन समर्थ हो सकता है" ।। ३५ ।।
प्रस्तुत मंत्री द्वारा दैव ( भाग्य ) सिद्धान्त का समर्थन दे राजन ! राजा को सब से पहिले देव ( भाग्य पूर्व जन्म में किये हुए पुण्यकर्म ) की शक्ति का विचार करना चाहिए। सदनन्तर इन प्रत्यक्षीभूत सूर्य आदि महों की अनुकूलता ( उच्चता ) का विचार करते हुए अपनी शक्ति या धन और धर्म के अनुबन्ध ( विरोध-रहितपने ) का भलीप्रकार चितवन करके [ शिष्टपालन, दुष्टनिमह-आदि कर्त्तव्य कर्म करने के लिए ] उत्साहित होना चाहिए ।
भावार्थ - प्राणियों द्वारा पूर्वजन्म में किये हुए पुण्य व पापकर्म को 'देव' कहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्रमश: सुख-सामग्री ( धनादि लक्ष्मी ) व दुखसामग्री ( दरिद्रता व मूर्खता आदि ) आहे होती हैं। अर्थात् - पूर्वजन्म में किये हुए पुण्य से इस जन्म में सुखसामग्री व राप से दुःखसामग्री प्र होती है | व्यास नीतिकार ने कहा है कि 'जिसने पूर्वजन्म में दान, अध्ययन व तपश्चर्या की है, पूर्वकालीन अभ्यास वरा इस जन्म में भी उसीप्रकार दान आदि पुण्यकर्म में प्रवृत्ति करता है।' यहाँपर प्रकरण में उक्त मंत्री यशोधर महाराज से कहता है कि हे राजन् ! आपको देवशक्ति- ध्यादि का इस विचार करना चाहिए कि मैंने पूर्वजन्म में दान आदि पुण्य संचय किया था जिसके फलस्वरूप मुझे राज्याधि लक्ष्मी प्राप्त हुई और इसी कारण मेरे सूर्य आदि ग्रह भी अनुकूल हैं और कोश ( खजाने ) भी पर्याप्त है
१. उपमालंकार अथवा दृष्टान्तालंकार । २. अर्थान्तरन्यास - अलङ्कार । ३. जाति - अलङ्कार 1 ४. आक्षे ५. उपमा व आपालंकार ।
६. तथा च व्यासः -- येन यच्च कृतं पूर्वं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन तच्चैवाभ्यस्यते पुनः ॥१॥ नीतिवाक्यामृत (भाषाटीका समेत) पृ० ३६७ से संगृहीतसम्पादक
लड्डार